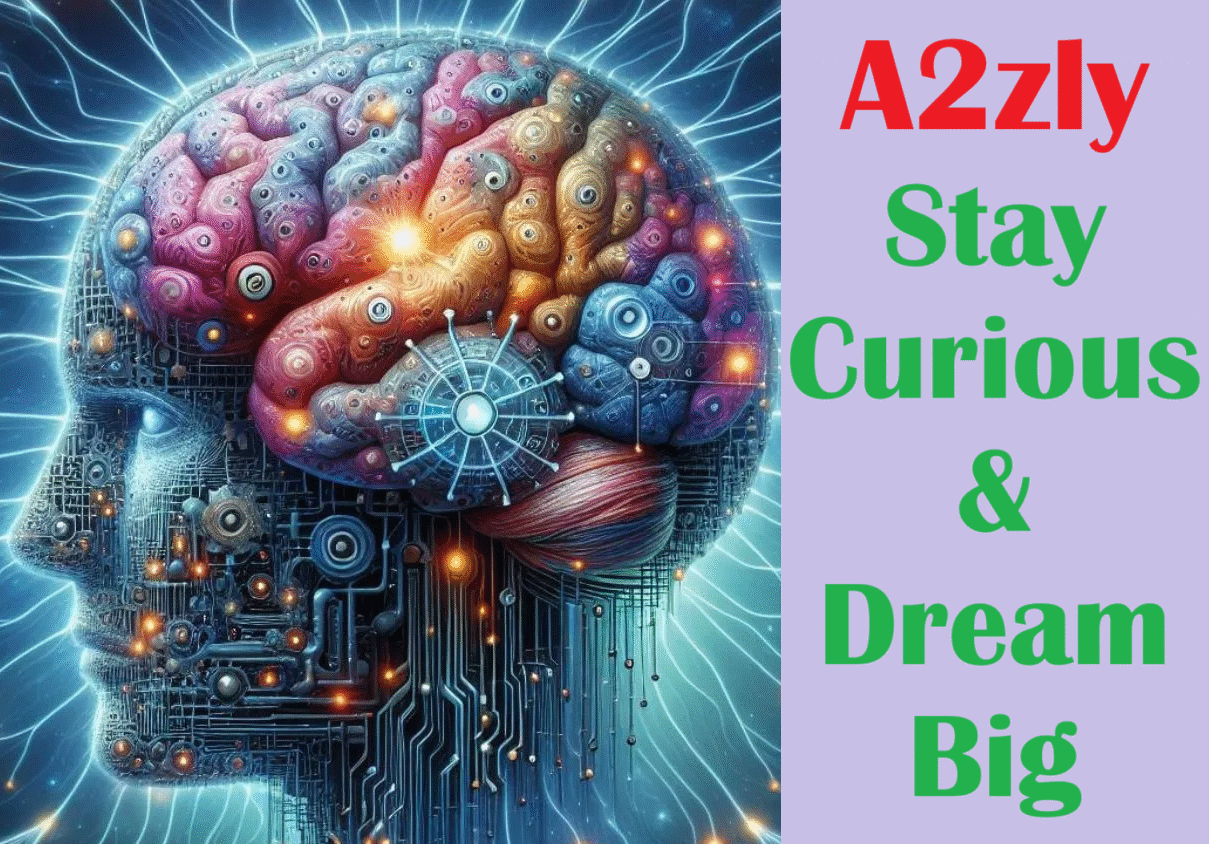Table of Contents
अध्याय 1-“स्वदेश” कविता के नोट्स प्रश्न-उत्तर रूप में
प्रश्न 1: “स्वदेश” कविता के कवि कौन हैं?
उत्तर 1: “स्वदेश” कविता के कवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ हैं, जो छायावाद आंदोलन के प्रमुख हिंदी कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 1898 में हुआ और मृत्यु 1972 में हुई ।
प्रश्न 2: कविता “स्वदेश” का केंद्रीय विषय क्या है?
उत्तर 2: कविता का केंद्रीय विषय देश-प्रेम है, जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत, और सामूहिक शक्ति के प्रति गर्व और समर्पण को दर्शाता है ।
प्रश्न 3: कवि देश-प्रेम के अभाव वाले हृदय को कैसे वर्णित करते हैं?
उत्तर 3: कवि देश-प्रेम के अभाव वाले हृदय को “पत्थर” कहते हैं, जो निर्जन और भावनाहीन है ।
प्रश्न 4: कविता में सार्थक जीवन की क्या विशेषताएँ बताई गई हैं?
उत्तर 4: सार्थक जीवन में उत्साह (जोश), साहस, भावनात्मक गहराई (भाव), और संसार के साथ प्रगति की गति में चलना शामिल है, जो राष्ट्रीय उत्थान में योगदान देता है।
प्रश्न 5: कविता में मातृभूमि को कैसे चित्रित किया गया है?
उत्तर 5: मातृभूमि को पोषण देने वाली माता-पिता के रूप में दर्शाया गया है, जो जल-पानी प्रदान करती है और जहाँ लोग इसके “राजा-रानी” हैं ।
प्रश्न 6: कविता में साहस की क्या भूमिका है?
उत्तर 6: साहस प्रगति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है, जैसे युद्ध में तोप और तलवार, जो चुनौतियों को पार करने में सहायक है ।
प्रश्न 7: कविता देश के वैश्विक प्रभाव को कैसे दर्शाती है?
उत्तर 7: कविता देश के ज्ञान और धन को खजाने के रूप में प्रस्तुत करती है, जो विश्व को प्रभावित और आकर्षित करता है।
प्रश्न 8: कवि का आह्वान क्या है?
उत्तर 8: कवि एकता, साहस और राष्ट्रीय प्रगति में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हैं, यह कहते हुए कि सब कुछ हमारे हाथों में है ।
प्रश्न 9: कविता में प्रतीकात्मकता का उपयोग कैसे हुआ है?
उत्तर 9: “पत्थर हृदय”, “काल-दीप”, और “दुनिया दीवानी” जैसे प्रतीक भावनात्मक तीव्रता, समय की क्षणभंगुरता और राष्ट्रीय गर्व को दर्शाते हैं ।
प्रश्न 10: कविता में दोहराव का क्या महत्व है?
उत्तर 10: “वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं” का दोहराव कविता के केंद्रीय संदेश को बल देता है, जो देश-प्रेम की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
पेज 4: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 3: “हम है जिसके राजा-रानी” — इस पंक्ति में ‘हम’ शब्द किसके लिए आया है?
उत्तर 3: देश के सभी प्राणियों के लिए।
विश्लेषण: यह पंक्ति देश के लोगों को “राजा-रानी” कहती है, जो देश की पहचान और इसके भविष्य के स्वामी हैं।
प्रश्न 4: कविता के अनुसार कैसा हृदय पत्थर के समान है?
उत्तर 4: जिसमें देश-प्रेम का भाव नहीं है।
विश्लेषण: कवि कहते हैं कि देश-प्रेम के बिना हृदय निर्जन और पत्थर जैसा है।
प्रश्न (ख): हो सकता है कि अपने समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार-विमर्श कीजिए कि अपने वे उत्तर ही क्यों चुने?
उत्तर (ख): मैंने उपरोक्त उत्तर इसलिए चुने:
- प्रश्न 3: “हम है जिसके राजा-रानी” में “हम” सभी प्राणियों को संदर्भित करता है, क्योंकि कविता देश को माता-पिता के रूप में दर्शाती है, जो सभी को पोषण देता है। अन्य विकल्प जैसे प्राकृतिक संसाधन या सामाजिक व्यवस्थाएँ संदर्भ के लिए पूर्ण नहीं हैं।
- प्रश्न 4: कविता स्पष्ट रूप से कहती है कि देश-प्रेम के बिना हृदय पत्थर है, इसलिए यह विकल्प सटीक है। साहस या प्रकृति की कमी कविता के मुख्य संदेश से मेल नहीं खाती।
विचार-विमर्श: मित्रों के साथ इन पंक्तियों के भाव और कविता के संदेश पर चर्चा की जा सकती है ताकि सभी की समझ स्पष्ट हो।
प्रश्न: मिलाकर करें मिलान
कॉलम 1 की पंक्तियों को कॉलम 2 के सही अर्थ से मिलाएँ:
- जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुँच सकेगा पार नहीं → 3. जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी कार्य को प्राप्त नहीं कर सकता।
- जो जीवित जोश जागा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं → 4. जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकता उसका जीवन निष्फल और अर्थहीन है।
- जिस पर गानी भी मस्त है, जिस पर है दुनिया दीवानी → 1. जिस देश की ज्ञान-बुद्धि से समूचा विश्व प्रभावित है।
- सब कुछ है अपने हाथों में, क्या ताप नहीं तलवार नहीं → 2. जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है।
विश्लेषण: मिलान पंक्तियों के संदर्भ और कविता के साहस, प्रेरणा, और वैश्विक प्रभाव के विषयों पर आधारित है ।
विचार-विमर्श के लिए
प्रश्न (क): “निश्चित है निःस्वार्थ निश्चित, है जान एक दिन जाने को। है काल-दीप जलता हृदय, जल जाना है पवनों को।”
उत्तर (क):
अर्थ: यह दोहा जीवन की क्षणभंगुरता और निःस्वार्थ कर्म की आवश्यकता को दर्शाता है। “निश्चित है निःस्वार्थ निश्चित, है जान एक दिन जाने को” का अर्थ है कि जीवन नश्वर है और निःस्वार्थ कर्म करना चाहिए। “है काल-दीप जलता हृदय, जल जाना है पवनों को” में समय को हृदय में जलते दीपक के रूप में चित्रित किया गया है, जो जीवन की गति को दर्शाता है।
विचार: यह पंक्ति मुझे देश के लिए निःस्वार्थ कार्य करने और समय की कीमत समझने की प्रेरणा देती है। समूह में चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि यह देश-प्रेम के साथ समयबद्ध कार्य की प्रेरणा देता है ।
प्रश्न (ख): “हम है जिसके राजा-रानी” — इस पंक्ति में राजा-रानी किसे और क्यों कहा गया है?
उत्तर (ख): “राजा-रानी” देश के सभी प्राणियों को कहा गया है क्योंकि देश उनकी माता-पिता के समान है, जो उन्हें जल-पानी और जीवन प्रदान करता है। वे देश के स्वामी हैं, जिनके हाथों में देश का भविष्य है ।
प्रश्न (ग): “संसार-संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति ‘संसार-संग’ नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं ले पाता है?”
उत्तर (ग): “संसार-संग चलना” का अर्थ विश्व के साथ प्रगति और परिवर्तन की गति में चलना है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वह समाज से पिछड़ जाता है, और उसका जीवन निष्फल हो जाता है, जिससे संसार उसकी उपेक्षा करता है ।
प्रश्न (घ): “उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं” — इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं?
उत्तर (घ): इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति मातृभूमि के प्रति संवेदनशील नहीं है, वह देश के लिए बोझ है। देश-प्रेम के बिना वह समाज या राष्ट्र के लिए योगदान नहीं देता ।
प्रश्न (ङ): कविता में देश-प्रेम के लिए वहाँ-सी बात आई है। आप “देश-प्रेम” में क्या समझते हैं?
उत्तर (ङ): कविता में देश-प्रेम को हृदय की संवेदना, साहस, और सामूहिक प्रगति के लिए कार्य करने के रूप में दर्शाया गया है। मेरे लिए देश-प्रेम का अर्थ है मातृभूमि की संस्कृति, संसाधनों, और लोगों के प्रति गर्व और समर्पण, साथ ही देश की बेहतरी के लिए सक्रिय योगदान ।
प्रश्न (च): यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश-प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएँ ढूँढिए और लिखिए।
उत्तर (च): रचना की अन्य विशेषताएँ:
- प्रेरणादायी स्वर: कविता जोश और उत्साह जगाती है।
- प्रतीकात्मक भाषा: “पत्थर हृदय” और “काल-दीप” भावनात्मक प्रभाव डालते हैं।
- लयबद्धता: दोहराव (“वह हृदय नहीं है पत्थर है”) कविता को प्रभावी बनाता है।
- सार्वभौमिक संदेश: सभी को देश के प्रति कर्तव्य के लिए प्रेरित करता है।
- संक्षिप्तता: संक्षिप्त पंक्तियों में गहरा संदेश देती है ।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में ‘है’ शब्द पहले आया है जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि ‘है’ का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह कैसी लगने लगेगी, जैसे…
उत्तर:
मूल पंक्तियाँ:
- जिस पर गानी भी मस्त है, जिस पर है दुनिया दीवानी।
पुनर्लिखित (“है” अंत में): - जिस पर गानी भी मस्त, जिस पर दुनिया दीवानी है।
सौंदर्य पर प्रभाव: मूल पंक्तियों में “है” की शुरुआती स्थिति लयात्मक प्रवाह बनाती है, जो कविता की संगीतमयता और भावनात्मक तीव्रता को बढ़ाती है। “है” को अंत में रखने से पंक्ति का लय टूटता है, और यह कम सामंजस्यपूर्ण लगती है।
उदाहरण विश्लेषण: - मूल: “जिस पर है दुनिया दीवानी” में उत्साहपूर्ण स्वर है।
- पुनर्लिखित: “जिस पर दुनिया दीवानी है” में स्वर समाप्ति पर केंद्रित हो जाता है, जो कम प्रभावी है।
साथियों के साथ चर्चा: मूल संरचना हिंदी काव्य की परंपरा के अनुरूप है, जहाँ क्रिया बीच में लय बनाए रखती है। पुनर्लिखित संस्करण कम आकर्षक लगता है।
प्रश्न: कविता में दिए कुछ शब्द नीचे तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों के लिए समानार्थी शब्द देखकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए।
उत्तर: दस्तावेज़ में विशिष्ट तालिका नहीं दी गई। कविता के सामान्य शब्दों के आधार पर संभावित समानार्थी:
- प्यार → प्रेम
- हृदय → दिल
- साहस → हिम्मत
- संसार → विश्व
- पत्थर → शिला
नोट: सटीक शब्दों के लिए तालिका प्रदान करें ।
अतिरिक्त नोट्स
- “स्वदेश प्रेम” के अंतर्गत कार्यों को चिह्नित करने का अभ्यास अधूरा है। पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति सम्मान, या राष्ट्रीय प्रगति में योगदान जैसे कार्य देश-प्रेम को दर्शाते हैं।
- “सब कुछ है अपने हाथों में, क्या ताप नहीं तलवार नहीं” व्यक्तिगत जिम्मेदारी को दर्शाता है, साहस और इच्छाशक्ति को प्रगति के लिए आवश्यक हथियार बताता है।
- “खादी गीत” आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गर्व के प्रतीक खादी को दर्शाता है, जो कविता के देश-प्रेम के विषय से मेल खाता है।
अध्याय 2-“दो गौरैया” और “मित्रलाभ” के नोट्स प्रश्न-उत्तर रूप में
“दो गौरैया”
प्रश्न 1: कहानी “दो गौरैया” का लेखक कौन है?
उत्तर 1: कहानी “दो गौरैया” के लेखक भीष्म साहनी हैं।
प्रश्न 2: कहानी का मुख्य विषय क्या है?
उत्तर 2: कहानी का मुख्य विषय मानव और प्रकृति के बीच संबंध, विशेष रूप से चिड़ियों के प्रति सहानुभूति और हास्यपूर्ण पारिवारिक गतिशीलता है। यह दर्शाता है कि कैसे प्रारंभिक असुविधा सहानुभूति में बदल सकती है।
प्रश्न 3: पिताजी को चिड़ियों से क्या परेशानी थी?
उत्तर 3: पिताजी को चिड़ियों के घोंसले और उनके शोर से परेशानी थी, क्योंकि वे घर को गंदा और अशांत करते थे। वे मानते थे कि वे घर के मालिक नहीं, बल्कि मेहमान हैं .
प्रश्न 4: माँ का चिड़ियों के प्रति दृष्टिकोण क्या था?
उत्तर 4: माँ चिड़ियों के प्रति सहानुभूति और हास्य का दृष्टिकोण रखती थीं। वे पिताजी के प्रयासों पर हँसती थीं और चिड़ियों को निकालने के बजाय उनके रहने की वकालत करती थीं ।
प्रश्न 5: कहानी में हास्य का उपयोग कैसे हुआ है?
उत्तर 5: हास्य माँ के व्यंग्यात्मक टिप्पणियों, पिताजी के अतिशयोक्तिपूर्ण प्रयासों (जैसे लाठी लेकर कूदना), और चिड़ियों के बार-बार लौटने से उत्पन्न होता है, जो स्थिति को हास्यास्पद बनाता है।
प्रश्न 6: पिताजी का व्यवहार अंत में कैसे बदलता है?
उत्तर 6: चिड़ियों के बच्चों को देखकर पिताजी का गुस्सा सहानुभूति में बदल जाता है। वे घोंसला तोड़ने से रुक जाते हैं और चिड़ियों को स्वीकार करते हुए मुस्कुराते हैं ।
प्रश्न 7: कहानी का नैतिक संदेश क्या है?
उत्तर 7: कहानी सिखाती है कि प्राकृतिक प्राणियों के प्रति सहानुभूति और धैर्य रखना चाहिए। छोटी असुविधाएँ भी समझ और करुणा से सुलझाई जा सकती हैं।
“मित्रलाभ”
प्रश्न 8: “पंचतंत्र” कहानी का लेखक कौन है?
उत्तर 8: “पंचतंत्र” की कहानी विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, हालाँकि यहाँ यह एक अंश के रूप में प्रस्तुत है।
प्रश्न 9: इस कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं?
उत्तर 9: मुख्य पात्र हैं: हिरण्यक (चूहा), लघुपतनक (कौआ), मणयक (हिरण), और चित्रांग (कछुआ)। ये सभी एक व्याध (शिकारी) से मुक्ति पाने के लिए एकजुट होते हैं।
प्रश्न 10: कहानी का मुख्य विषय क्या है?
उत्तर 10: कहानी मित्रता की शक्ति, बुद्धिमानी, और सहयोग को दर्शाती है। यह सिखाती है कि मित्र मिलकर किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं।
प्रश्न 11: हिरण्यक ने व्याध के जाल से अपने मित्रों को कैसे बचाया?
उत्तर 11: हिरण्यक ने अपने तेज दाँतों से जाल काटकर पहले चित्रांग, फिर लघुपतनक, और अंत में मणयक को मुक्त किया, जिससे सभी व्याध से बच गए।
प्रश्न 12: कहानी में व्याध का क्या हुआ?
उत्तर 12: व्याध को कोई शिकार नहीं मिला, और जब उसने मणयक को पकड़ा, तो चित्रांग की चालाकी और हिरण्यक की मदद से मणयक भी बच गया। व्याध निराश होकर चला गया।
प्रश्न 13: कहानी का नैतिक संदेश क्या है?
उत्तर 13: मित्रता में बड़ी शक्ति होती है। मित्रों को एक-दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और बुद्धि से किसी भी संकट से बचा जा सकता है।
अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर के सामने सही (✓) का निशान लगाएँ।
- पिताजी ने कहा कि घर साय बना हुआ है क्योंकि-
- घर की बनावट साय जैसी बहुत विशाल है
- घर में विभिन्न परिंदे और जल-जनु रहते हैं
- पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं (✓)
- घर में विभिन्न जीव-जंतु आते-जाते रहते हैं
विश्लेषण: पिताजी कहते हैं कि वे घर के मालिक नहीं, बल्कि मेहमान हैं, क्योंकि चिड़ियाँ और अन्य जीव घर में रहते हैं ।
- कहानी में ‘घर के असली मालिक’ किसे कहा गया है?
- माँ और पिताजी को जिनमें रहने की इच्छा थी
- लेखक को जिन्होंने यह कहानी लिखी
- जीव-जंतुओं को जो उसमें घर में रहते थे (✓)
- मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते थे
विश्लेषण: चिड़ियाँ और अन्य जीव-जंतु घर में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, इसलिए उन्हें असली मालिक कहा गया ।
- चिड़ियों के प्रवेश पर माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएँ क्या थीं?
- दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया
- पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया (✓)
- दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया
- माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया
विश्लेषण: पिताजी चिड़ियों को निकालना चाहते थे, लेकिन माँ ने हँसकर और व्यंग्य से उनका विरोध किया ।
- माँ बार-बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थीं, इससे क्या पता चलता है?
- माँ चाहती थीं कि चिड़ियाँ घर से भगाए न जाएँ (✓)
- माँ को पिताजी के उपाय नहीं भाते थे
- माँ को चिड़ियों को भगाने की गतिविधियों पर हँसी थी
- माँ को दूसरों पर हँसना और उपहास करना अच्छा लगता था
विश्लेषण: माँ का हँसना और मजाक करना दर्शाता है कि वे चिड़ियों के प्रति सहानुभूति रखती थीं और उन्हें भगाने के खिलाफ थीं ।
- कहानी में चिड़ियों के बार-बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है?
- दूसरों पर निर्भर रहना
- असफलताओं में हार मान लेना
- अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना (✓)
- सब कुछ छोड़कर कहीं और चले जाना
विश्लेषण: चिड़ियाँ बार-बार लौटती हैं, जो उनके अपने घर (घोंसले) के प्रति दृढ़ता और प्रयास को दर्शाता है ।
प्रश्न (ख): हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार-विमर्श कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?
उत्तर (ख): मैंने उपरोक्त उत्तर इसलिए चुने:
- प्रश्न 1: पिताजी का कहना कि वे मेहमान हैं, यह दर्शाता है कि जीव-जंतु घर के असली मालिक हैं। अन्य विकल्प कहानी के संदर्भ से मेल नहीं खाते।
- प्रश्न 2: चिड़ियाँ और जीव-जंतु घर में स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए वे असली मालिक हैं।
- प्रश्न 3: माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएँ विरोधाभासी थीं; पिताजी निकालना चाहते थे, माँ सहानुभूति दिखाती थीं।
- प्रश्न 4: माँ का मजाक चिड़ियों के प्रति उनकी सहानुभूति को दर्शाता है, न कि उपहास की आदत।
- प्रश्न 5: चिड़ियों का बार-बार लौटना दृढ़ता का प्रतीक है, जो कहानी में स्पष्ट है।
विचार-विमर्श: मित्रों के साथ चर्चा में, कहानी के हास्य, सहानुभूति, और चिड़ियों की दृढ़ता पर ध्यान देना चाहिए ताकि उत्तरों की समझ स्पष्ट हो ।
प्रश्न: मिलाकर करें मिलान
कॉलम 1 की पंक्तियों को कॉलम 2 के सही अर्थ से मिलाएँ:
- वह शोर मचाता है कि कानों के परदे फट जाएँ → 2. पिताजी का गुस्सा चिड़ियों की चहचहाहट से बढ़ जाता है, लेकिन लोग इसे संगीतमय समझते हैं।
- अंगन में आम का पेड़ ही सबसे सुंदर → 1. आम के पेड़ पर अलग-अलग पक्षी आकर चहचहाते हैं।
विश्लेषण: पहली पंक्ति पिताजी के गुस्से और चिड़ियों के शोर को दर्शाती है, जो दूसरों को संगीतमय लगता है। दूसरी पंक्ति आम के पेड़ को पक्षियों के आकर्षण का केंद्र बताती है।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: बदली कहानी
मन में आए कि घोंसले में अंडों से बच्चे न निकले होते, तो ऐसी में कहानी कैसे बढ़ती? यह बदली हुई कहानी लिखिए।
उत्तर: यदि घोंसले में अंडों से बच्चे न निकले होते, तो कहानी इस प्रकार होती:
पिताजी को चिड़ियों के शोर और गंदगी से परेशानी होती। वे लाठी लेकर घोंसला तोड़ने की कोशिश करते, और माँ फिर भी हँसकर उनका मजाक उड़ातीं। चिड़ियाँ बार-बार लौटतीं, लेकिन बिना बच्चों के, पिताजी का गुस्सा बढ़ता जाता। अंत में, वे घोंसला पूरी तरह तोड़ देते, और चिड़ियाँ हमेशा के लिए चली जातीं। माँ उदास होकर कहतीं, “अब घर सूना हो गया।” पिताजी को अपनी गलती का एहसास होता, लेकिन चिड़ियाँ लौटती नहीं। कहानी का अंत दुखद होता, जो सहानुभूति के बजाय पछतावे पर केंद्रित होता।
विश्लेषण: बच्चों की अनुपस्थिति कहानी को सहानुभूति से वंचित कर देती, और पिताजी का गुस्सा हावी रहता, जिससे नैतिक संदेश कमजोर पड़ता ।
प्रश्न: कहने के ढंग/क्रिया विशेषण
निम्नलिखित रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए।
(क) “पिताजी ने झिड़ककर कहा”, “तू खड़ा क्या देख रहा है”
(ख) “खीझ दी”, “खीझकर बोली माँ”
(ग) “किसी को सचमुच बाहर निकालना हो”, “उसका घर तोड़ देना चाहिए”, उन्होंने गुस्से में कहा।
अब आप इन मिलते-जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए।
उत्तर:
वाक्य निर्माण:
(क) झिड़ककर:
- शिक्षक ने झिड़ककर कहा, “तुम होमवर्क क्यों नहीं लाए?”
- भाई ने झिड़ककर बोला, “तू हमेशा मेरा सामान बिगाड़ता है!”
(ख) खीझकर: - माँ ने खीझकर कहा, “बार-बार एक ही बात क्यों पूछते हो?”
- दुकानदार ने खीझकर जवाब दिया, “यह सामान वापस नहीं होगा।”
(ग) गुस्से में: - पिताजी ने गुस्से में कहा, “यह काम अभी पूरा करो!”
- दोस्त ने गुस्से में चिल्लाया, “तुमने मेरा सामान क्यों छुआ?”
मिलते-जुलते क्रिया विशेषण और वाक्य:
- चिढ़कर:
- बहन ने चिढ़कर कहा, “तुम हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो?”
- बच्चे ने चिढ़कर बोला, “मुझे यह खेल पसंद नहीं!”
- हँसकर:
- दादी ने हँसकर कहा, “तुम्हारी शरारतें मुझे याद दिलाती हैं।”
- मित्र ने हँसकर बोला, “तू तो हर बार यही गलती करता है!”
- सहमकर:
- बच्चा सहमकर बोला, “मुझे अंधेरे से डर लगता है।”
- वह सहमकर पूछने लगा, “क्या यह सचमुच भूत था?”
विश्लेषण: ये क्रिया विशेषण भावनाओं को व्यक्त करते हैं और वाक्य को जीवंत बनाते हैं। कहानी में ये पात्रों के मनोभावों को उजागर करते हैं।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): आपको इस कहानी में ऐसी कौन-सी विशेषताएँ दिखाई देती हैं। उन्हें अपने पाठ्यपुस्तक के साथ मिलकर पढ़िए और उनकी सूची बनाइए।
उत्तर (क): कहानी की विशेषताएँ:
- हास्य: माँ का पिताजी के प्रयासों पर हँसना और व्यंग्य ।
- सहानुभूति: चिड़ियों के बच्चों के प्रति पिताजी का बदलता दृष्टिकोण ।
- प्रकृति के प्रति प्रेम: चिड़ियों को अंत में स्वीकार करना ।
- पारिवारिक गतिशीलता: माँ और पिताजी के बीच हास्यपूर्ण संवाद ।
- नैतिक संदेश: सहानुभूति और धैर्य का महत्व ।
प्रश्न (ख): इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है। इनके उदाहरण कहानी में से चुनकर लिखिए।
उत्तर (ख):
- किसी बात को कल्पना से बढ़ा-चढ़ाकर कहना:
- उदाहरण: “वह शोर मचाता है कि कानों के परदे फट जाएँ” ।
- विश्लेषण: चिड़ियों का शोर अतिशयोक्ति से वर्णित है।
- हास्य यानी हँसी-मजाक का उपयोग किया जाना:
- उदाहरण: माँ का कहना, “चिड़ियाँ एक-दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्या रहा है?”।
- विश्लेषण: माँ का व्यंग्य हास्य उत्पन्न करता है।
- सोचा कुछ और, हुआ कुछ और:
- उदाहरण: पिताजी चिड़ियों को भगाना चाहते थे, लेकिन बच्चों को देखकर उन्हें रहने दिया ।
- विश्लेषण: पिताजी का इरादा बदल गया।
- दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना:
- उदाहरण: माँ ने चिड़ियों के चहचहाने को उनके संवाद के रूप में अनुमानित किया ।
- विश्लेषण: माँ ने चिड़ियों के व्यवहार को मानवीय भावनाओं से जोड़ा।
- किसी की कही बात को उनके शब्दों में लिखना:
- उदाहरण: “छोड़ो जी, छोड़ो तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालो”।
- विश्लेषण: माँ के शब्द सीधे उद्धृत किए गए।
- किसी प्राणी या उसके कार्यों को कोई अन्य नाम देना:
- उदाहरण: चिड़ियों को “घर के असली मालिक” कहा गया ।
- विश्लेषण: यह उपमा चिड़ियों की स्वतंत्रता को दर्शाती है।
- किसने किससे कोई बात कही, यह साफ-साफ बताए बिना उस संवाद को लिखना:
- उदाहरण: “निकलेंगी कैसे नहीं?” पिताजी बोले ।
- विश्लेषण: संवाद संक्षिप्त और स्वाभाविक है।
प्रश्न (ग): आपकी बात
- “घर में चिड़ियाँ घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झाँककर देखा और दोनों एक साथ ‘ची-ची’ करने लगीं।” आपने अपने घर के आसपास चिड़ियों को कब-कब देखा है? उनके व्यवहार में आपको कौन-कौन से भाव दिखाई देते हैं?
उत्तर 1: मैंने अपने घर की बालकनी में चिड़ियाँ अक्सर देखी हैं, विशेष रूप से सुबह जब वे दाना चुगने आती हैं। उनके व्यवहार में उत्साह, सतर्कता, और सामाजिकता दिखती है। वे एक-दूसरे से चहचहाकर संवाद करती हैं, जो खुशी और समुदाय का भाव दर्शाता है। कभी-कभी खतरे पर वे तेजी से उड़ जाती हैं, जो डर और सावधानी को दिखाता है। - “अब घर में फिर से शोर होने लगा था, पर अबकी बार पिताजी उनकी ओर देख-देखकर केवल मुस्कुराते रहे।” कहानी के अंत में पिताजी चिड़ियों को अपने घर में स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या किसी अन्य जीव के साथ साझा करते हैं? उनके साथ व्यवहार में यदि कोई समस्या आती है, तो उसे कैसे सुलझाते हैं?
उत्तर 2: मैं अपने घर की छत पर गौरैया और कबूतरों के साथ स्थान साझा करता हूँ। वे वहाँ दाना चुगने और पानी पीने आते हैं। समस्या तब आती है जब वे गंदगी करते हैं। मैं इसे सुलझाने के लिए नियमित सफाई करता हूँ और उनके लिए अलग से दाना-पानी रखता हूँ, ताकि वे परेशान न हों। इससे सह-अस्तित्व आसान हो जाता है। - परिवार के लोग चिड़ियों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु चिड़ियों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो?
उत्तर 3: हाँ, एक बार मैं एक पड़ोसी से परेशान था क्योंकि वह जोर-जोर से बात करता था। लेकिन जब मैंने उनसे बात की, तो पता चला कि वे बहुत दयालु और मददगार हैं। उनकी मदद से मेरे परिवार ने एक कठिन समय में सहायता पाई। इससे मेरा उनके प्रति दृष्टिकोण बदल गया, और अब मैं उनकी आदतों को सहजता से स्वीकार करता हूँ।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): आपको इस कहानी में कौन-कौन से व्यंग्य प्रकट हुए हैं? उसे उद्धृत करके लिखिए।
उत्तर (क):
- उद्धरण: “छोड़ो जी, छोड़ो तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालो।”
- विश्लेषण: माँ का यह व्यंग्य पिताजी की असफलता पर हल्का उपहास है, जो उनकी कोशिशों को हास्यपूर्ण बनाता है।
- उद्धरण: “चिड़ियाँ एक-दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्या रहा है?”
- विश्लेषण: माँ ने पिताजी के कूदने और ताली बजाने को चिड़ियों के दृष्टिकोण से मजाकिया ढंग से प्रस्तुत किया।
- उद्धरण: “इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी। पंखा चला देते, तो ये उड़ जातीं।”
- विश्लेषण: माँ का यह कथन पिताजी के जटिल प्रयासों पर सरल समाधान सुझाकर व्यंग्य करता है।
प्रश्न (ख): अब इनमें से कौन-कौन से व्यंग्य “हास्य व्यंग्य” कहे जा सकते हैं? अब इन पर सही का निशान लगाइए।
उत्तर (ख):
- उपरोक्त सभी व्यंग्य हास्य व्यंग्य हैं, क्योंकि वे पिताजी की कोशिशों को हल्के-फुल्के और मजाकिया ढंग से प्रस्तुत करते हैं, बिना किसी को ठेस पहुँचाए।
- “छोड़ो जी, छोड़ो तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालो।” (✓)
- “चिड़ियाँ एक-दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्या रहा है?” (✓)
- “इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी। पंखा चला देते, तो ये उड़ जातीं।” (✓)
विश्लेषण: ये व्यंग्य हास्य उत्पन्न करते हैं और कहानी को मनोरंजक बनाते हैं ।
अध्याय 3-“एक आशीर्वाद” के नोट्स प्रश्न-उत्तर रूप में
कविता: एक आशीर्वाद (दुष्यंत कुमार)
प्रश्न 1: कविता “एक आशीर्वाद” का लेखक कौन है?
उत्तर 1: कविता “एक आशीर्वाद” के लेखक दुष्यंत कुमार हैं ।
प्रश्न 2: कविता का मुख्य विषय क्या है?
उत्तर 2: कविता का मुख्य विषय बड़े सपनों को पाने की प्रेरणा, चुनौतियों का सामना करना, और जीवन में उत्साह, हास्य, और गीत के साथ आगे बढ़ना है ।
प्रश्न 3: कविता में “बड़े सपने” का क्या अर्थ है?
उत्तर 3: “बड़े सपने” का अर्थ है महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। ये सपने कठिनाइयों को पार करके सत्य को प्राप्त करने की इच्छा को दर्शाते हैं (“तेरे स्वप्न बड़े हों”)।
प्रश्न 4: कविता में किन क्रियाओं का उल्लेख है जो सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं?
उत्तर 4: कविता में चलना, सीखना, मचलना, हँसना, मुस्कराना, गाना, ललचाना, और अँगली जलाना जैसी क्रियाएँ हैं, जो उत्साह और प्रयास को दर्शाती हैं ।
प्रश्न 5: “चाँद-तारों-सी आशाएँ सच्चाइयों के लिए” का क्या भाव है?
उत्तर 5: यह पंक्ति सच्चाई और उच्च लक्ष्यों के लिए असीम आकांक्षाएँ रखने की प्रेरणा देती है, जैसे चाँद और तारे जो ऊँचे और प्रेरक हैं ।
प्रश्न 6: कविता में “अँगली जलाएँ” का क्या अर्थ है?
उत्तर 6: “अँगली जलाएँ” का अर्थ है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना और कठिनाइयों का सामना करना, जैसे दीये की रोशनी के लिए पास जाना ।
प्रश्न 7: कविता का नैतिक संदेश क्या है?
उत्तर 7: कविता सिखाती है कि बड़े सपने देखने चाहिए, कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, और हँसते-गाते जीवन में आगे बढ़ना चाहिए ।
अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (केवल हिंदी में)
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर के सामने सही (✓) का निशान लगाएँ।
- “उँगली जलाएँ” पंक्ति में उँगली जलाने का भाव है-
- चुनौतियों को स्वीकार करना (✓)
- प्रकाश का प्रसार करना
- अपने के नाते का अनुभव करना
- कार्यों से नहीं घबराना
विश्लेषण: “उँगली जलाएँ” का अर्थ जोखिम उठाकर लक्ष्य की ओर बढ़ना है, जो चुनौतियों को स्वीकार करने से संबंधित है ।
- “अपने पाँवों पर खड़े हों” पंक्ति में क्या अर्थ है?
- अपने पैरों पर खड़े होना
- सफलता प्राप्त करना
- कठिनाइयों का सामना करना
- आत्मनिर्भर होना (✓)
विश्लेषण: यह पंक्ति आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को दर्शाती है, जो अपने पाँवों पर खड़े होने का प्रतीक है ।
प्रश्न (ख): हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार-विमर्श कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?
उत्तर (ख): मैंने उपरोक्त उत्तर इसलिए चुने:
- प्रश्न 1: “उँगली जलाएँ” चुनौतियों को स्वीकार करने का प्रतीक है, क्योंकि यह जोखिम लेने और लक्ष्य की ओर बढ़ने को दर्शाता है। अन्य विकल्प इस भाव से मेल नहीं खाते।
- प्रश्न 2: “अपने पाँवों पर खड़े हों” आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, जो कविता के संदेश का मुख्य हिस्सा है। अन्य विकल्प आंशिक रूप से सही हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता सबसे उपयुक्त है।
विचार-विमर्श: मित्रों के साथ चर्चा में, कविता के प्रेरणादायक स्वर और आत्मनिर्भरता पर जोर देना चाहिए। पंक्तियों के भावों को कविता के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है ।
प्रश्न: मिलाकर करें मिलान
कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ कॉलम 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदेश कॉलम 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव (संदेश) से मिलाएँ।
| क्रम | कॉलम 1 | कॉलम 2 |
|---|---|---|
| 1. | भावना की गाँठ से उतरकर जल्दी पृथ्वी पर चलना सीखें | 3. भावनाओं में न बहकर वास्तविकता का सामना करना |
| 2. | हर दीये की रोशनी देखकर ललचाएँ | 1. विभिन्न ज्ञान के उजाले की ओर आकर्षित होना और उसे पाने की ललक रखना |
| 3. | चाँद-तारों-सी आशाएँ सच्चाइयों के लिए स्वप्न-मचलना सीखें | 4. असम्भव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हट और प्रयास करना |
| 4. | हँसें-मुस्कराएँ-गाएँ | 2. सपनों को आधार और मुसीबतों में बाधाओं, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें |
विश्लेषण:
- पंक्ति 1 वास्तविकता में जीने की सीख देती है।
- पंक्ति 2 ज्ञान और लक्ष्यों की ओर आकर्षण को दर्शाती है।
- पंक्ति 3 उच्च आकांक्षाओं और सत्य की खोज को प्रेरित करती है।
- पंक्ति 4 जीवन में उत्साह और सकारात्मकता बनाए रखने की बात करती है।
प्रश्न: पंक्तियों पर चर्चा
पाठ से सुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। हँसें-मुस्कराएँ-गाएँ और इन पर विचार-विमर्श। आपने इनका क्या अर्थ समझा? अपने विचार अपने समूह में साझा करें और लिखें।
उत्तर:
पंक्ति: हँसें-मुस्कराएँ-गाएँ
अर्थ: यह पंक्ति जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। कठिन परिस्थितियों में भी हँसना, मुस्कराना, और गाना मनोबल को बनाए रखता है। यह सुझाव देता है कि हमें निराशा के बजाय आशावाद और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
चर्चा: समूह में इस पंक्ति पर चर्चा करते समय, हमने महसूस किया कि यह जीवन की चुनौतियों को हल्के ढंग से लेने और खुशी को अपनाने की सलाह देती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई परीक्षा में असफल हो, तो उसे हँसकर नई रणनीति बनानी चाहिए। यह पंक्ति हमें प्रेरित करती है कि जीवन को गीत की तरह जीवंत बनाएँ ।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: अनुमान और कल्पना से
अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए-
- कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन-कौन से हो सकते हैं और क्यों?
उत्तर 1: मेरे अनुसार बड़े सपने निम्नलिखित हो सकते हैं:
- वैज्ञानिक बनना: नई खोजों से दुनिया को बेहतर बनाना। यह सपना इसलिए बड़ा है क्योंकि यह समाज के लिए उपयोगी है।
- समाजसेवी बनना: गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। यह सपना इसलिए बड़ा है क्योंकि यह मानवता की सेवा करता है।
- खेल में विश्व चैंपियन बनना: देश का नाम रोशन करना। यह सपना मेहनत और समर्पण माँगता है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि बड़े सपने वे हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव लाते हैं। ये सपने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प की माँग करते हैं ।
- “हर दीये की रोशनी देखकर ललचाएँ/अँगली जलाएँ” पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या-क्या होना आवश्यक है और क्यों? (संकल्प, योजना, प्रयास आदि)
उत्तर 2: ललक के साथ निम्नलिखित आवश्यक हैं:
- संकल्प: दृढ़ निश्चय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देता है। बिना संकल्प के ललक कमजोर पड़ सकती है।
- योजना: लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट योजना बनाना जरूरी है, जैसे समय प्रबंधन और संसाधनों का उपयोग।
- प्रयास: निरंतर मेहनत और अभ्यास से ही सपने पूरे होते हैं।
- धैर्य: कठिनाइयों में हार न मानना और धैर्य रखना जरूरी है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि ललक तो प्रारंभिक प्रेरणा है, लेकिन संकल्प, योजना, और प्रयास इसे साकार करते हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर बनने की ललक के साथ पढ़ाई की योजना और मेहनत जरूरी है।
- कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है। आपको उससे बातचीत करनी हो तो क्या बात करेंगे?
उत्तर 3: यदि मेरा सपना (वैज्ञानिक बनना) मेरा मित्र हो, तो मैं उससे कहूँगा:
- “तू मुझे हर दिन प्रेरित करता है, लेकिन रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को कैसे पार करूँ?”
- “मुझे कौन-से कौशल सीखने चाहिए ताकि तुझे जल्दी पा सकूँ?”
- “जब मैं हताश हो जाऊँ, तो मुझे उत्साहित करने के लिए क्या करूँ?”
चर्चा: समूह में हमने माना कि सपने से बातचीत हमें आत्म-मंथन करने और लक्ष्य की ओर स्पष्टता पाने में मदद करती है। यह हमें प्रेरणा और दिशा देता है।
- यदि आप किसी के आशीर्वाद देना चाहते हों तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों?
उत्तर 4: मैं अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दूँगा:
- आशीर्वाद: “तुझे हमेशा बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शक्ति मिले।”
- क्यों: वह अभी युवा है और उसके पास असीम संभावनाएँ हैं। यह आशीर्वाद उसे प्रेरित करेगा कि वह कठिनाइयों से न डरे और अपने लक्ष्यों को पाए।
चर्चा: समूह में हमने माना कि आशीर्वाद प्रेरणा और सकारात्मकता का स्रोत है। यह दूसरों को आत्मविश्वास देता है ।
प्रश्न (क): कविता की रचना
इस कविता में सपने को चलने, मुस्कराने, गाने हुए बताया गया है। इस प्रकार की अन्य विशेषताएँ जो इस कविता में इस प्रकार दिखाई देती हैं, उन्हें लिखें और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए।
उत्तर (क): कविता में सपने की अन्य विशेषताएँ:
- सपने प्रेरक हैं: “तेरे स्वप्न बड़े हों” सपनों को महत्वाकांक्षी और प्रेरणादायक बनाता है।
- सपने जोखिम माँगते हैं: “अँगली जलाएँ” जोखिम और मेहनत की आवश्यकता को दर्शाता है।
- सपने गतिशील हैं: “चलना सीखें, मचलना सीखें” सपनों को गतिशील और सक्रिय बनाता है।
- सपने सकारात्मकता लाते हैं: “हँसें-मुस्कराएँ-गाएँ” जीवन में उत्साह और खुशी जोड़ता है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि ये विशेषताएँ सपनों को जीवंत और मानवीय बनाती हैं। सपने केवल विचार नहीं, बल्कि एक मित्र की तरह मार्गदर्शन करते हैं ।
प्रश्न (ख): सृजन
इस कविता के आधार पर एक मज़ेदार शब्द है, स्वप्न। इस शब्द को केंद्र में रखकर एक कविता बनाएँ जिसमें विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी कविता बनाकर कक्षा में सुनाएँ।
उत्तर (ख):
स्वप्न को
देखते देखा है,
चलते देखा है,
उड़ते देखा है,
गाते देखा है,
स्वप्न को
रोशनी बनते देखा है,
सपनों को सच करते देखा है।
विश्लेषण: यह कविता स्वप्न को गतिशील, प्रेरक, और सकारात्मक बनाती है, जैसा कि मूल कविता में है। विभिन्न क्रियाएँ स्वप्न की जीवंतता को दर्शाती हैं ।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: कविता का शीर्षक
कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है जो कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। यदि इस कविता की थीम या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन-सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों?
उत्तर:
शीर्षक: “तेरे स्वप्न बड़े हों”
क्यों: यह पंक्ति कविता का केंद्रीय विचार है, जो बड़े सपनों को देखने और उन्हें पाने की प्रेरणा देती है। यह कविता के प्रेरणादायक और आशीर्वादपूर्ण स्वर को पूरी तरह दर्शाता है।
प्रश्न: भाषा की बात
- नीचे दिए गए रिक्त स्थान में ‘पृथ्वी’ से शुरू होने वाले शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखें।
उत्तर 1:
- पृथ्वी
- पृथ्वीपति
- पृथ्वीतल
- पृथ्वीवासी
- पृथ्वीगोल
विश्लेषण: ये शब्द पृथ्वी से संबंधित हैं और कविता के संदर्भ में वास्तविकता को दर्शाते हैं। समूह में चर्चा से और भी शब्द मिल सकते हैं ।
- कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर चर्चा बनाएँ जो समान अर्थ देते हों।
| शब्द | अन्य शब्द | समान अर्थ वाले शब्द |
|---|---|---|
| पृथ्वी | धरा, वसुधा, अकृति, सुता | धरा, वसुधा |
| चाँद | मधुकर, सूरि, निवारक, मयंक | मयंक |
| तारे | तथन, संग, तारक, उद्धरण | तारक |
| रोशनी | प्रकाश, लतिमा, उज्ज्वलता, आलोक | प्रकाश, उज्ज्वलता, आलोक |
| स्थान | स्थान, इच्छा, यथार्थ, कल्पना | यथार्थ |
| दिया | दीप, ज्योति, दीपक, प्रदीप | दीप, दीपक, प्रदीप |
विश्लेषण:
- पृथ्वी: धरा और वसुधा पृथ्वी के पर्यायवाची हैं।
- चाँद: मयंक चाँद का पर्यायवाची है।
- तारे: तारक तारों का पर्यायवाची है।
- रोशनी: प्रकाश, उज्ज्वलता, और आलोक समान अर्थ देते हैं।
- स्थान: यथार्थ स्थान के संदर्भ में उपयुक्त है।
- दिया: दीप, दीपक, और प्रदीप समान अर्थ वाले हैं।
प्रश्न: आना-जाना
‘आना’ और ‘जाना’ दो महत्वपूर्ण क्रियाएँ हैं। कक्षा में दो समूह बनाएँ। एक समूह का नाम ‘आना’ और दूसरे समूह का नाम ‘जाना’ होगा। अब अपने-अपने समूह में दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य बनाएँ और उन्हें चार्ट पर चिपकाकर अपनी कक्षा में लगाएँ।
उत्तर:
‘आना’ समूह के वाक्य:
- मैं रोज सुबह स्कूल आता हूँ।
- मेरे दोस्त मेरे घर खेलने आए।
- बारिश के बाद धूप फिर से आई।
‘जाना’ समूह के वाक्य:
- मैं हर रविवार बाजार जाता हूँ।
- वह अपने गाँव छुट्टियों में गया।
- हमें सपनों को पूरा करने के लिए आगे जाना होगा।
विश्लेषण: ये वाक्य रोजमर्रा के जीवन और कविता के प्रेरणादायक संदर्भ को दर्शाते हैं। इन्हें चार्ट पर लिखकर कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: हँसें-मुस्कराएँ-गाएँ
अपने किसी एक दिन की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दीजिए और अपनी डायरी में लिखें कि आप दिनभर में कब-कब हँसे, कब-कब मुस्कराए, कब-कब गाए, कब-कब ललचाए?
उत्तर:
डायरी प्रविष्टि:
आज सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल में हँसा जब उन्होंने एक मजेदार चुटकुला सुनाया। दोपहर में शिक्षक ने मेरी प्रशंसा की, तो मैं मुस्कराया। शाम को मैंने अपने पसंदीदा गाने को गुनगुनाया, जिससे मन खुश हुआ। रात में माँ ने मेरे पसंदीदा भोजन की तस्वीर दिखाई, तो मैं उसकी ओर ललचाया।
विश्लेषण: यह गतिविधि कविता के सकारात्मक स्वर को जीवन से जोड़ती है, जो हँसने, मुस्कराने, और गाने की प्रेरणा देती है।
प्रश्न: पाठ से आगे
- कविता के माध्यम से बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने का आशीर्वाद दिया गया है। दिन-प्रतिदिन के जीवन में आपको अपने माता-पिता, अध्यापक एवं परिजनों से किस तरह के आशीर्वाद मिलते हैं? अपनी लेखन पुस्तिका में लिखें।
उत्तर 1: मेरे माता-पिता मुझे आशीर्वाद देते हैं कि मैं पढ़ाई में मेहनत करूँ और एक अच्छा इंसान बनूँ। मेरे अध्यापक मुझे आशीर्वाद देते हैं कि मैं हमेशा सीखता रहूँ और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करूँ। मेरे दादाजी कहते हैं, “हमेशा सच बोलो और दूसरों की मदद करो।” ये आशीर्वाद मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ूँ। - आप भी अपने से छोटों के प्रति किन्हीं न किसी प्रकार की शुभेच्छा प्रकट करें- उन्हें लिखें।
उत्तर 2: मेरे छोटे भाई के लिए:
- “तुझे हमेशा खुश रहने और अपने सपनों को पाने की शक्ति मिले।”
- “हर कठिनाई में हँसते-मुस्कराते रहो।”
विश्लेषण: ये शुभेच्छाएँ कविता के आशीर्वादपूर्ण स्वर को दर्शाती हैं और छोटों को प्रेरित करती हैं ।
प्रश्न: सपनों की बातें
आप क्या हँसना चाहते हैं और क्या गाना चाहते हैं? उन्हें एक पर्ची पर लिखें। पर्ची पर अपना नाम लिखना आवश्यक नहीं है। अपने अध्यापक द्वारा दी गई डिब्बे में अपनी-अपनी पर्चियों को डाल दें। अध्यापक एक-एक करके इन पर्चियों को निकालकर सुनाएँ। सभी विद्यार्थी अपने-अपने सुझाव दें कि उन सपनों को पूरा करने के लिए-
- किस तरह के प्रयास करने होंगे?
- किस तरह से योजना बनानी होगी?
- किससे और किस प्रकार का सहयोग लिया जा सकता है?
- लक्ष्य-प्राप्ति में सम्भावित चुनौतियाँ कौन-कौन सी हो सकती हैं?
उत्तर:
पर्ची पर लिखा सपना: मैं हँसना चाहता हूँ जब मैं एक वैज्ञानिक बनूँ और गाना चाहता हूँ जब मेरी खोज दुनिया को बेहतर बनाए।
सुझाव:
- प्रयास: नियमित पढ़ाई, विज्ञान की किताबें पढ़ना, और प्रयोगशाला में अभ्यास करना।
- योजना: समय प्रबंधन, जैसे रोज 2 घंटे विज्ञान पढ़ना और सप्ताह में एक बार नए प्रयोग करना।
- सहयोग: शिक्षकों से मार्गदर्शन, माता-पिता से प्रोत्साहन, और वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेना।
- चुनौतियाँ: समय की कमी, जटिल विषयों को समझने में कठिनाई, और संसाधनों की सीमित उपलब्धता।
विश्लेषण: यह गतिविधि कविता के सपनों को वास्तविकता से जोड़ती है और व्यावहारिक योजना बनाने की प्रेरणा देती है।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: हमारे सपने
अपने माता-पिता या अभिभावक आपकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को जानते-समझते हैं। वे उन्हें पूरा करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न करते हैं। अपने माता-पिता या अभिभावक से उनके द्वारा देखे गए सपने और इच्छाओं के बारे में पूछिए कि वे क्या-क्या करना चाहते थे या चाहते हैं? तालिका में उन सपनों को लिखिए।
उत्तर:
| नाम | सपने और इच्छाएँ |
|---|---|
| माता | समाजसेवा करना और एक स्कूल खोलना ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। |
| पिता | एक सफल व्यवसायी बनना और परिवार को हर सुख देना। |
विश्लेषण: माता-पिता से बात करने पर पता चला कि उनके सपने समाज और परिवार की भलाई से जुड़े हैं। यह गतिविधि हमें उनके सपनों को समझने और उनकी प्रेरणा लेने का अवसर देती है ।
अध्याय 4-“हरिद्वार की यात्रा” के नोट्स प्रश्न-उत्तर रूप में
लेखक: भारतेंदु हरिश्चंद्र
प्रश्न 1: लेखक कौन हैं और उन्होंने कब हरिद्वार की यात्रा की?
उत्तर 1: लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और उन्होंने 1871 में हरिद्वार की यात्रा की ।
प्रश्न 2: लेखक ने हरिद्वार के बारे में क्या कहा?
उत्तर 2: लेखक ने हरिद्वार को प्राकृतिक सौंदर्य, पवित्रता, और शांति से भरा स्थान बताया। यहाँ की गंगा, सुगंधित हवा, और प्रकृति लोगों को आनंद देती है। यहाँ झगड़े का नाम तक नहीं है।
प्रश्न 3: लेखक के अनुसार हरिद्वार की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर 3: हरिद्वार की विशेषताएँ:
- प्राकृतिक सौंदर्य: तीन ओर से पर्वतों से घिरा, गंगा का तट।
- पवित्रता और शांति: यहाँ वैराग्य और भक्ति का उदय होता है।
- सुगंधित वातावरण: हवा में विलायती गुलाब, चमेली आदि की सुगंध।
- आत्मनिर्भरता: यहाँ के लोग सज्जन और आत्मनिर्भर हैं।
प्रश्न 4: लेखक ने शिक्षा के बारे में क्या विचार व्यक्त किए?
उत्तर 4: लेखक का मानना है कि शिक्षा की पूरी व्यवस्था से ही समाज की प्रगति संभव है।
प्रश्न 5: हरिद्वार में भोजन का अनुभव कैसा था?
उत्तर 5: लेखक ने कहा कि पत्थर पर किया गया भोजन सोने की थाल के भोजन से भी अधिक सुखद था, क्योंकि यह प्रकृति के बीच और शांत वातावरण में था।
प्रश्न 6: लेखक ने हरिद्वार को क्यों तीर्थस्थल माना?
उत्तर 6: हरिद्वार को तीर्थस्थल माना क्योंकि यहाँ गंगा का पवित्र जल, सुगंधित हवा, और शांत वातावरण है। यहाँ भक्ति और वैराग्य का माहौल है, जो मन को शांति देता है।
प्रश्न 7: लेखक का पत्र किसे संबोधित था और क्यों?
उत्तर 7: लेखक ने पत्र संपादक महोदय को संबोधित किया, ताकि उनके पाठकों को हरिद्वार के गुणों का वर्णन पढ़कर प्रेरणा मिले और वे इसे तीर्थस्थल के रूप में स्वीकार करें।
अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (केवल हिंदी में)
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर के सामने सही (✓) का निशान लगाएँ।
- “सज्जन ऐसे कि पलट मारने से फल देने हैं” का क्या अर्थ है?
- लेखक के अनुसार सज्जन लोग उदार होना शुरू से ही चाहते हैं (✓)
- लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को भावनात्मक रूप में व्यक्त कर रहे हैं
- लेखक का मानना है कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत उदार हैं
- लेखक का पलट मारने से केवल एक पल नष्ट करना पसंद था
विश्लेषण: यह पंक्ति हरिद्वार के लोगों की उदारता को दर्शाती है, जो स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करते हैं।
- “वैराग्य और भक्ति का उदय होता था” इस कथन से लेखक का कौन-सा भाव प्रकट होता है?
- शारीरिक शांति और मानसिक सबलता
- आध्यात्मिक सुख और मानसिक विकास
- मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभूति (✓)
- सामाजिक समृद्धि और पारलौकिक प्रेम
विश्लेषण: यह कथन हरिद्वार के आध्यात्मिक माहौल को दर्शाता है, जो मन को शांति और भक्ति की ओर ले जाता है।
- “पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था” इस वाक्य का सार्थक अनुभव निकाला गया है:
- समृद्धि में सुख होता है
- सुखी होने पत्थर पर भोजन करते हैं
- लेखक के पास सोने की थाल नहीं थी
- पत्थर पर किया भोजन अधिक सुखद था (✓)
विश्लेषण: प्रकृति के बीच भोजन का सुख सोने की थाल से अधिक था, क्योंकि यह शांति और प्राकृतिक वातावरण से जुड़ा था।
- “एक दिल में भी भागवत जी के तट पर स्नान करके पत्थर पर जल के अंजलि निकट पहुँचकर भोजन किया” यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है?
- अंधविश्वास और लालच
- मानवता और देशप्रेम
- सादगी और आत्मनिर्भरता (✓)
- स्वच्छता और प्रकृति प्रेम
विश्लेषण: यह प्रसंग प्रकृति के साथ सादगी और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।
- लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था?
- राजनीतिक
- आध्यात्मिक (✓)
- सामाजिक
- प्राकृतिक
विश्लेषण: हरिद्वार का अनुभव आध्यात्मिक था, क्योंकि यहाँ भक्ति और वैराग्य का माहौल था।
- पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है?
- कठिन शब्दों का प्रयोग और जटिलता
- मुहावरों का अधिक प्रयोग
- सरलता और सौम्यता (✓)
- जटिलता और संक्षिप्तता
विश्लेषण: पत्र की भाषा सरल और सौम्य है, जो पाठकों को आसानी से समझ आती है।
प्रश्न (ख): हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार-विमर्श कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?
उत्तर (ख): मैंने उपरोक्त उत्तर इसलिए चुने:
- प्रश्न 1: “सज्जन ऐसे कि पलट मारने से फल देने हैं” लोगों की उदारता को दर्शाता है, जो स्वाभाविक रूप से मदद करते हैं।
- प्रश्न 2: “वैराग्य और भक्ति” आध्यात्मिक शांति और भक्ति को दर्शाता है, जो हरिद्वार की विशेषता है।
- प्रश्न 3: पत्थर पर भोजन का सुख प्रकृति के साथ जुड़ाव से आता है, न कि भौतिक समृद्धि से।
- प्रश्न 4: यह प्रसंग सादगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, जो प्रकृति के बीच भोजन से स्पष्ट है।
- प्रश्न 5: हरिद्वार का अनुभव आध्यात्मिक है, क्योंकि यहाँ भक्ति और शांति का माहौल है।
- प्रश्न 6: पत्र की भाषा सरल और सौम्य है, जो पाठकों को प्रेरित करती है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि हरिद्वार का आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व इन उत्तरों को सही बनाता है।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: मिलकर करें मिलान
पत्र से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। आपस में चर्चा कीजिए और उनके अनुरूप समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए।
उत्तर: OCR में इस खंड के लिए स्पष्ट शब्द और समानार्थी नहीं दिए गए हैं। हालांकि, सामान्य शब्दों के आधार पर एक उदाहरण:
| शब्द | समानार्थी शब्द |
|---|---|
| गंगा | भागीरथी, सुरसरि |
| पवित्रता | शुद्धता, निर्मलता |
| सज्जन | भद्र, उदार |
| भक्ति | श्रद्धा, उपासना |
विश्लेषण: ये शब्द पत्र के संदर्भ में हरिद्वार की विशेषताओं को दर्शाते हैं। समूह में चर्चा से और शब्द जोड़े जा सकते हैं।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): पंक्तियों पर चर्चा
पत्र से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए।
- पंक्ति: “अच्छी की क्या साइसे विलक्षण होती है जिसमें से विलायती, जावित्री आदि की अच्छी सुगंध आती है मानो वह प्रत्यक्ष प्रगट होता है कि यह ऐसी गुणमयी है कि यहाँ की थाल भी ऐसी गुणमयी है!”
अर्थ: यह पंक्ति हरिद्वार की हवा की सुगंध और पवित्रता को दर्शाती है। विलायती गुलाब और जावित्री जैसी सुगंध हवा को विशेष बनाती है, जो प्रकृति की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से दिखाती है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि यह पंक्ति हरिद्वार के प्राकृतिक सौंदर्य और शुद्धता को उजागर करती है। यहाँ की हवा मन को शांति देती है । - पंक्ति: “अहा! इस जम में भी धाय है जिनसे अच्छी किल्लियाँ जाते हैं। चल, फूल, गूल, गंगा, पते, घाट, बीज, लकड़ी और गाय, यहाँ तक कि जल में भी कोयले और गाय से लोगों का मनोहन पूर्ण करते हैं!”
अर्थ: यह पंक्ति हरिद्वार की प्राकृतिक और आध्यात्मिक संपदा को दर्शाती है। यहाँ के फल, फूल, गंगा, और अन्य प्राकृतिक तत्व लोगों के मन को आनंदित करते हैं।
चर्चा: समूह में हमने माना कि यह पंक्ति हरिद्वार की समृद्धि और प्रकृति के साथ जुड़ाव को दिखाती है। यहाँ की हर चीज मन को मोह लेती है ।
प्रश्न (ख): सोच-विचार के लिए
- पंक्ति: “और संपादक महोदय, मैं चित से तो अब तक वहाँ निवास करता है…”
प्रश्न: लेखक का यह वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? कब-कब?
उत्तर:
अर्थ: लेखक का यह वाक्य दर्शाता है कि हरिद्वार की शांति और सौंदर्य ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा, और वे मानसिक रूप से वहाँ रह रहे हैं।
अनुभव: हाँ, मैंने अपने गाँव की यात्रा के दौरान ऐसा अनुभव किया। वहाँ की शांति और प्रकृति ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं बार-बार वहाँ लौटने की सोचता हूँ।
विश्लेषण: यह पंक्ति हरिद्वार के स्थायी प्रभाव को दर्शाती है। - प्रश्न: किन-किन स्थान से लौटने के बाद भी उनके लिए मन में मोहन रहता है?
उत्तर: मेरे लिए निम्नलिखित स्थान ऐसे हैं:
- हिमाचल प्रदेश: वहाँ की पहाड़ियाँ और शांति मन को मोह लेती हैं।
- मेरे गाँव का तालाब: वहाँ की शांति और प्रकृति मुझे हमेशा याद रहती है।
विश्लेषण: हरिद्वार जैसे स्थान अपने सौंदर्य और शांति के कारण मन में बसे रहते हैं।
- पंक्ति: “मुझे भी यदि वह विलक्षण सौभाग्य हो एक ऐसे को लेखक लिखने मान लेते हैं।”
प्रश्न: लेखक का यह कथन आपके सामने में कितना सत्य है? क्या आप भी ऐसे सौभाग्यशाली लोगों से मिलते हैं? उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तर:
अर्थ: लेखक कहते हैं कि हरिद्वार जैसे स्थान का वर्णन करना सौभाग्य की बात है।
सत्यता: यह कथन सत्य है, क्योंकि प्रकृति और आध्यात्मिक स्थानों का वर्णन मन को प्रेरित करता है।
उदाहरण: मेरे शिक्षक ने एक बार हिमालय की यात्रा का वर्णन किया, जिससे मुझे लगा कि मैं वहाँ गया हूँ। ऐसे लोग जो अपने अनुभव साझा करते हैं, सौभाग्यशाली हैं।
विश्लेषण: यह पंक्ति अनुभव साझा करने की शक्ति को दर्शाती है। - प्रश्न: आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को “टिकने योग्य” क्यों कहा? उस स्थान में कौन-कौन सी विशेषताएँ होंगी जो उसे टिकने योग्य मनोहन हों?
उत्तर:
क्यों टिकने योग्य: लेखक ने हरिद्वार को टिकने योग्य कहा क्योंकि यहाँ शांति, पवित्रता, और प्राकृतिक सौंदर्य है।
विशेषताएँ:
- गंगा का पवित्र जल।
- सुगंधित हवा और प्राकृतिक वातावरण।
- भक्ति और वैराग्य का माहौल।
- लोगों की उदारता और आत्मनिर्भरता।
विश्लेषण: ये विशेषताएँ हरिद्वार को मनोहन बनाती हैं।
- पंक्ति: “फल, फूल, गूल, गंगा, पते, घाट, बीज, लकड़ी और गाय, यहाँ तक कि जल में भी कोयले और गाय से लोगों का मनोहन पूर्ण करते हैं।”
प्रश्न: इस वाक्य के माध्यम से आपको सुख के बारे में कौन-कौन सी बातें सूझ रही हैं?
उत्तर:
सुख की बातें:
- प्रकृति का सान्निध्य सुख देता है।
- सादगी और शांति मन को आनंदित करती है।
- प्राकृतिक तत्व जैसे फल, फूल, और गंगा मन को मोहते हैं।
- हरिद्वार का वातावरण आत्मिक सुख प्रदान करता है।
विश्लेषण: यह पंक्ति प्रकृति और सादगी से मिलने वाले सुख को दर्शाती है।
प्रश्न (ग): अनुमान और कल्पना से
- पंक्ति: “यह भूमि तीन ओर सुदूर हो-देरे पर्वतों से घिरी है…”
प्रश्न: कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं। आप वहाँ क्या-क्या करना चाहेंगे?
उत्तर: मैं हरिद्वार में निम्नलिखित करना चाहूँगा:
- गंगा के तट पर स्नान करना और ध्यान करना।
- हर की पौड़ी पर गंगा आरती देखना।
- पास के पर्वतों पर ट्रेकिंग करना।
- स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेना।
विश्लेषण: हरिद्वार का प्राकृतिक और आध्यात्मिक माहौल इन गतिविधियों को प्रेरित करता है।
अभ्यास प्रश्न
- पंक्ति: “जल के चलने पास ही ठे-ठे-ठे आते थे।”
प्रश्न: कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर हैं और पानी के छींटे आपके मुँह पर आ रहे हैं। अपने अनुभव को अपनी कल्पना से लिखिए।
उत्तर: मैं गंगा के तट पर खड़ा हूँ। ठंडे पानी के छींटे मेरे चेहरे पर पड़ रहे हैं, जो मन को शीतलता दे रहे हैं। गंगा की लहरों की आवाज और हवा की सुगंध मन को शांत करती है। मैं महसूस करता हूँ कि मेरे सारे तनाव बह गए हैं। यह अनुभव मुझे प्रकृति के करीब लाता है।
विश्लेषण: यह कल्पना हरिद्वार के शांत और पवित्र वातावरण को दर्शाती है। - पंक्ति: “सज्जन ऐसे कि पलट मारने से फल देने हैं।”
प्रश्न: यदि पेड़-पौधे सचमुच मज्जनों की तरह व्यवहार करने लगें तो क्या होगा?
उत्तर: यदि पेड़-पौधे सज्जनों की तरह व्यवहार करें, तो:
- वे बिना माँगे फल, फूल, और छाया देंगे।
- पर्यावरण और शुद्ध रहेगा, क्योंकि पेड़ स्वयं अपनी देखभाल करेंगे।
- लोग प्रकृति से और अधिक प्रेम करेंगे।
विश्लेषण: यह कल्पना प्रकृति की उदारता और हरिद्वार के लोगों की सज्जनता को जोड़ती है।
- पंक्ति: “पत्थर पर का भोजन जो सुख दिया वह…”
प्रश्न: इस पत्र में गंगा जी के साथ “हैं” और जी-लगाकर गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा?
उत्तर: लेखक ने गंगा जी के साथ “हैं” और “जी” का प्रयोग आदर और पवित्रता दर्शाने के लिए किया। गंगा को भारत में माता और पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए बहुवचन और “जी” का प्रयोग सम्मान प्रकट करता है।
विश्लेषण: यह भाषा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उपयोग है। - प्रश्न: कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार एक अंधविश्वासित या दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ गए हैं। उनकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए।
उत्तर: सुझाव:
- उनकी सहायता के लिए हमेशा साथ रहें और गंगा तट तक सुरक्षित ले जाएँ।
- गंगा आरती की ध्वनि और सुगंध का वर्णन करें।
- उनके लिए स्थानीय कहानियाँ और हरिद्वार का महत्व बताएँ।
- आरामदायक स्थान पर बैठकर उन्हें प्रकृति की अनुभूति कराएँ।
विश्लेषण: ये सुझाव उनकी यात्रा को स्मरणीय और आध्यात्मिक बनाएंगे।
- प्रश्न: “मेरे साथ काल्लू जी भी परमानंद थे।” लेखक और काल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा का एक काल्पनिक संवाद लिखिए।
उत्तर:
लेखक: काल्लू जी, यह गंगा का तट कितना शांत है!
काल्लू जी: हाँ, हरिश्चंद्र जी, यहाँ की हवा में सुगंध और मन में शांति है।
लेखक: यहाँ का भोजन पत्थर पर भी सोने की थाल से बढ़कर है।
काल्लू जी: बिल्कुल! यहाँ की सादगी और प्रकृति का सान्निध्य अनमोल है।
विश्लेषण: यह संवाद हरिद्वार के सौंदर्य और शांति को दर्शाता है। - पंक्ति: “यह भूमि तीन ओर सुदूर हो-देरे पर्वतों से घिरी है।”
प्रश्न: लेखक और प्रकृति के बीच एक काल्पनिक संवाद तैयार कीजिए- जैसे पर्वत बोल रहे हों।
उत्तर:
लेखक: हे पर्वत, तुम हरिद्वार को इतना सुंदर क्यों बनाते हो?
पर्वत: मैं गंगा को अपनी गोद में सजाता हूँ ताकि लोग शांति पाएँ।
लेखक: तुम्हारी शांति और विशालता मन को मोह लेती है।
पर्वत: मेरी चोटियाँ और गंगा की लहरें मिलकर भक्ति का गीत गाती हैं।
विश्लेषण: यह संवाद प्रकृति और मानव के बीच गहरा संबंध दर्शाता है। - प्रश्न: ‘है’ और ‘हैं’ का उपयोग। गंगा शब्द एकवचन है, फिर भी इसके साथ ‘हैं’ का प्रयोग क्यों?
उत्तर: गंगा के साथ ‘हैं’ का प्रयोग आदर और सांस्कृतिक महत्व के कारण किया गया है। गंगा को माता माना जाता है, और बहुवचन का प्रयोग सम्मान दर्शाता है। उदाहरण:
- “गंगा जी हमारी माता हैं।”
- “भारत के प्राचीन मंदिर सुंदर हैं।”
विश्लेषण: यह भाषा का सांस्कृतिक उपयोग है, जो आदर प्रदर्शित करता है।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: अब ‘आदरार्थी बहुवचन’ को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
उत्तर:
- प्राचार्य जी विद्यालय में नहीं हैं, वे अभी समारोह में उपस्थित हैं।
- माता-पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए।
- मेरी बहन बाजार जा रही है, वहाँ से किताबें ले आएगी।
- बाहर फेरीवाला है, उसे बुला लीजिए।
- डाकिया जी आए हैं, उन्हें भी बुला लीजिए।
- आप तो बहुत दिन बाद आए हैं, आपका स्वागत है।
- डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए।
- आपके माता-पिता कहाँ हैं? काम में व्यस्त हैं।
विश्लेषण: आदरार्थी बहुवचन का प्रयोग सम्मान दर्शाने के लिए किया गया है।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): काल की पहचान
पंक्ति: “यहाँ हर की पौड़ी नामक एक पवित्र घाट है और यहाँ स्नान भी होता है।”
प्रश्न: नीचे दी गई पत्र की इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए, इनमें दिया कौन-सा काल प्रदर्शित कर रहा है?
उत्तर:
- निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान देंगे। – भविष्य काल
- यह भूमि तीन ओर सुदूर हो-देरे पर्वतों से घिरी है। – वर्तमान काल
- सज्जन ऐसे कि पलट मारने से फल देने हैं। – वर्तमान काल
- पत्र में वैराग्य, भक्ति और प्रेम का उदय होता था। – भूतकाल
- मैं दीवाना हुआ उनके तट के उस पर टिका था। – भूतकाल
विश्लेषण: ये काल पत्र के संदर्भ को स्पष्ट करते हैं।
प्रश्न (ख): अब इन वाक्यों के काल को अन्य कालों में बदलकर लिखिए।
उत्तर:
- मूल: निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान देंगे। (भविष्य काल)
- भूतकाल: निश्चय था कि आपने इस पत्र को स्थान दिया।
- वर्तमान काल: निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दे रहे हैं।
- मूल: यह भूमि तीन ओर सुदूर हो-देरे पर्वतों से घिरी है। (वर्तमान काल)
- भूतकाल: यह भूमि तीन ओर सुदूर हो-देरे पर्वतों से घिरी थी।
- भविष्य काल: यह भूमि तीन ओर सुदूर हो-देरे पर्वतों से घिरी होगी।
- मूल: सज्जन ऐसे कि पलट मारने से फल देने हैं। (वर्तमान काल)
- भूतकाल: सज्जन ऐसे थे कि पलट मारने से फल देते थे।
- भविष्य काल: सज्जन ऐसे होंगे कि पलट मारने से फल देंगे।
- मूल: पत्र में वैराग्य, भक्ति और प्रेम का उदय होता था। (भूतकाल)
- वर्तमान काल: पत्र में वैराग्य, भक्ति और प्रेम का उदय होता है।
- भविष्य काल: पत्र में वैराग्य, भक्ति और प्रेम का उदय होगा।
- मूल: मैं दीवाना हुआ उनके तट के उस पर टिका था। (भूतकाल)
- वर्तमान काल: मैं दीवाना हूँ उनके तट के उस पर टिका हूँ।
- भविष्य काल: मैं दीवाना होऊँगा उनके तट के उस पर टिका होऊँगा।
विश्लेषण: काल बदलने से वाक्य का समय संदर्भ बदलता है, लेकिन अर्थ वही रहता है।
प्रश्न (ग): इस रचना में भारतेंदु की न कही-कही प्राचीन कवि का प्रयोग किया है, जैसे- शिखर के लिए शिखर, यात्रियों के लिए यात्रियों। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए।
उत्तर:
- शिखर – पर्वत की चोटी
- यात्री – यात्रियों
- तीर्थ – पवित्र स्थान
- स्नान – गंगा में डुबकी
- सुगंध – खुशबू
विश्लेषण: ये शब्द प्राचीन और साहित्यिक शैली को दर्शाते हैं, जो पत्र को विशेष बनाते हैं।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: पाठ से आगे – आपकी बात
- पंक्ति: “मैंने गंगा जी के तट पर स्नान करके… भोजन किया।”
प्रश्न: क्या आपने कभी खुले वातावरण में या प्रकृति के पास भोजन किया है? वह अनुभव घर के खाने से कैसे भिन्न था?
उत्तर: हाँ, मैंने अपने गाँव में एक नदी के किनारे भोजन किया। यह अनुभव घर के खाने से भिन्न था क्योंकि:
- प्रकृति की शांति और हवा ने भोजन को और स्वादिष्ट बनाया।
- खुला वातावरण और पक्षियों की आवाज ने मन को प्रसन्न किया।
- यह अनुभव सादगी और प्रकृति से जुड़ाव का था।
विश्लेषण: प्रकृति में भोजन का सुख आध्यात्मिक और शांत होता है।
- पंक्ति: “उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था।”
प्रश्न: आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया, जब किसी सामान्य-सी वस्तु ने आपको गहरा सुख दिया हो?
उत्तर: हाँ, एक बार मैंने अपने दोस्तों के साथ एक साधारण पिकनिक में रोटी और आचार खाया। वह साधारण भोजन दोस्तों की हँसी और प्रकृति के बीच इतना सुखद था कि वह आज भी याद है।
विश्लेषण: सादगी में सुख की अनुभूति हरिद्वार के अनुभव से मिलती-जुलती है। - पंक्ति: “हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी।”
प्रश्न: आपको किस स्थान पर पवित्रता और प्रसन्नता का अनुभव होता है? उस स्थान की कौन-कौन सी विशेषताएँ आपको अच्छी लगीं?
उत्तर: मुझे मेरे गाँव का मंदिर पवित्र और प्रसन्नता देता है।
विशेषताएँ:
- शांत वातावरण और घंटियों की आवाज।
- फूलों की सुगंध और दीपों की रोशनी।
- भक्तों की भक्ति और सामुदायिक भावना।
विश्लेषण: यह हरिद्वार की पवित्रता और शांति से मिलता-जुलता है।
- पंक्ति: “पास में वर्णित है, वहाँ के वृक्ष ‘फल, फूल, गाय… जल में भी कोयले और गाय से लोगों का मनोहन पूर्ण करते हैं।'”
प्रश्न: क्या आपके जीवन में कोई पेड़, फूल या प्राकृतिक वस्तु है जिससे आप विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं? क्यों?
उत्तर: मैं अपने घर के बगीचे में लगे आम के पेड़ से जुड़ाव महसूस करता हूँ।
क्यों:
- यह मुझे छाया और फल देता है।
- बचपन में इसके नीचे खेलना यादगार है।
- इसकी हरियाली मन को शांति देती है।
विश्लेषण: यह हरिद्वार के प्राकृतिक तत्वों से जुड़ाव को दर्शाता है।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): अपने किसी मित्र के साथ बिना बोले संवाद कीजिए— संकेतों से। आप सोचिए कि भारत में भ्रमण करने के लिए क्या-क्या आवश्यक होता है?
उत्तर: संकेतों से संवाद:
- हाथ से नक्शा बनाना: यात्रा की योजना और नक्शा जरूरी।
- बैग का इशारा: सामान, कपड़े, और पानी की बोतल।
- कैमरे का संकेत: फोटो खींचने के लिए कैमरा।
- हाथ जोड़ना: स्थानीय संस्कृति का सम्मान।
विश्लेषण: यह गतिविधि यात्रा की तैयारी को रचनात्मक रूप से दर्शाती है।
प्रश्न (ख): यात्रा करते हुए ऐतिहासिक यात्रियों की स्मृति के लिए आप क्या करेंगे?
- एक मसाले का नाम
- कपास से जुड़ा एक शब्द
- जहाँ स्नान होता है
- दूध के किसी अंश का नाम
- एक पवित्र स्थल का नाम
- व्यापार से जुड़ा शब्द
- एक नदी का नाम
- एक पर्वत का नाम
- एक पवित्र स्थल का नाम
उत्तर: - मसाला: जावित्री
- कपास से शब्द: सूत
- जहाँ स्नान होता है: हर की पौड़ी
- दूध का अंश: मलाई
- पवित्र स्थल: वैष्णो देवी
- व्यापार से शब्द: दुकान
- नदी: यमुना
- पर्वत: हिमालय
- पवित्र स्थल: काशी
विश्लेषण: ये शब्द हरिद्वार के संदर्भ और भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं ।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक है – “अंधेर नगरी।” इसे पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूँढकर पढ़िए और अपने समूह के साथ चर्चा कीजिए।
उत्तर:
विवरण: “अंधेर नगरी” भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक व्यंग्यात्मक नाटक है, जो सामाजिक और प्रशासनिक अव्यवस्था पर कटाक्ष करता है। इसमें एक ऐसी नगरी का वर्णन है जहाँ सब कुछ एक समान मूल्य पर बिकता है, चाहे वह मिठाई हो या सब्जी। यह नाटक अज्ञानता और अन्याय को उजागर करता है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि यह नाटक आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह सामाजिक असमानता और मूर्खतापूर्ण नियमों पर प्रहार करता है। उदाहरण के लिए, नाटक में गुरु घंटाल की मूर्खता आज के कुछ नेताओं की नीतियों से मिलती है।
विश्लेषण: यह गतिविधि भारतेंदु के साहित्यिक योगदान को समझने में मदद करती है ।
अध्याय 5- कबीर के दोहों के नोट्स प्रश्न-उत्तर रूप में
लेखक: संत कबीर
प्रश्न 1: कबीर कौन थे और उनका जन्म कब हुआ?
उत्तर 1: कबीर 15वीं शताब्दी के संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म काशी (वाराणसी) में माना जाता है। उनकी रचनाएँ भक्ति और सत्य के मार्ग को दर्शाती हैं।
प्रश्न 2: कबीर की रचनाओं की विशेषता क्या है?
उत्तर 2: कबीर की रचनाएँ सरल, सहज और सत्य पर आधारित हैं। उनके दोहे जीवन की सच्चाई, आध्यात्मिकता, और सामाजिक सुधार पर बल देते हैं। ये भजनों की तरह गाए और पढ़ाए जाते हैं ।
प्रश्न 3: कबीर के दोहों का मुख्य संदेश क्या है?
उत्तर 3: कबीर के दोहे निम्नलिखित संदेश देते हैं:
- सत्य और ईमानदारी का महत्व।
- आलोचना को स्वीकार कर आत्म-सुधार करना।
- मधुर वाणी का प्रयोग।
- अच्छी संगति का प्रभाव।
- गुरु का महत्व और आत्म-निरीक्षण।
प्रश्न 4: कबीर ने गुरु को गोविंद से ऊपर क्यों माना?
उत्तर 4: कबीर ने गुरु को गोविंद (ईश्वर) से ऊपर माना क्योंकि गुरु वह मार्गदर्शक है जो हमें ईश्वर तक पहुँचाता है। गुरु के बिना सत्य और ज्ञान की प्राप्ति कठिन है ।
प्रश्न 5: कबीर के अनुसार संगति का क्या प्रभाव है?
उत्तर 5: कबीर कहते हैं कि जैसी संगति होती है, वैसा ही फल मिलता है। अच्छी संगति सकारात्मक विचार और व्यवहार को प्रेरित करती है, जबकि बुरी संगति नकारात्मक प्रभाव डालती है।
प्रश्न 6: कबीर ने आलोचना को कैसे देखा?
उत्तर 6: कबीर ने आलोचना को सकारात्मक माना। वे कहते हैं कि निंदक को पास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारी कमियों को बताकर सुधार का अवसर देता है, जैसे साबुन गंदगी साफ करता है।
प्रश्न 7: कबीर के दोहों में सादगी और मधुर वाणी का महत्व क्यों है?
उत्तर 7: कबीर के अनुसार, सादगी और मधुर वाणी मन को शांति देती है और दूसरों के साथ संबंधों को मधुर बनाती है। यह आत्मिक और सामाजिक सुख का स्रोत है।
अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (केवल हिंदी में)
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर के सामने सही (✓) का निशान लगाएँ।
- “गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय।” इस दोहे में किसका बखान किया गया है?
- गुरु का महत्व (✓)
- गोविंद का महत्व
- भक्ति का महत्व
विश्लेषण: यह दोहा गुरु के महत्व को दर्शाता है, जो हमें ईश्वर तक पहुँचाता है।
- “अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।” इस दोहे का मूल संदेश क्या है?
- हमेशा चुप रहने में ही सम्मान भला है
- बारिश और धूप से बचना चाहिए
- परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है (✓)
- हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए
विश्लेषण: यह दोहा जीवन में संतुलन का महत्व बताता है; न अति बोलना अच्छा है, न अति चुप रहना ।
- “बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।” यह दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है?
- समय का सहमूल्य उपयोग करना
- दूसरों के काम आना (✓)
- धैर्यपूर्वक और शांति में काम करना
- सभी के प्रति उदार रहना
विश्लेषण: यह दोहा बताता है कि केवल बड़ा होना पर्याप्त नहीं; दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए ।
- “ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय। औरन को सीतल करे, आपहु सीतल होय।” इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
- लोग हमारी प्रशंसा और सम्मान से बढ़ते हैं
- दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है (✓)
- किसी में द्वेष होने पर उसमें जीत हासिल होती है
- सुनने वालों का मन धैर्य-उत्साह भटककर रहता है
विश्लेषण: मधुर वाणी दूसरों और स्वयं को शांति देती है ।
- “सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सत्य है, ता हृदय हरि आप।” इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
- सत्य और झूठ में कोई अंतर नहीं होता
- सत्य का पालन करना साधना की तरह पवित्र है (✓)
- कठिन परिस्थितियों में जीवन में सफलता तय करता है
- सत्य महत्त्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय कष्टमुक्त होता है
विश्लेषण: सत्य को तप के समान और झूठ को पाप के समान माना गया है।
- “निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।” यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है?
- आलोचना से बचना चाहिए
- आलोचकों को दूर रखना चाहिए
- आलोचकों को पास रखना चाहिए (✓)
- आलोचकों की निंदा करनी चाहिए
विश्लेषण: आलोचक हमारी कमियों को बताकर सुधार का अवसर देता है।
- “साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय। सार-सार को गहि लेइ, छाया देइ उड़ाय।” इस दोहे में ‘सूप’ किसका प्रतीक है?
- मन की कल्पनाओं का
- सूप गुणों का (✓)
- निंदक और सुपुत्र का
- कठोर और कोमल स्वभाव का
विश्लेषण: सूप अच्छे-बुरे को छानकर सार को ग्रहण करता है, जो साधु के गुण को दर्शाता है।
प्रश्न (ब): हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?
उत्तर (ब): मैंने उपरोक्त उत्तर इसलिए चुने:
- प्रश्न 1: गुरु का महत्व इस दोहे में स्पष्ट है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक मार्ग दिखाता है।
- प्रश्न 2: संतुलन जीवन का मूल मंत्र है, जो इस दोहे में “अति” से बचने की सलाह देता है।
- प्रश्न 3: खजूर का पेड़ बड़ा होने के बावजूद छाया और फल नहीं देता, इसलिए दूसरों के काम आना जरूरी है।
- प्रश्न 4: मधुर वाणी शांति देती है, जो इस दोहे का मुख्य संदेश है।
- प्रश्न 5: सत्य को तप के समान माना गया, जो आध्यात्मिक मूल्य है।
- प्रश्न 6: निंदक हमारी कमियों को उजागर करता है, इसलिए उसे पास रखना चाहिए।
- प्रश्न 7: सूप अच्छे-बुरे को छानता है, जो साधु के गुण का प्रतीक है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि कबीर के दोहे सरल भाषा में गहरे जीवन मूल्यों को दर्शाते हैं।
अभ्यास प्रश्न
मिलकर करें मिलान
प्रश्न (क): पाठ में चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। इन्हें स्तंभ 2 में दिए गए उनके सही अर्थ या संदर्भ में मिलाइए।
उत्तर: OCR में स्तंभ 2 के कुछ हिस्से अस्पष्ट हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर:
| क्रम | स्तंभ 1 | स्तंभ 2 |
|---|---|---|
| 1. | गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय | बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय। |
| 2. | ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय | औरन को सीतल करे, आपहु सीतल होय। |
विश्लेषण: ये पंक्तियाँ गुरु के महत्व और मधुर वाणी के प्रभाव को दर्शाती हैं ।
अभ्यास प्रश्न
मिलकर करें मिलान
प्रश्न (ब): नीचे स्तंभ 1 में दोहों की पंक्तियों को स्तंभ 2 में दी गई उपयुक्त पंक्तियों से जोड़िए।
उत्तर:
| क्रम | स्तंभ 1 | स्तंभ 2 |
|---|---|---|
| 1. | गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय | बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय। |
| 2. | अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप | अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। |
| 3. | ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय | औरन को सीतल करे, आपहु सीतल होय। |
| 4. | निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय | बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय। |
| 5. | साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय | सार-सार को गहि लेइ, छाया देइ उड़ाय। |
| 6. | कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवाँ जाय | जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाय। |
| 7. | बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर | पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। |
| 8. | सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप | जाके हृदय सत्य है, ता हृदय हरि आप। |
विश्लेषण: यह मिलान दोहों के अर्थ को स्पष्ट करता है।
पंक्तियों पर चर्चा
प्रश्न (क): “कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवाँ जाय। जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाय।”
उत्तर:
अर्थ: यह दोहा कहता है कि मन एक पक्षी की तरह स्वतंत्र है और जहाँ चाहे वहाँ जाता है। लेकिन जैसी संगति होती है, वैसा ही फल मिलता है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि यह दोहा संगति के प्रभाव को दर्शाता है। अच्छी संगति सकारात्मक व्यवहार बनाती है, जबकि बुरी संगति नकारात्मक प्रभाव डालती है।
प्रश्न (ख): “सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सत्य है, ता हृदय हरि आप।”
उत्तर:
अर्थ: सत्य सबसे बड़ा तप है और झूठ सबसे बड़ा पाप। जिसके हृदय में सत्य है, वह ईश्वर के समान है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि यह दोहा सत्य के महत्व को दर्शाता है। सत्य बोलने से मन शुद्ध और शांत रहता है।
सोच-विचार के लिए
प्रश्न (क): “गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय।” इस दोहे में गुरु को गोविंद से ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं?
उत्तर: हाँ, मैं सहमत हूँ। गुरु वह मार्गदर्शक है जो हमें सत्य और ईश्वर तक पहुँचाता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के, ईश्वर को समझना कठिन है। उदाहरण: मेरे शिक्षक ने मुझे मेहनत और ईमानदारी सिखाई, जिससे मेरा जीवन बेहतर हुआ।
विश्लेषण: यह दोहा गुरु के महत्व को रेखांकित करता है।
प्रश्न (ख): “बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।” बड़े या संपन्न होने के साथ-साथ मनुष्य में और कौन-कौन सी विशेषताएँ होनी चाहिए?
उत्तर: मनुष्य में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए:
- दूसरों के लिए उपयोगी होना।
- उदारता और सहानुभूति।
- सादगी और मधुर व्यवहार।
- सत्य और ईमानदारी।
विश्लेषण: केवल बड़ा होना पर्याप्त नहीं; दूसरों के काम आना जरूरी है।
प्रश्न (ग): “ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय।” क्या आप मानते हैं कि वाणी का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं, स्वयं पर भी पड़ता है?
उत्तर: हाँ, मधुर वाणी का प्रभाव दूसरों और स्वयं पर पड़ता है।
उदाहरण: जब मैंने अपने मित्र से नम्रता से बात की, तो उसका गुस्सा शांत हुआ और मुझे भी शांति मिली।
विश्लेषण: मधुर वाणी मन को शांत और संबंधों को मधुर बनाती है .
प्रश्न (ङ): “जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाय।” हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: संगति हमारे विचारों और व्यवहार को आकार देती है।
उदाहरण: जब मैं मेहनती दोस्तों के साथ रहा, तो मेरी पढ़ाई में सुधार हुआ। लेकिन एक बार गलत संगति में पड़ने से मेरा समय बर्बाद हुआ।
विश्लेषण: यह दोहा संगति के प्रभाव को दर्शाता है।
अभ्यास प्रश्न
दोहे की रचना
प्रश्न (क): दोहे की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें-
- एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द एक साथ आए हैं।
- “गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय।” (गुरु, गोविंद)
- “साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय।” (साधु, सूप)
- एक शब्द एक साथ दो बार आया है।
- “अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप।” (अति-अति)
- “सार-सार को गहि लेइ, छाया देइ उड़ाय।” (सार-सार)
- लगभग एक जैसे शब्द, जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर है।
- “बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।” (पेड़, खजूर)
- “जलके हृदय सत्य है, ता हृदय हरि आप।” (जल, जाल नहीं, लेकिन सत्य-हरि)
- एक ही पंक्ति में विशेषताधिक शब्दों का प्रयोग।
- “सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।” (सत्य-झूठ)
- “ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय।” (मधुर-आपा)
- किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है।
- “साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय।” (साधु की तुलना सूप से)
- “बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।” (बड़े व्यक्ति की तुलना खजूर से)
- किसी को कोई अन्य नाम दे दिया गया है।
- कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं, लेकिन “गोविंद” ईश्वर का पर्याय है।
- किसी शब्द की कोई शैली नहीं है।
- “चुप” के स्थान पर “चुप” ही प्रयोग हुआ है, जैसे “अति का भला न चुप।”
- उदाहरण द्वारा बात को समझाया गया है।
- “निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।” (साबुन का उदाहरण)
- “साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय।” (सूप का उदाहरण)
प्रश्न (ख): अपने समूह की सूची को कक्षा में साझा कीजिए।
उत्तर: उपरोक्त सूची समूह में चर्चा के बाद तैयार की गई। हमने माना कि कबीर के दोहों में सरलता, समान ध्वनियाँ, और प्रतीकात्मकता उनकी शक्ति हैं। कक्षा में इसे साझा करने से हमें दोहों की गहराई समझने में मदद मिली ।
अनुमान और कल्पना से
प्रश्न (क): “गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय।”
- यदि आपके सामने यह स्थिति होती तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों?
उत्तर: मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करता, क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो मुझे ईश्वर तक ले जाता है। गुरु का ज्ञान मुझे सही रास्ता दिखाता है।
विश्लेषण: गुरु का मार्गदर्शन जीवन में आधारभूत है (पेज 6)। - यदि आपमें कोई गुरु या शिक्षक न होता तो क्या होता?
उत्तर: बिना गुरु के मैं जीवन के सही मूल्यों और दिशा से भटक सकता था। उदाहरण: मेरे शिक्षक ने मुझे मेहनत सिखाई, वरना मैं आलसी रह सकता था।
विश्लेषण: गुरु का अभाव जीवन को दिशाहीन बना सकता है ।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (ब): “अति का भला न बोलना…” इस दोहे का आज के समय में क्या महत्त्व है?
उत्तर:
महत्त्व: यह दोहा आज के समय में संतुलन का पाठ पढ़ाता है। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अति बोलते हैं या चुप रहते हैं, जो विवाद पैदा करता है। संतुलित वाणी से शांति बनी रहती है।
पक्ष में तर्क:
- वाणी पर संयम से गलतफहमियाँ कम होती हैं।
- संतुलित बोलचाल सम्मान बढ़ाती है।
विपक्ष में तर्क: - अत्यधिक चुप रहना आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है।
- कुछ परिस्थितियों में खुलकर बोलना जरूरी है।
विश्लेषण: यह दोहा संतुलन और संयम की प्रासंगिकता को दर्शाता है ।
प्रश्न (ग): पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों की सूची अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए।
उत्तर:
पक्ष में तर्क:
- संतुलित वाणी से संबंध मधुर रहते हैं।
- अति बोलने से विवाद और गलतफहमियाँ बढ़ती हैं।
विपक्ष में तर्क: - चुप रहना आत्मविश्वास की कमी दिखाता है।
- सत्य को व्यक्त करने के लिए बोलना जरूरी है।
विश्लेषण: यह चर्चा दोहे की प्रासंगिकता को रेखांकित करती है।
शब्द से जुड़े शब्द
प्रश्न: कबीर से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए।
उत्तर:
- कबीर: संत, कवि।
- दोहे: गुरु, सत्य, बानी, संगति, निंदक, सूप, खजूर।
- कहावतें: “जैसी संगति, वैसा रंग।”
चर्चा: समूह में हमने माना कि ये शब्द कबीर की शिक्षाओं को सरलता से व्यक्त करते हैं ।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: कहावतों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए।
उत्तर:
- जैसी संगति, वैसा रंग: गलत दोस्तों की संगति ने उसे गलत रास्ते पर ले गया।
- सत्य का बल: सत्य बोलकर उसने सबका दिल जीत लिया।
- मधुर वाणी: उसकी मधुर बातों ने सभी को शांत कर दिया।
विश्लेषण: ये कहावतें कबीर के दोहों से प्रेरित हैं।
प्रश्न: पाठ के किसी एक दोहे को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:
दोहा: “ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय। औरन को सीतल करे, आपहु सीतल होय।”
- गायन: लोकगीत शैली में इसे भजन के रूप में गाया जा सकता है।
- भाव-नृत्य: नृत्य के माध्यम से मधुर वाणी का प्रभाव दिखाया जा सकता है।
- अभिनय: एक दोस्त गुस्से में चिल्लाता है, दूसरा उसे मधुर वाणी से शांत करता है।
विश्लेषण: यह प्रस्तुति दोहे के संदेश को रचनात्मक बनाती है।
पाठ से आगे
प्रश्न (क): “गुरु गोविंद दोऊ खड़े…” आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने दिशा दिखाई?
उत्तर: मेरे गणित शिक्षक ने मुझे मेहनत और अनुशासन सिखाया। उनकी प्रेरणा से मैंने अपनी पढ़ाई में सुधार किया।
विश्लेषण: यह दोहा गुरु के महत्व को दर्शाता है।
प्रश्न (ख): “निंदक नियरे राखिए…” क्या किसी ने आपकी कमियों को बताया जिससे सुधार हुआ?
उत्तर: मेरे मित्र ने बताया कि मैं समय पर काम नहीं करता। इससे मैंने समय प्रबंधन सीखा और मेरे अंक बेहतर हुए।
विश्लेषण: आलोचना सुधार का अवसर देती है।
प्रश्न (ग): “कबीरा मन पंछी भया…” क्या संगति ने आपके विचारों को प्रभावित किया?
उत्तर: हाँ, मेरे मेहनती दोस्तों की संगति ने मुझे पढ़ाई में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
विश्लेषण: संगति विचारों और व्यवहार को आकार देती है।
सृजन
प्रश्न (क): “सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।” इस दोहे पर आधारित कहानी।
उत्तर:
एक बार एक स्कूल में क्रिकेट मैच था। अमन की टीम हार रही थी, और उसका दोस्त नियम तोड़कर जीतने की सलाह दे रहा था। अमन ने सत्य का साथ दिया और नियम तोड़ने से मना कर दिया। हालांकि उसकी टीम हार गई, लेकिन शिक्षक ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। अमन को समझ आया कि सत्य का पालन ही सच्ची जीत है।
विश्लेषण: यह कहानी सत्य के महत्व को दर्शाती है।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (ख): “गुरु गोविंद दोऊ खड़े…” अपने प्रेरणादायक शिक्षक पर निबंध।
उत्तर:
मेरे प्रेरणादायक शिक्षक
मेरे हिंदी शिक्षक, श्री रमेश शर्मा, मेरे जीवन के प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने मुझे न केवल हिंदी साहित्य सिखाया, बल्कि सत्य, ईमानदारी और मेहनत के मूल्य भी सिखाए। एक बार जब मैं परीक्षा में असफल हुआ, तो उन्होंने मुझे हार नहीं मानने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षाएँ मुझे कबीर के दोहे “गुरु गोविंद दोऊ खड़े” की याद दिलाती हैं, क्योंकि वे मुझे सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी मधुर वाणी और धैर्य ने मुझे आत्मविश्वास दिया।
विश्लेषण: यह निबंध गुरु के महत्व को दर्शाता है।
कबीर हमारे समय में
प्रश्न (क): कबीर आज के समय में किन विषयों पर कविता लिख सकते हैं?
उत्तर:
- सोशल मीडिया का दुरुपयोग।
- पर्यावरण संरक्षण।
- सामाजिक समानता।
- साइबर सुरक्षा।
प्रश्न (ख): इन विषयों पर दो-दो पंक्तियाँ।
उत्तर:
- सोशल मीडिया:
सोशल मीडिया मन को भटकाए, सत्य को छोड़ झूठ अपनाए।
मधुर वाणी से सत्य बोलो, मन को शांत और साफ रखो। - पर्यावरण:
पेड़-पौधे साँसें देते, इन्हें काटना पाप सम है।
प्रकृति की रक्षा साधु सुभाय, सूप जैसा सार ग्रहण कर।
विश्लेषण: ये पंक्तियाँ कबीर की शैली में आधुनिक समस्याओं को दर्शाती हैं।
साइबर सुरक्षा और दोहे
प्रश्न (क): “अति का भला न बोलना…” इंटरनेट पर अनावश्यक सूचनाएँ साझा करने के संकट?
उत्तर:
- निजी जानकारी चोरी हो सकती है।
- साइबर धोखाधड़ी का खतरा।
- गलत सूचनाओं से प्रतिष्ठा को हानि।
विश्लेषण: अनावश्यक साझा करना असंतुलन का परिणाम है।
प्रश्न (ख): “साधु ऐसा चाहिए…” जानकारी को छानने की आवश्यकता क्यों?
उत्तर:
- क्यों: सारी जानकारी सही नहीं होती; गलत सूचना हानिकारक हो सकती है।
- कैसे तय करें: विश्वसनीय स्रोतों (जैसे सरकारी वेबसाइट) से जानकारी लें। सूप की तरह अच्छा-बुरा छानें।
विश्लेषण: यह दोहा सतर्कता और विवेक का महत्व दर्शाता है।
आज के समय में
प्रश्न: दी गई घटनाओं के लिए उपयुक्त दोहे लिखिए।
उत्तर:
- घटना: अमित का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वह गलत संगति में चला गया।
दोहा: “कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवाँ जाय। जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाय।” - घटना: एक विद्यार्थी इंटरनेट पर सूचनाएँ खोज रहा था। पिता ने कहा, “हर जानकारी सही नहीं होती।”
दोहा: “साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय। सार-सार को गहि लेइ, छाया देइ उड़ाय।”
विश्लेषण: ये दोहे घटनाओं के संदर्भ को स्पष्ट करते हैं।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: आपका मित्र आपकी गलती पर आलोचना करता है। आप पहले परेशान होते हैं, फिर सोचते हैं…
उत्तर:
दोहा: “निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।”
विश्लेषण: यह दोहा आलोचना को सकारात्मक रूप से लेने की सलाह देता है, क्योंकि यह सुधार का अवसर देता है।
अध्याय 6-एक टोकरी भर मिट्टी- नोट्स प्रश्न-उत्तर रूप में
लेखक: माधवराव सप्रे
प्रश्न 1: कहानी का मुख्य विषय क्या है?
उत्तर 1: कहानी का मुख्य विषय एक गरीब वृद्धा की झोंपड़ी के प्रति लगाव और जमींदार के लालच के कारण हुए अन्याय की कहानी है, जो अंत में दया और पश्चाताप के माध्यम से न्याय की ओर बढ़ती है (पेज 1-2)।
प्रश्न 2: वृद्धा की झोंपड़ी क्यों महत्वपूर्ण थी?
उत्तर 2: वृद्धा की झोंपड़ी उसकी यादों का आधार थी, जहाँ उसने अपने पति और पुत्र के साथ समय बिताया था। उसकी पोती के लिए भी यह एकमात्र घर था, जिसके बिना वह खाना-पीना छोड़ चुकी थी (पेज 1)।
प्रश्न 3: जमींदार ने वृद्धा की झोंपड़ी पर कब्जा कैसे किया?
उत्तर 3: जमींदार ने अपनी शक्ति और वकीलों की मदद से अदालत के माध्यम से झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया, वृद्धा को बेदखल कर दिया (पेज 1)।
प्रश्न 4: वृद्धा ने जमींदार से क्या अनुरोध किया?
उत्तर 4: वृद्धा ने झोंपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेने की अनुमति मांगी ताकि वह अपनी पोती के लिए चूल्हा बनाकर रोटी पका सके, जिससे पोती खाना शुरू कर दे (पेज 1-2)।
प्रश्न 5: जमींदार का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ?
उत्तर 5: जब वृद्धा ने जमींदार से टोकरी को हाथ लगाने को कहा और बताया कि झोंपड़ी में अनगिनत टोकरियों जितनी मिट्टी का भार है, तो जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आँखें खुलीं, और उन्होंने पश्चाताप करते हुए वृद्धा की झोंपड़ी वापस कर दी (पेज 2)।
प्रश्न 6: कहानी का मुख्य संदेश क्या है?
उत्तर 6: कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची शक्ति दया और न्याय में है। धन और अहंकार से प्रेरित कार्य पश्चाताप का कारण बनते हैं, और मानवता व करुणा ही सही मार्ग दिखाती है (पेज 2, 11)।
प्रश्न 7: कहानी में किन भावनाओं का चित्रण हुआ है?
उत्तर 7: कहानी में दुख, लगाव, करुणा, पश्चाताप, विनम्रता, और न्याय जैसे भावों का चित्रण हुआ है (पेज 9, 11)।
प्रश्न 8: कहानी की शैली की विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर 8: कहानी में प्रश्नोत्तरी शैली, वर्णनात्मकता, भावात्मकता, संवादात्मकता, नाटकीयता, और चरित्र चित्रण का उपयोग हुआ है, जो पाठक को कहानी से जोड़ता है (पेज 9)।
अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (केवल हिंदी में)
पेज 3: मेरी समझ से
प्रश्न (क): निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा (★) बनाइए।
- जमींदार को झोंपड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी?
- झोंपड़ी जरूरी हो चुकी थी
- झोंपड़ी रास्ते में बाधा थी
- वह अहाते को विस्तार करना चाहता था (★)
- वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था
विश्लेषण: जमींदार अपने महल के अहाते को विस्तार करना चाहता था, इसलिए झोंपड़ी पर कब्जा किया (पेज 1)।
- वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी?
- क्रोध और शान्ति करके
- अदालत से अनुमति लेकर
- विनती और नम्रता से (★)
- चुपचाप उठाकर ले गई
विश्लेषण: वृद्धा ने गिड़गिड़ाकर और नम्रता से मिट्टी ले जाने की अनुमति मांगी (पेज 1)।
- वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है?
- दया
- लगाव (★)
- गुस्सा
- डर
विश्लेषण: पोती का खाना-पीना छोड़ना झोंपड़ी के प्रति उसके गहरे लगाव को दर्शाता है (पेज 1)।
- कहानी का अंत कैसा है?
- दुखद
- सुखद (★)
- प्रेरणादायक (★)
- सकारात्मक (★)
विश्लेषण: कहानी का अंत सुखद, सकारात्मक, और प्रेरणादायक है, क्योंकि जमींदार ने झोंपड़ी वापस कर दी (पेज 2)।
प्रश्न (ख): हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?
उत्तर: मैंने उपरोक्त उत्तर इसलिए चुने:
- प्रश्न 1: जमींदार का उद्देश्य अहाते का विस्तार था, न कि पुराना झगड़ा या बाधा।
- प्रश्न 2: वृद्धा की विनम्रता कहानी में स्पष्ट है, क्योंकि उसने गिड़गिड़ाकर अनुरोध किया।
- प्रश्न 3: पोती का व्यवहार लगाव को दर्शाता है, क्योंकि वह झोंपड़ी के बिना जी नहीं सकती थी।
- प्रश्न 4: अंत सुखद और प्रेरणादायक है, क्योंकि जमींदार का हृदय परिवर्तन हुआ।
चर्चा: समूह में हमने माना कि कहानी मानवता और दया के महत्व को दर्शाती है (पेज 3)।
पेज 7: अभ्यास प्रश्न
मुहावरे
प्रश्न (क): इस वाक्य में मुहावरों की पहचान करके उन्हें रेखांकित कीजिए।
वाक्य: “बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की धोती गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया।”
उत्तर:
- बाल की खाल निकालने वाले
- धोती गर्म कर
विश्लेषण: ये मुहावरे वकीलों की सूक्ष्मता और रिश्वतखोरी को दर्शाते हैं (पेज 7)।
प्रश्न (ख): ‘बाल’ शब्द से जुड़े निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए।
उत्तर:
- बाल बांका न होना: जमींदार की शक्ति के सामने भी वृद्धा का हौसला ऐसा था कि उसका बाल बांका न हुआ।
- बाल बराबर: वृद्धा की बातों में बाल बराबर सत्य था, जिसने जमींदार का मन बदल दिया।
- बाल बराबर फर्क होना: जमींदार और वृद्धा की स्थिति में बाल बराबर फर्क था, फिर भी दया ने सब बराबर कर दिया।
- बाल-बाल बचना: वृद्धा की झोंपड़ी बाल-बाल बची, जब जमींदार ने उसे वापस कर दिया।
विश्लेषण: ये वाक्य कहानी के संदर्भ में मुहावरों का सटीक उपयोग दर्शाते हैं (पेज 7)।
पेज 8: अभ्यास प्रश्न
नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में बदलें:
उत्तर:
क) वह गिड़गिड़ाकर बोली।
- वर्तमान काल: वह गिड़गिड़ाकर बोल रही है।
- भविष्य काल: वह गिड़गिड़ाकर बोलेगी।
ख) श्रीमान् ने आज्ञा दे दी।
- वर्तमान काल: श्रीमान् आज्ञा दे रहे हैं।
- भविष्य काल: श्रीमान् आज्ञा देंगे।
ग) उसकी आँखों से आँसू की धारा बहने लगी।
- वर्तमान काल: उसकी आँखों से आँसू की धारा बह रही है।
- भविष्य काल: उसकी आँखों से आँसू की धारा बहेगी।
घ) जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई।
- वर्तमान काल: जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हो रही है।
- भविष्य काल: जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होगी।
ङ) उन्होंने वृद्धा से क्षमा माँगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी।
- वर्तमान काल: वे वृद्धा से क्षमा माँग रहे हैं और उसकी झोंपड़ी वापस दे रहे हैं।
- भविष्य काल: वे वृद्धा से क्षमा माँगेंगे और उसकी झोंपड़ी वापस देंगे।
विश्लेषण: ये परिवर्तन क्रिया के काल को स्पष्ट करते हैं (पेज 8)।
वचन की पहचान
वाक्य: “उनके मन में कुछ दया आ गई।” और “उनकी आँखें खुल गईं।”
प्रश्न: इनमें क्या अंतर है, और क्यों?
उत्तर:
- अंतर: “मन” एकवचन है, जबकि “आँखें” बहुवचन है।
- कारण: “मन” एक व्यक्ति का एक ही होता है, इसलिए एकवचन में प्रयोग हुआ। “आँखें” दो होती हैं, इसलिए बहुवचन में प्रयोग हुआ। अनुस्वार (ं) से बहुवचन का बोध होता है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि शब्दों का वचन अर्थ को स्पष्ट करता है (पेज 8)।
रिक्त स्थान भरें:
उत्तर:
- क) वृद्धा झोंपड़ी के भीतर (गई)
- ख) वृद्धा गिड़गिड़ाकर (बोली)
- ग) पोती ने खाना-पीना छोड़ (दिया है)
- घ) उसकी आँखों से आँसू की धारा बहने (लगी थी)
- ङ) उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले (आई)
- च) झोंपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को जला (रही थीं)
- छ) पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी-सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला (दिए हैं)
विश्लेषण: ये शब्द कहानी के संदर्भ में सही काल और अर्थ पूर्ण करते हैं (पेज 8)।
पेज 9: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): कहानी की विशेषताएँ ढूँढ़कर उनकी सूची बनाइए।
उत्तर:
- प्रश्नोत्तरी शैली: वृद्धा की विनती पाठक को सोचने पर मजबूर करती है।
- वर्णनात्मकता: झोंपड़ी और वृद्धा की भावनाओं का चित्रण जीवंत है।
- भावात्मकता: वृद्धा का दुख और जमींदार का पश्चाताप गहरे भाव जगाते हैं।
- संवादात्मकता: वृद्धा और जमींदार के संवाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
- नाटकीयता: टोकरी उठाने का दृश्य नाटकीय और प्रभावशाली है।
- चरित्र चित्रण: वृद्धा की विनम्रता और जमींदार का हृदय परिवर्तन स्पष्ट है।
विश्लेषण: ये विशेषताएँ कहानी को प्रभावी बनाती हैं (पेज 9)।
प्रश्न (ख): कहानी की विशेषताओं के उदाहरण:
| कहानी की विशेषताएँ | कहानी से उदाहरण |
|---|---|
| 1. प्रश्नोत्तरी शैली | “आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी का भार आप कैसे उठा सकेंगे?” |
| 2. वर्णनात्मकता | “जब उसे अपनी पूर्वस्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट-फूट कर रोने लगती थी।” |
| 3. भावात्मकता | “अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी।” |
| 4. संवादात्मकता | “महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए।” |
| 5. नाटकीयता | “यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी।” |
| 6. चरित्र चित्रण | “जमींदार साहब धन-मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे।” |
| विश्लेषण: ये उदाहरण कहानी की शैली को स्पष्ट करते हैं (पेज 9)। |
पेज 11: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: नीचे दी गई पंक्तियों में प्रकट हो रहे भावों से उनका मिलान कीजिए।
उत्तर:
| क्रम | पंक्तियाँ | भाववाचक संज्ञा |
|---|---|---|
| 1. | वह लज्जित होकर कहने लगे- ‘नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी।’ | लज्जा / पछतावा |
| 2. | दुख के उपर्युक्त उच्च वचन सुनकर उनकी आँखें खुल गईं। | बोध / आत्मज्ञान |
| 3. | उनके मन में कुछ दया आ गई। | करुणा / दया |
| 4. | इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। | आस्था / विश्वास |
| 5. | महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। | विनम्रता / विनय |
| 6. | अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। | जुड़ाव / लगाव |
| 7. | जमींदार साहब धन-मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। | अहंकार / घमंड |
| 8. | उस झोंपड़ी में उनका मन ऐसा कुछ लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। | जुड़ाव / लगाव |
| 9. | जब उसे अपनी पूर्वस्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट-फूट कर रोने लगी थी। | दुख / पीड़ा |
| 10. | बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की धोती गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। | क्रूरता / अन्याय |
| विश्लेषण: ये मिलान कहानी के भावनात्मक गहराई को दर्शाते हैं (पेज 11)। |
वाक्य विस्तार
प्रश्न: नीचे दिए गए वाक्यों का विस्तार करें (15-20 शब्द):
उत्तर:
- एक झोंपड़ी थी: एक पुरानी, स्मृतियों से भरी झोंपड़ी थी, जहाँ वृद्धा अपनी पोती के साथ दुख-सुख में रहती थी।
- श्रीमान टहल रहे थे: श्रीमान जमींदार अपने विशाल महल के अहाते में टहल रहे थे, नौकरों को काम सौंपते हुए।
- वह रोने लगी: वृद्धा अपनी झोंपड़ी की यादों में खोकर, आँसुओं के साथ दुख में फूट-फूट कर रोने लगी।
- चूल्हा बनाया: वृद्धा ने अपनी पोती के लिए झोंपड़ी की मिट्टी से चूल्हा बनाया, ताकि वह रोटी खाए।
- आगे बढ़ो: वृद्धा ने कांपते कदमों और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पोती के लिए आगे बढ़ने का हौसला दिखाया।
विश्लेषण: ये विस्तार कहानी के संदर्भ को गहराई देते हैं (पेज 12)।
पेज 12: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): यदि कहानी आज के समय की हो, तो जमींदार वृद्धा की पोती को समर्पण करने के लिए फोन करता है। उनकी बातचीत लिखें।
उत्तर:
- जमींदार: सुनो, तुम्हारी दादी की झोंपड़ी मेरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। तुम्हें हर सुविधा दूँगा, छोड़ दो।
- पोती: महाराज, यह झोंपड़ी मेरी दादी की यादों का घर है। इसे छोड़ना हमारे लिए असंभव है।
- जमींदार: अरे, मैं तुम्हें नया घर दूँगा, क्या कमी रह जाएगी?
- पोती: नया घर यादों की जगह नहीं ले सकता। कृपया इसे हमें वापस दे दें।
विश्लेषण: यह संवाद पोती के लगाव और जमींदार के लालच को दर्शाता है (पेज 12)।
प्रश्न (ख): जमींदार का मित्र उसे झोंपड़ी छोड़ने की सलाह देता है। उनकी बातचीत लिखें।
उत्तर:
- मित्र: जमींदार जी, इस झोंपड़ी को छोड़ दीजिए। यह वृद्धा की आखिरी उम्मीद है।
- जमींदार: मुझे उपदेश मत दो। यह मेरे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है।
- मित्र: धन से ज्यादा मानवता महत्वपूर्ण है। उसकी दुखभरी कहानी सुनकर आपका मन भी पिघल जाएगा।
- जमींदार: ठीक है, मैं सोचूँगा। शायद तुम सही हो।
विश्लेषण: यह संवाद मित्र की सलाह और जमींदार के अहंकार को दर्शाता है (पेज 12)।
प्रश्न (ग): पोती की डायरी:
उत्तर:
मेरी डायरी
2 मई – आज दादी बहुत परेशान थीं। उन्होंने बताया कि जमींदार ने हमारी झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। यह घर मेरी दादी की यादों का खजाना है। मेरे पिता और दादाजी की स्मृतियाँ यहाँ बसी हैं। मैंने खाना-पीना छोड़ दिया, क्योंकि यह मेरा घर है। दादी मिट्टी लेने गई थीं, ताकि चूल्हा बनाकर मुझे रोटी खिलाएँ। मुझे उम्मीद है कि जमींदार का मन बदलेगा।
विश्लेषण: डायरी पोती के गहरे लगाव को दर्शाती है (पेज 12)।
पेज 13: पाठ से आगे
प्रश्न (क): पोती अपने घर से बहुत प्यार करती थी। अपने घर के प्रति लगाव का अनुभव बताएँ।
उत्तर: मेरा घर मेरे लिए बहुत खास है। यह वह जगह है जहाँ मैंने अपने दादाजी के साथ कहानियाँ सुनीं। हर कोना उनकी यादों से भरा है। इसे छोड़ना मेरे लिए असंभव है।
विश्लेषण: यह अनुभव कहानी के लगाव के भाव से मेल खाता है (पेज 13)।
प्रश्न (ख): क्या आपको किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से इतना लगाव हुआ है?
उत्तर: हाँ, मुझे अपनी दादी की दी हुई अंगूठी से बहुत लगाव है। यह उनकी निशानी है। जब भी मैं उदास होती हूँ, इसे देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। इसे खोना मेरे लिए असहनीय होगा।
विश्लेषण: यह व्यक्तिगत अनुभव कहानी के भाव से जुड़ता है (पेज 13)।
प्रश्न (ग): क्या आपने किसी को पश्चाताप करते देखा है?
उत्तर: हाँ, मेरे दोस्त ने एक बार गुस्से में मुझसे झूठ बोला था। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी माँगी, और हमारा रिश्ता फिर से मधुर हो गया।
परिणाम: पश्चाताप ने हमारे बीच विश्वास बहाल किया।
विश्लेषण: यह जमींदार के पश्चाताप से मेल खाता है (पेज 13)।
प्रश्न (घ): क्या आपने अहंकार में कोई काम किया और पछताए?
उत्तर: हाँ, एक बार मैंने अहंकार में अपने सहपाठी की मदद करने से मना कर दिया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह गलत था। मैंने उससे माफी माँगी और उसकी मदद की।
सीख: मैंने सीखा कि दया और सहायता दूसरों के साथ संबंध मधुर बनाती है।
विश्लेषण: यह कहानी के संदेश से मेल खाता है (पेज 13)।
न्याय और समता
प्रश्न (क): क्या आपने ऐसा अन्याय देखा, पढ़ा या सुना है?
उत्तर: हाँ, मैंने सुना कि एक गाँव में एक गरीब परिवार का खेत एक अमीर व्यक्ति ने जबरन ले लिया। परिवार ने कोर्ट में केस किया और अंत में उन्हें उनका खेत वापस मिला।
विश्लेषण: यह कहानी के अन्याय से मिलता-जुलता है (पेज 13)।
प्रश्न (ख): ऐसी स्थितियों में निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
उत्तर:
- मैं: कानूनी सहायता लूँगा, जैसे वकील या NGO से मदद।
- आस-पास के लोग: सामुदायिक समर्थन, जागरूकता फैलाना, और सामाजिक संगठनों की मदद लेना।
विश्लेषण: यह सामाजिक न्याय के लिए कदमों को दर्शाता है (पेज 13)।
प्रश्न (ग): “सच्ची शक्ति दया और न्याय में है।” अपने विचार लिखें।
उत्तर: यह कथन सत्य है। दया और न्याय से समाज में शांति और समानता आती है। जमींदार ने जब दया दिखाई, तो वृद्धा को उसका घर मिला। यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति धन में नहीं, बल्कि करुणा और सही कार्य में है।
विश्लेषण: यह कहानी के मुख्य संदेश को रेखांकित करता है (पेज 13)।
पेज 14: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: अपने घर की कहानी की खोजबीन करें।
उत्तर: मेरे घर की कहानी मेरे दादाजी से शुरू होती है। उन्होंने 40 साल पहले इसे बनवाया था। इसे बनाने के लिए उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और परिवार की मदद से ईंट-गारा जोड़ा। यह घर हमारी एकता और प्यार का प्रतीक है।
विश्लेषण: यह गतिविधि घर के प्रति लगाव को समझने में मदद करती है (पेज 14)।
न्याय और करुणा से जुड़ी सहायता
प्रश्न: नागरिक शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दें।
उत्तर:
- सार्वजनिक शिकायत सुविधा: https://pgportal.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
- जनसुनवाई: https://jansunwai.up.nic.in पर स्थानीय समस्याओं का समाधान।
- सामाजिक कल्याण योजनाएँ: https://eshram.gov.in/hi/social-security-welfare-schemes पर जानकारी।
जागरूकता: मैं अपने परिवार को इन वेबसाइटों के बारे में बताऊँगा ताकि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें।
विश्लेषण: ये संसाधन नागरिकों को सशक्त बनाते हैं (पेज 14)।
आज की पहेली
प्रश्न: नीचे दिए गए शब्दों से सही शब्द बनाएँ।
उत्तर:
- ट क री इ ये = टोकरी
- व आ द = वृद्धा
- है ल व क = हतप्रभ
- बू ओ इ प इ द अ = बूढ़ी प्यारी
- ज द आ म इ र इ अ = जमींदार साहब
- त आ इ ई ओ क ल = ताई की टोकरी
- ता = ताकत
विश्लेषण: ये शब्द कहानी के संदर्भ में सटीक हैं (पेज 14)।
पेज 15: खोजबीन के लिए
प्रश्न: पंचतंत्र की एक कहानी पढ़ें और कक्षा में सुनाएँ।
उत्तर: मैंने पंचतंत्र की कहानी “दो मित्र और भालू” पढ़ी। यह कहानी दो मित्रों की यात्रा और एक भालू से मुलाकात की है। एक मित्र खतरे में पेड़ पर चढ़ जाता है, जबकि दूसरा जमीन पर लेटकर भालू से बचता है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे। मैं इसे कक्षा में नाटक के रूप में सुनाऊँगा।
विश्लेषण: यह गतिविधि कहानी कहने की परंपरा को जीवित रखती है (पेज 15)।
अध्याय 7- मत बं|धो: नोट्स प्रश्न-उत्तर रूप में
कवि: महादेवी वर्मा
प्रश्न 1: कविता का शीर्षक “मत बंधो” क्या संदेश देता है?
उत्तर 1: शीर्षक “मत बंधो” सपनों की स्वतंत्रता और उनकी गति को न रोकने का संदेश देता है, जो प्रगति और सृजन का आधार हैं (पेज 2)।
प्रश्न 2: कविता का मुख्य भाव क्या है?
उत्तर 2: कविता का मुख्य भाव यह है कि सपनों को बंधन में नहीं बाँधना चाहिए, क्योंकि वे प्रेरणा, स्वतंत्रता और सृजन का स्रोत हैं (पेज 2)।
प्रश्न 3: कविता में सपनों की तुलना किन-किन चीजों से की गई है?
उत्तर 3: सपनों की तुलना पक्षियों, बीजों, और अग्नि से की गई है, जो उनकी स्वतंत्रता, विकास, और ऊर्जा को दर्शाते हैं (पेज 3, 6)।
प्रश्न 4: “आरोहण” और “अवरोहण” का क्या अर्थ है, और इनका कविता में महत्व क्या है?
उत्तर 4: “आरोहण” का अर्थ ऊपर उठना और “अवरोहण” का अर्थ नीचे उतरना है। कविता में ये सपनों की गतिशीलता और उनके चक्र को दर्शाते हैं, जो जीवन में उतार-चढ़ाव का प्रतीक हैं (पेज 7)।
प्रश्न 5: कविता में शिल्प और कला का क्या महत्व बताया गया है?
उत्तर 5: शिल्प और कला को स्वर्ग बनाने का साधन बताया गया है, जो सपनों को वास्तविकता में बदलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं (पेज 8, 12)।
प्रश्न 6: कविता की शैली की विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर 6: कविता में प्रश्नोत्तरी शैली, विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग, समानार्थी शब्द, संयोजन, और सपनों का मानवीकरण जैसी विशेषताएँ हैं, जो इसे प्रभावशाली बनाती हैं (पेज 6)।
प्रश्न 7: कविता में सपनों की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर 7: सपनों की स्वतंत्रता इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रेरणा, सृजन, और मानव की उन्नति का आधार हैं। उन्हें रोकने से प्रगति रुकती है (पेज 2, 3)।
प्रश्न 8: कविता का संदेश हमारे जीवन से कैसे जुड़ता है?
उत्तर 8: कविता हमें सिखाती है कि सपनों को स्वतंत्र रखकर और कला व शिल्प के माध्यम से उन्हें साकार करके हम अपने जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बना सकते हैं (पेज 8, 10)।
अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (केवल हिंदी में)
पेज 2: मेरी समझ से
प्रश्न (क): निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के समक्ष तारा (★) बनाइए।
- आप इनमें से कविता का मुख्य भाव क्या समझते हैं?
- सपने मात्र कल्पनाएँ हैं
- सपनों को भूल जाना चाहिए
- सपनों की स्वतंत्रता नहीं चाहिए
- सपने देखना अच्छी बात है (★)
विश्लेषण: कविता सपनों को प्रेरणा और सृजन का स्रोत बताती है (पेज 2)।
- “मत बंधो” कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है?
- प्रेम की
- शिक्षा की
- सपनों की (★)
- अधिकार की
विश्लेषण: कविता सपनों की स्वतंत्रता पर जोर देती है (पेज 2)।
प्रश्न (ख): हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?
उत्तर: मैंने ये उत्तर इसलिए चुने:
- प्रश्न 1: सपने देखना अच्छी बात है, क्योंकि कविता सपनों को प्रेरणा और सृजन का आधार बताती है।
- प्रश्न 2: कविता स्पष्ट रूप से सपनों की स्वतंत्रता की बात करती है, न कि प्रेम, शिक्षा या अधिकार की।
चर्चा: समूह में हमने माना कि सपने जीवन को दिशा और प्रेरणा देते हैं (पेज 2)।
पेज 3: पंक्तियों पर चर्चा
प्रश्न (क): “शौरभ डूब जाता है नम में…”
उत्तर: इस पंक्ति का अर्थ है कि सपने (शौरभ) अगर बंधनों (नम) में डूब जाएँ, तो वे अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। बीज यदि मिट्टी में गिरकर नम हो जाए, तो वह उड़ नहीं सकता, यानी सपनों को बंधनों से मुक्त रखना चाहिए।
चर्चा: समूह में हमने माना कि यह पंक्ति सपनों की स्वतंत्रता और उनकी गतिशीलता को दर्शाती है (पेज 3)।
प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के समक्ष तारा (★) बनाइए।
- “इन सपनों के पंख न काटो” पंक्ति में सपनों के “पंख” होने की कल्पना किस गहराई की बात है?
- सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं (★)
- सपने पहचान की ऊँचाइयों तक ले जाते हैं
- सपने पक्षियों की तरह उन्मन भाव से उड़ते हैं
- सपने पक्षियों की तरह कोमल और नाजुक प्रकार के होते हैं
विश्लेषण: पंख सपनों की प्रेरणा और स्वतंत्रता को दर्शाते हैं (पेज 3)।
- “सपनों वसंत का फिर कोई शिल्प” पंक्ति में “सपनों” से आप क्या समझते हैं?
- जहाँ किसी पक्षी का सांनातिक कष्ट न हो
- जहाँ अनुत्तमीय पर स्वतंत्रता हो (★)
- जहाँ पक्षी सहायकों पर आधारित हों
- जहाँ सभी प्राणी एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील हों
विश्लेषण: सपने स्वतंत्रता और सृजन का प्रतीक हैं (पेज 3)।
- यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या हो सकता है?
- वह बहुत तेजी से उग सकता है
- वह और गहरा हो सकता है
- उसकी उड़ान रुक सकती है (★)
- वह बढ़कर सीधा बन सकता है
विश्लेषण: धूल में गिरा बीज उड़ नहीं सकता, जैसे बंधन में सपने रुक जाते हैं (पेज 3)।
प्रश्न (ख): अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?
उत्तर: मैंने ये उत्तर इसलिए चुने:
- प्रश्न 3: पंख प्रेरणा का प्रतीक हैं, जो सपनों को नया करने की शक्ति देते हैं।
- प्रश्न 4: सपने स्वतंत्रता और सृजन का आधार हैं, जो अनुत्तमीय स्वतंत्रता को दर्शाते हैं।
- प्रश्न 5: धूल में गिरा बीज उड़ नहीं सकता, जो सपनों के बंधन को दर्शाता है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि सपनों की स्वतंत्रता प्रगति के लिए जरूरी है (पेज 3)।
पेज 4: मिलाकर करें मिलान
प्रश्न: कविता की पंक्तियों को उनके भाव या संदर्भ से मिलाएँ।
उत्तर:
| क्रम | पंक्तियाँ | भाव या संदर्भ |
|---|---|---|
| 1. | इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो! | स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की कुंजी है। (★) |
| 2. | नम तक जाने से मत रोको, धरती से उसको मत बोलो! | सपनों को ऊँचाइयों तक जाने से मत रोको। (★) |
| 3. | इसका आरोहण मत रोको! इसका अवरोहण मत बोलो! | सपनों के उतार-चढ़ाव को स्वीकार करें। (★) |
| विश्लेषण: ये मिलान सपनों की स्वतंत्रता और गतिशीलता को दर्शाते हैं (पेज 4)। |
पेज 5: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न (क): कविता में सपनों की गति न बाँधने की बात क्यों कही गई होगी?
उत्तर: सपनों की गति न बाँधने की बात इसलिए कही गई, क्योंकि सपने प्रेरणा और सृजन का स्रोत हैं। उन्हें रोकने से व्यक्ति की प्रगति और रचनात्मकता रुक सकती है। सपनों को स्वतंत्र छोड़ने से वे वास्तविकता में बदल सकते हैं (पेज 5)।
प्रश्न (ख): कविता में सौरभ, बीज, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को कैसे विशेष बताया गया है?
उत्तर:
- सौरभ: सपनों को सुगंध की तरह बताया, जो जीवन को आनंदमय बनाते हैं।
- बीज: सपने बीज की तरह हैं, जो उड़ सकते हैं और नई संभावनाएँ जन्म दे सकते हैं।
- अग्नि: सपने अग्नि की तरह हैं, जो ऊर्जा और प्रकाश देते हैं।
विशिष्टताएँ: ये उदाहरण सपनों की गतिशीलता, प्रेरणा, और सृजनशीलता को दर्शाते हैं (पेज 5)।
प्रश्न (ग): कविता में ‘आरोहण’ और ‘अवरोहण’ दोनों के महत्व की बात की गई है। उदाहरण देकर बताएँ कि आपने ‘आरोहण’ और ‘अवरोहण’ को कब-कब देखा?
उत्तर:
- आरोहण: जब मैंने स्कूल में निबंध प्रतियोगिता जीती, तो मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। यह मेरे सपनों का ऊपर उठना था।
- अवरोहण: जब मैं गणित में असफल हुआ, तो मुझे निराशा हुई, लेकिन इससे मैंने सीखा और मेहनत की।
विश्लेषण: ये उदाहरण सपनों के उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं (पेज 5)।
प्रश्न (घ): “सपनों में दोनों गति है: उड़ने और अबोध में साता है” इसका क्या अर्थ है?
उत्तर: इसका अर्थ है कि सपने उड़ान (आरोहण) और उतरने (अवरोहण) दोनों की गति रखते हैं। मेरे अनुभव में, जब मैंने गायन सीखने का सपना देखा, तो मैंने मेहनत की (आरोहण), और जब असफलता मिली, तो मैंने धैर्य रखा (अवरोहण), जिससे मेरा सपना वास्तविकता बना।
विश्लेषण: यह सपनों की गतिशीलता को दर्शाता है (पेज 5)।
प्रश्न (ङ): कविता का शीर्षक है ‘मत बंधो’। यदि आपको इस कविता को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे?
उत्तर: मैं कविता का नाम “सपनों की उड़ान” दूँगा।
कारण: यह नाम सपनों की स्वतंत्रता और उनकी गतिशीलता को दर्शाता है, जो कविता का मुख्य भाव है (पेज 5)।
प्रश्न (च): मान लीजिए आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं? उस संसार में आप क्या-क्या रखना चाहेंगे और क्या-क्या नहीं?
उत्तर:
- रखना चाहूँगा: समानता, शिक्षा, कला, प्रकृति, और सहानुभूति, ताकि सभी खुश और प्रेरित रहें।
- नहीं रखूँगा: अन्याय, भेदभाव, और हिंसा, क्योंकि ये सपनों को बाँधते हैं।
विश्लेषण: यह सपनों की स्वतंत्रता और कविता के संदेश से प्रेरित है (पेज 5)।
प्रश्न (छ): कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात की गई है। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन-सी कला सीखना चाहेंगे?
उत्तर: मैं चित्रकला सीखना चाहूँगा। यह मेरे विचारों को रंगों और आकृतियों के माध्यम से व्यक्त करने में मदद करेगी, जिससे मेरा जीवन सुंदर और रचनात्मक बनेगा।
विश्लेषण: कला जीवन को सृजनात्मक बनाती है (पेज 5)।
प्रश्न (ज): “शौरभ डूब जाता है नम में/ फिर वह लौट कहाँ आता है?” यदि आपको अपने बीत हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो आप बीत चुके समय में क्या-क्या परिवर्तन करना चाहेंगे?
उत्तर: मैं अपने स्कूल के समय में लौटकर अधिक मेहनत करना चाहूँगा, विशेषकर गणित में, ताकि बेहतर अंक प्राप्त कर सकूँ। साथ ही, अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना चाहूँगा।
विश्लेषण: यह सपनों को साकार करने की प्रेरणा से जुड़ा है (पेज 5)।
प्रश्न (झ): “बीज धूल में गिर जाता जो/ वह नम में कब उड़ पाता है?” यदि सपने बीज की तरह हों तो उन्हें अपने लिए किन बीजों की आवश्यकता होगी?
उत्तर: सपनों के लिए प्रेरणा, मेहनत, धैर्य, और अवसर जैसे बीजों की आवश्यकता होगी। जैसे पौधे को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही सपनों को समर्थन और स्वतंत्रता चाहिए।
विश्लेषण: यह सपनों की स्वतंत्रता और विकास को दर्शाता है (पेज 5)।
प्रश्न (ञ): “स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प, भूमि को खिलवायेगा!” यदि आपके पास स्वर्ग बनाने का शिल्प या विचारों का स्वर्ग बनाया जा सकता है, तो आपके सपनों या विचारों में क्या होगा?
उत्तर: मेरे स्वर्ग में शिक्षा, समानता, और प्रकृति का संरक्षण होगा। मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने सपनों को स्वतंत्रता से जी सके। इसे बचाने के लिए मैं शिक्षा और जागरूकता फैलाऊँगा।
विश्लेषण: यह कविता के सृजनात्मक संदेश से जुड़ा है (पेज 5)।
पेज 6: कविता की रचना
प्रश्न (क): अपने समूह के साथ मिलकर कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए।
उत्तर:
- विपरीतार्थक शब्द: जैसे “आरोहण” और “अवरोहण”।
- पुनरावृत्ति: “मत बंधो” का बार-बार प्रयोग।
- समानार्थी शब्द: सपनों के लिए सौरभ, बीज, अग्नि।
- प्रश्नोत्तरी शैली: “वह नम में कब उड़ पाता है?”
- संयोजन: “और”, “फिर” जैसे शब्दों का प्रयोग।
- मानवीकरण: सपनों को पंख और गति के साथ चित्रित करना।
चर्चा: समूह में हमने इन विशेषताओं को कविता की प्रभावशीलता का आधार माना (पेज 6)।
प्रश्न (ख): विशेषताओं का पंक्तियों से मिलान कीजिए।
उत्तर:
| क्रम | विशेषता | पंक्ति |
|---|---|---|
| 1. | विपरीतार्थक शब्द | इसका आरोहण मत रोको! इसका अवरोहण मत बोलो! |
| 2. | पुनरावृत्ति | इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो! |
| 3. | समानार्थी शब्द | स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को खिलवायेगा! |
| 4. | प्रश्न पूछा गया | वह नम में कब उड़ पाता है? |
| 5. | संयोजन | दीप्ति लिए मूँह भर आयेगा! स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प… |
| 6. | सपनों का मानवीकरण | इन सपनों के पंख न काटो |
| विश्लेषण: ये मिलान कविता की शैली को स्पष्ट करते हैं (पेज 6)। |
पेज 7: शब्दों की बात
प्रश्न (क): रिक्त स्थान में ‘आरोहण’ और ‘अवरोहण’ भरे जाएँ।
उत्तर: यह पंक्ति पहले ही पूरी है: “इसका आरोहण मत रोको! इसका अवरोहण मत बोलो!”
विश्लेषण: यह पंक्ति सपनों की गतिशीलता को दर्शाती है (पेज 7)।
पेज 8: शब्दकोश से
प्रश्न: “शिल्प” शब्द से संबंधित शब्दों के अर्थ लिखिए।
उत्तर:
- शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजनों, शिल्पकर्म, शिल्पिक, शिल्पकार्य: कारीगर जो कला या हस्तशिल्प बनाता है।
- शिल्पकला: शिल्प की कला, जैसे मूर्तिकला या चित्रकला।
- शिल्पकौशल: शिल्प में निपुणता या कुशलता।
- शिल्पगुण, शिल्पौघ: शिल्प की विशेषता या गुणवत्ता।
- शिल्पविद्या: शिल्प की शिक्षा या तकनीक।
- शिल्पशाला, शिल्पालय: वह स्थान जहाँ शिल्प कार्य होता है।
विश्लेषण: ये शब्द शिल्प के महत्व को दर्शाते हैं (पेज 8)।
प्रश्न (क): कविता में वर्तमान काल की पंक्तियों को भूतकाल और भविष्य काल में लिखिए।
उत्तर:
- वर्तमान: इन सपनों के पंख न काटो।
- भूतकाल: इन सपनों के पंख न काटे।
- भविष्य काल: इन सपनों के पंख न काटना।
- वर्तमान: इसका आरोहण मत रोको!
- भूतकाल: इसका आरोहण मत रोका!
- भविष्य काल: इसका आरोहण मत रोकना!
- वर्तमान: स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को खिलवायेगा।
- भूतकाल: स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को खिलवाया।
- भविष्य काल: स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को खिलवायेगा।
विश्लेषण: ये परिवर्तन कविता के काल को स्पष्ट करते हैं (पेज 8)।
प्रश्न (ख): आप “बाँधने” का प्रयोग किन-किन स्थितियों या वस्तुओं के लिए करते हैं?
उत्तर:
- स्थितियाँ: विचारों को बाँधना, स्वतंत्रता को बाँधना, प्रगति को बाँधना।
- वस्तुएँ: रस्सी से सामान बाँधना, कपड़े से बाल बाँधना।
विश्लेषण: यह कविता के बंधन के संदेश से जुड़ा है (पेज 8)।
प्रश्न (ग): आपने घर, आस-पास और विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए क्या-क्या प्रयास करेंगे?
उत्तर:
- घर: साफ-सफाई, पौधे लगाना, और दीवारों पर चित्रकला।
- आस-पास: कचरा प्रबंधन, पेड़ लगाना, और जागरूकता फैलाना।
- विद्यालय: दीवारों पर चित्रकारी, पुस्तकालय को व्यवस्थित करना, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।
चर्चा: समूह में हमने माना कि ये प्रयास जीवन को सुंदर बनाते हैं (पेज 8)।
प्रश्न (घ): आपका कौन-सा सपना ऐसा है जो सिद्ध होने पर दूसरों की सहायता कर सकता है?
उत्तर: मेरा सपना एक शिक्षक बनने का है। यह सिद्ध होने पर मैं बच्चों को शिक्षा देकर उनके सपनों को साकार करने में मदद कर सकता हूँ।
विश्लेषण: यह कविता के सामाजिक संदेश से जुड़ा है (पेज 8)।
पेज 10: कविता आगे बढ़ाइए
प्रश्न (क): नीचे दी गई पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए, अपनी एक कविता तैयार कीजिए।
उत्तर:
इस सपनों के पंख न काटो
इस सपनों की गति मत बांधो
उनके रंगों को उड़ने दो
स्वर्ग की राहें बनने दो।
विश्लेषण: यह कविता सपनों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है (पेज 10)।
प्रश्न (ख): मान लीजिए आपका सपना खो गया हो। उसके खो जाने की रिपोर्ट तैयार करें।
उत्तर:
प्रिय प्राचार्य महोदय,
विषय: खोए हुए सपने की रिपोर्ट
मैं, कक्षा 10 का छात्र, सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा सपना, एक वैज्ञानिक बनने का, कुछ बंधनों के कारण खो गया है। समय की कमी और संसाधनों की कमी ने इसे प्रभावित किया। कृपया मुझे मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करें ताकि मैं अपने सपने को पुनर्जनन कर सकूँ।
धन्यवाद,
[आपका नाम]
विश्लेषण: यह सपनों के महत्व को दर्शाता है (पेज 10)।
प्रश्न (ग): वाद-विवाद: “स्वतंत्रता बीज सपनों की उसकी कल्पना और विचारों की नहीं।”
उत्तर:
- समूह 1 (विपक्ष में): स्वतंत्रता केवल सपनों की नहीं, बल्कि कल्पना और विचारों की भी है। विचार और कल्पना सपनों को जन्म देते हैं।
- समूह 2 (पक्ष में): स्वतंत्रता सपनों की है, क्योंकि सपने ही प्रेरणा का स्रोत हैं।
अनुच्छेद: वाद-विवाद से मैंने सीखा कि स्वतंत्रता सपनों, कल्पना, और विचारों, तीनों के लिए जरूरी है। बिना विचारों के सपने अधूरे हैं, और बिना स्वतंत्रता के कोई सृजन संभव नहीं।
विश्लेषण: यह कविता के संदेश को गहराई देता है (पेज 10)।
पेज 12: शिल्प-कार्य मिलान
प्रश्न: शिल्प-कार्य को उनके अर्थ या व्याख्या से मिलाइए।
उत्तर:
| शिल्प-कार्य | अर्थ या व्याख्या |
|---|---|
| 1. काँच शिल्प | काँच से मूर्तियाँ, सजावटी वस्तुएँ और शीशे की खिड़कियाँ आदि बनाना (★) |
| 2. मिट्टी शिल्प | मिट्टी से बर्तन, मूर्तियाँ, और सजावटी वस्तुएँ बनाना (★) |
| 3. कागज शिल्प | कागज से खिलौने, सजावट, और पेपर मेशी बनाना (★) |
| 4. लकड़ी शिल्प | लकड़ी से वस्तुएँ, खिलौने, मेज आदि बनाना (★) |
| 5. धातु शिल्प | धातु से बर्तन, मूर्तियाँ, और सजावटी जेवर बनाना (★) |
| 6. काष्ठ शिल्प | लकड़ी, पत्थर या धातु पर नक्काशी जैसे डिजाइन बनाना (★) |
| 7. चित्र शिल्प | पारंपरिक चित्रकला जैसे मूर्तियाँ, थंग्का आदि से कलाकृतियाँ बनाना (★) |
| 8. चमड़ा शिल्प | चमड़े से बटुआ, बैग, और सजावटी वस्तुएँ बनाना (★) |
| 9. बाँस और बेंत शिल्प | बाँस और बेंत से टोकरियाँ, कुर्सियाँ, और चटाई बनाना (★) |
| 10. मिट्टी एवं आभूषण शिल्प | मिट्टी से बने आभूषण और सजावटी वस्तुएँ बनाना (★) |
| 11. लाख शिल्प | लाख से खिलौने, डिब्बे और सजावटी वस्तुएँ बनाना (★) |
| 12. रेशा शिल्प | रेशों से चटाई, बेंत, और अन्य उपयोगी वस्तुएँ बनाना (★) |
| 13. चिककन शिल्प | सन या अन्य रेशों से मूर्तियाँ, मेज की सजावट आदि बनाना (★) |
| 14. नक्काशी शिल्प | पत्थर, मिट्टी या धातु पर मूर्तियाँ, डिजाइन आदि बनाना (★) |
| विश्लेषण: ये मिलान शिल्प की विविधता को दर्शाते हैं (पेज 12)। |
पेज 13: झरोखे से
प्रश्न (क): अपने विद्यालय या परिवार के साथ हस्तशिल्प से जुड़े किसी स्थान या कार्यशाला का भ्रमण करें और उस हस्तशिल्प के बारे में एक रिपोर्ट बनाएँ।
उत्तर:
रिपोर्ट: मिट्टी शिल्प कार्यशाला भ्रमण
मैंने अपने परिवार के साथ स्थानीय मिट्टी शिल्प कार्यशाला का भ्रमण किया। वहाँ कारीगर मिट्टी से बर्तन, मूर्तियाँ, और सजावटी वस्तुएँ बना रहे थे। मैंने देखा कि वे मिट्टी को गूँथकर, चाक पर आकार देकर, और फिर भट्टी में पकाकर वस्तुएँ तैयार करते हैं। यह शिल्प धैर्य और कौशल का प्रतीक है।
विश्लेषण: यह शिल्प के महत्व को दर्शाता है (पेज 13)।
प्रश्न (ख): राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय की वेबसाइट में कौन-सी हस्तशिल्प या कलाकृति सबसे अच्छी लगी?
उत्तर: राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय (https://nationalcraftsmuseum.nic.in/) पर मुझे मधुबनी चित्रकला सबसे अच्छी लगी। इसके रंग और जटिल डिजाइन प्रकृति और संस्कृति को दर्शाते हैं। यह कला बिहार की परंपरा को जीवित रखती है।
विश्लेषण: यह कविता के शिल्प और सृजन के संदेश से जुड़ा है (पेज 13)।
अध्याय 8-नए मेहमान: नोट्स प्रश्न-उत्तर रूप में
लेखक: उदयशंकर भट्ट
प्रश्न 1: एकांकी का शीर्षक “नए मेहमान” क्या संदेश देता है?
उत्तर 1: शीर्षक “नए मेहमान” आतिथ्य की भारतीय परंपरा और अप्रत्याशित मेहमानों के आगमन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दर्शाता है, जो परिवार की कठिनाइयों के बावजूद उनके सत्कार को उजागर करता है (पेज 1)।
प्रश्न 2: एकांकी का मुख्य विषय क्या है?
उत्तर 2: एकांकी का मुख्य विषय मध्यमवर्गीय परिवार की आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयाँ, भीषण गर्मी, और मेहमानों के प्रति आतिथ्य की भावना है, जो सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाता है (पेज 1, 2)।
प्रश्न 3: विश्वनाथ और रेवती के जीवन में क्या समस्याएँ हैं?
उत्तर 3: विश्वनाथ और रेवती किराए के छोटे मकान में रहते हैं, जहाँ गर्मी, पानी की कमी, और पड़ोसियों का असहयोग उनकी समस्याएँ हैं। रेवती को सिरदर्द और विश्वनाथ को काम का तनाव है (पेज 2, 3, 7)।
प्रश्न 4: नन्हेमल और बाबूलाल का व्यवहार कैसा है?
उत्तर 4: नन्हेमल और बाबूलाल अपरिचित मेहमान हैं, जो बिना स्पष्ट परिचय के विश्वनाथ के घर आते हैं। उनका व्यवहार लापरवाह और अस्पष्ट है, जिससे विश्वनाथ और रेवती को असुविधा होती है (पेज 5, 6, 10)।
प्रश्न 5: आमगुक के आगमन का क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर 5: आमगुक, रेवती का भाई, एक परिचित मेहमान के रूप में आता है। उसका आगमन रेवती को राहत देता है, और वह उसके लिए तुरंत खाना बनाने को तैयार हो जाती है, जो आतिथ्य की भावना को दर्शाता है (पेज 11, 12)।
प्रश्न 6: एकांकी में गर्मी की भीषणता को कैसे दर्शाया गया है?
उत्तर 6: गर्मी की भीषणता को पंक्तियों जैसे “सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो” और “प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती” के माध्यम से दर्शाया गया है, जो पात्रों की परेशानी को उजागर करता है (पेज 3, 15)।
प्रश्न 7: पड़ोसी का व्यवहार कैसा है और यह कहानी में क्या भूमिका निभाता है?
उत्तर 7: पड़ोसी असहयोगी और क्रोधी है, जो छत पर पानी फैलने पर शिकायत करता है। यह सामाजिक असंवेदनशीलता को दर्शाता है और परिवार की कठिनाइयों को बढ़ाता है (पेज 8, 9)।
प्रश्न 8: एकांकी में आतिथ्य की भावना कैसे उभरती है?
उत्तर 8: विश्वनाथ और रेवती, कठिनाइयों के बावजूद, मेहमानों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं, जो भारतीय संस्कृति में “अतिथि देवो भव” की परंपरा को दर्शाता है (पेज 8, 12, 21)।
अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (केवल हिंदी में)
पेज 13: मेरी समझ से
प्रश्न (क): निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के समक्ष तारा (★) बनाएँ। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं।
- आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को “शरीफ” लड़के किस संदर्भ में कहा?
- अतिथियों को सेवा करने के कारण (★)
- किसी तरह का प्रस्ताव न करने के कारण
- आज्ञाकारी के भाव के कारण (★)
- गर्मी को चुपचाप सहते के कारण
विश्लेषण: बच्चे मेहमानों को पानी और पंखा देने में मदद करते हैं, जो उनकी शराफत और आज्ञाकारिता को दर्शाता है (पेज 6)।
- “एक तो ये पड़ोसी हैं, निर्दयी…” विश्वनाथ ने अपने पड़ोसियों को निर्दयी क्यों कहा?
- उन्हें गम में देखकर प्रसन्न होते हैं (★)
- पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं (★)
- लड़ने-झगड़ने के अवसर बढ़ाते हैं
- अतिथियों का अपमान करते हैं
विश्लेषण: पड़ोसी छत पर खाट बिछाने की अनुमति नहीं देते और शिकायत करते हैं, जो उनकी निर्दयता को दर्शाता है (पेज 2, 9)।
- “ईश्वर करें इन दिनों कोई मेहमान न आए” रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही है?
- मेहमान के सत्कार की व्यवस्था न होने के कारण (★)
- रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक न होने के कारण (★)
- अतिथियों के आने से घर का खर्च बढ़ाने के कारण
- उस अतिथियों का आना-जाना पसंद न होने के कारण
विश्लेषण: रेवती को सिरदर्द है और घर में संसाधनों की कमी है, इसलिए वह मेहमानों के आने की कामना नहीं करती (पेज 3, 7)।
- “न भगवान कोई मुसीबत न आ जाए” रेवती कौन-सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है?
- पानी की कमी होने की
- पड़ोसियों के चिल्लाने की
- मेहमानों के आने की (★)
- गर्मी के कारण बीमारी की
विश्लेषण: रेवती अपरिचित मेहमानों के आगमन को मुसीबत मानती है, क्योंकि यह उनकी कठिनाइयों को बढ़ाता है (पेज 4, 7)।
प्रश्न (ख): अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?
उत्तर: मैंने ये उत्तर इसलिए चुने:
- प्रश्न 1: बच्चे मेहमानों की सेवा करते हैं और आज्ञाकारी हैं, जो उनकी शराफत को दर्शाता है।
- प्रश्न 2: पड़ोसी सहयोग नहीं करते और शिकायत करते हैं, जो उनकी निर्दयता को दिखाता है।
- प्रश्न 3: रेवती का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और संसाधनों की कमी है, इसलिए वह मेहमानों के आने से चिंतित है।
- प्रश्न 4: अपरिचित मेहमानों का आगमन रेवती के लिए मुसीबत है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि एकांकी मध्यमवर्गीय परिवार की कठिनाइयों और आतिथ्य की भावना को दर्शाती है (पेज 13)।
पेज 14: पंक्तियों पर चर्चा
प्रश्न: निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए और कक्षा में साझा कीजिए।
उत्तर:
- “पानी पीते-पीते पेट फुला जा रहा है, और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती।”
अर्थ: यह पंक्ति गर्मी की भीषणता को दर्शाती है, जहाँ बहुत पानी पीने के बावजूद प्यास नहीं बुझती, जो शारीरिक और मानसिक थकान को दिखाता है (पेज 2)। - “सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो।”
अर्थ: यह गर्मी की तीव्रता को चित्रित करता है, जैसे पूरा शहर आग की लपटों में हो (पेज 3)। - “घर तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं।”
अर्थ: यह परिवार की मजबूरी को दर्शाता है, जो छोटे मकान में गर्मी के कारण तप रहा है, जैसे चने भाड़ में भुनते हैं (पेज 7)। - “आह, अब जान में जान आई।”
अर्थ: यह पंक्ति पानी पीने के बाद राहत की अनुभूति को दर्शाती है, जो गर्मी में जीवन का आधार है (पेज 6)।
चर्चा: समूह में हमने माना कि ये पंक्तियाँ गर्मी और कठिनाइयों को प्रभावी ढंग से चित्रित करती हैं (पेज 14)।
पेज 14: मिलकर करें मिलान
प्रश्न: स्तंभ 1 की पंक्तियों को स्तंभ 2 के सही भावों से मिलाइए।
उत्तर:
| क्रम | स्तंभ 1 | स्तंभ 2 |
|---|---|---|
| 6. | लाखों के आदमी खाक में मिल गए। | बहुत ही समृद्ध दुकान के मालिक अब उनके पास कुछ भी नहीं है (★) |
| 7. | भोजन की व्यवस्था काम तक हो जाएगी | खाने में क्या हर-दर हो (★) |
| 8. | चोटी ऐसी चर रही है, जैसे पुरानी हो | कपड़ा पसीने से भीगकर पुराने जैसा हो गया है (★) |
| 9. | पहले अपना ध्यान फिर दूसरा काम | पहले आत्मा फिर परमात्मा (★) |
| 10. | माल-मसाला तो अँटी में है न? | धनराशि सुरक्षित तो है न! (★) |
| विश्लेषण: ये मिलान एकांकी के संदर्भ और भाव को स्पष्ट करते हैं (पेज 14)। |
पेज 15: सोच-विचार के लिए
प्रश्न (क): “शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं।” नन्हेमल का “ऐसे ही मकान” से क्या आशय है?
उत्तर: नन्हेमल का “ऐसे ही मकान” से आशय छोटे, तंग, और गर्म मकानों से है, जो शहरों में मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए आम हैं। ये मकान हवा और जगह की कमी से ग्रस्त हैं (पेज 6)।
प्रश्न (ख): पड़ोसी की विश्वनाथ से किस तरह की शिकायत है? आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित?
उत्तर:
- शिकायत: पड़ोसी की शिकायत है कि विश्वनाथ के मेहमानों ने छत पर पानी फैलाया, जिससे गंदगी हुई।
- उचित/अनुचित: पड़ोसी का व्यवहार अनुचित है। छोटी-सी गलती पर चिल्लाना और सहयोग न करना असंवेदनशीलता दर्शाता है। विश्वनाथ ने माफी माँगी और सफाई का वादा किया, फिर भी पड़ोसी क्रोधित रहा, जो उचित नहीं है (पेज 9)।
प्रश्न (ग): एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है। क्या?
उत्तर: विश्वनाथ उन्हें इसलिए घर में आने देता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में “अतिथि देवो भव” की परंपरा है। वह मेहमानों का सम्मान करता है, भले ही वे अपरिचित हों। यह उसकी उदारता और आतिथ्य की भावना को दर्शाता है (पेज 9, 21)।
प्रश्न (घ): एकांकी के उन वाक्यों को छाँटकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं।
उत्तर:
- “मैं संपताराम को नहीं जानता।” (पेज 6)
- “क्या पूछ लो? दो-तीन बार पूछा, ठीक-ठीक उत्तर ही नहीं देते।” (पेज 7)
- “जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए हैं।” (पेज 9)
- “पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ।” (पेज 11)
विश्लेषण: ये वाक्य नन्हेमल और बाबूलाल के अपरिचित होने को दर्शाते हैं (पेज 6, 7, 9, 11)।
प्रश्न (ङ): एकांकी के उन वाक्यों को छाँटकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है।
उत्तर:
- “बड़ी गर्मी है।” (पेज 2)
- “सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो।” (पेज 3)
- “पानी पीते-पीते पेट फुला जा रहा है, और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती।” (पेज 2)
- “चारों तरफ दीवारें तप रही हैं।” (पेज 4)
- “तमाम शरीर मारे गरमी के उबल उठा है।” (पेज 3)
विश्लेषण: ये वाक्य गर्मी की तीव्रता को दर्शाते हैं (पेज 2, 3, 4)।
पेज 15: अनुमान और कल्पना से
प्रश्न (क): विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है। साथ ही रेवती की अनिच्छा का विचार करके बाजार से भोजन का सुझाव भी देता है। लेकिन उनके स्वयं भोजन बनाने के विषय में क्यों नहीं सोचा?
उत्तर: विश्वनाथ ने स्वयं भोजन बनाने के बारे में इसलिए नहीं सोचा, क्योंकि सामाजिक परंपराओं में भोजन बनाना आमतौर पर महिलाओं का कार्य माना जाता था। रेवती घर की गृहिणी थी, और विश्वनाथ को काम पर जाना था, इसलिए उसने यह जिम्मेदारी रेवती पर छोड़ी। साथ ही, वह रेवती की अनिच्छा को समझता था, इसलिए बाजार से भोजन मँगाने का सुझाव दिया (पेज 8)।
प्रश्न (ख): विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों के प्रयोजन की व्यवस्था करता है और छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद को इस तरह के अनुरोध करने की क्या माँगें थीं?
उत्तर: प्रमोद को यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई, क्योंकि वह बड़ा बेटा था और परिवार में मदद करना उसका कर्तव्य था। वह मेहमानों को पानी, बरफ, और नल दिखाने जैसे कार्य करता है, जो उसकी आज्ञाकारिता और शराफत को दर्शाता है। साथ ही, वह अपनी छोटी बहन किरण का ध्यान रखता है, जो पारिवारिक जिम्मेदारी को दिखाता है (पेज 4, 5, 8)।
प्रश्न (ग): “कैसी बातें करते हो, भैया! मैं अभी खाना बनाती हूँ” भोजन, गर्मी और सिर में दर्द के बावजूद भी रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्यों तैयार हो गई होगी?
उत्तर: रेवती इसलिए तैयार हो गई, क्योंकि मेहमान उसका भाई आमगुक था, जो परिचित और प्रिय था। भारतीय संस्कृति में आतिथ्य को महत्व दिया जाता है, और रेवती ने अपने भाई के लिए सत्कार को प्राथमिकता दी, भले ही वह बीमार थी। यह उसकी पारिवारिक भावना और कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाता है (पेज 12)।
प्रश्न (घ): गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियों के स्थान पर सर्दी और वर्षा की भीषणता के लिए वाक्य लिखिए।
उत्तर:
| गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियाँ | सर्दी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियाँ | वर्षा की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियाँ |
|---|---|---|
| 1. यह गर्मी में भुन रहा है। | यह सर्दी में ठिठुर रहा है। | यह वर्षा में भीग रहा है। |
| 2. पर बरफ कोई कहीं तक पिया। | पर गर्म पानी कोई कहीं तक पिया। | पर छाता कोई कहीं तक लिया। |
| 3. सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। | सारे शहर में जैसे बर्फ गिर रही हो। | सारे शहर में जैसे पानी बरस रहा हो। |
| 4. प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। | ठंड है कि कम होने का नाम नहीं लेती। | गीलापन है कि सूखने का नाम नहीं लेता। |
| 5. चारों तरफ दीवारें तप रही हैं। | चारों तरफ दीवारें ठंडी हो रही हैं। | चारों तरफ दीवारें गीली हो रही हैं। |
| विश्लेषण: ये वाक्य मौसम की विभिन्न परिस्थितियों को दर्शाते हैं (पेज 15)। |
पेज 17: अभिनय की बारी
प्रश्न (क): क्या आपने कभी मंच पर कोई एकांकी या नाटक देखा है? यदि आपको अपने विद्यालय में इस एकांकी का मंचन करना हो, तो आप क्या-क्या करेंगे?
उत्तर: हाँ, मैंने स्कूल में एक नाटक देखा है। यदि मुझे “नए मेहमान” का मंचन करना हो, तो मैं निम्नलिखित करूँगा:
- पात्र चयन: विश्वनाथ, रेवती, नन्हेमल, बाबूलाल, और आमगुक के लिए उपयुक्त छात्र चुनूँगा।
- मंच सज्जा: छोटे मकान का दृश्य बनाने के लिए मेज, खाट, और पंखा रखूँगा।
- संवाद: संवादों को भावपूर्ण और स्वाभाविक तरीके से प्रस्तुत करवाऊँगा।
- परिवर्तन: गर्मी की भीषणता को और प्रभावी बनाने के लिए पंखे की आवाज और पसीने की अभिनय शैली जोड़ूँगा।
- पात्र: नन्हेमल और बाबूलाल को हास्यपूर्ण और विश्वनाथ को गंभीर दिखाऊँगा।
विश्लेषण: यह मंचन को रोचक और प्रभावी बनाएगा (पेज 17)।
प्रश्न (ख): अपने समूह में इस एकांकी को प्रस्तुत करने की तैयारी करें। कौन किस पात्र का अभिनय करेगा?
उत्तर:
- विश्वनाथ: समूह का गंभीर और जिम्मेदार छात्र।
- रेवती: एक संवेदनशील और भावपूर्ण छात्रा।
- नन्हेमल: हास्यपूर्ण और बातूनी छात्र।
- बाबूलाल: नन्हेमल का साथी, लापरवाह शैली वाला छात्र।
- आमगुक: शांत और परिचित पात्र के लिए उपयुक्त छात्र।
- प्रमोद और किरण: आज्ञाकारी और सहायक बच्चे।
विश्लेषण: यह चयन पात्रों के स्वभाव के अनुरूप है। मंचन 10-15 मिनट में पूरा होगा (पेज 17)।
पेज 18: भाषा की बात
प्रश्न: एकांकी में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले शब्दों को नोट करें।
उत्तर:
- पंखा करना: गर्मी में राहत के लिए हवा करना।
- पसीने से नहा गया: अत्यधिक गर्मी से पसीना बहना।
- गला सूखा जा रहा है: प्यास की तीव्रता।
- जान में जान आई: पानी पीने से राहत।
विश्लेषण: ये शब्द गर्मी और थकान को प्रभावी ढंग से दर्शाते हैं (पेज 18)।
प्रश्न: एकांकी में आए अन्य मुहावरों की पहचान करें और उनके अर्थ समझकर अपने वाक्यों में प्रयोग करें।
उत्तर:
- मुहावरा: दिन-रात एक करना (पेज 2)
अर्थ: बहुत मेहनत करना।
वाक्य: मैंने परीक्षा की तैयारी के लिए दिन-रात एक कर दिया। - मुहावरा: खाक में मिलना (पेज 5)
अर्थ: बर्बाद हो जाना।
वाक्य: उसकी गलत नीतियों से उसका व्यापार खाक में मिल गया। - मुहावरा: सिर फट रहा है (पेज 3)
अर्थ: तीव्र सिरदर्द होना।
वाक्य: गर्मी के कारण मेरा सिर फट रहा है।
विश्लेषण: ये मुहावरे संवादों को जीवंत बनाते हैं (पेज 18)।
प्रश्न (क): “ही” के प्रयोग से वाक्य में बल और उसके हटाने से कमी पर चर्चा करें।
उत्तर:
- वाक्य: “वह तो कहो, मैं भी ढूँढ़कर ही रहा।”
- “ही” का प्रभाव: यह ढूँढने की निश्चितता और दृढ़ता को दर्शाता है।
- “ही” हटाने पर: “वह तो कहो, मैं भी ढूँढकर रहा।” यह कम निश्चित और कम प्रभावी लगता है।
चर्चा: समूह में हमने माना कि “ही” वाक्य में जोर और विश्वास जोड़ता है (पेज 18)।
प्रश्न (ख): “ही” का प्रयोग करके वाक्य बनाएँ।
उत्तर:
- विश्वनाथ के अतिथि यहाँ बैठेंगे और किसी के अतिथि नहीं।
- विश्वनाथ के अतिथि यहाँ ही बैठेंगे और किसी के अतिथि नहीं।
- विश्वनाथ के अतिथि यहाँ बैठेंगे यहाँ के अतिरिक्त और कहीं नहीं।
- विश्वनाथ के अतिथि यहाँ ही बैठेंगे यहाँ के अतिरिक्त और कहीं नहीं।
- विश्वनाथ के अतिथि यहाँ बैठेंगे यहाँ रुकना निश्चित है।
- विश्वनाथ के अतिथि यहाँ ही बैठेंगे यहाँ रुकना निश्चित है।
विश्लेषण: “ही” वाक्य में निश्चितता और विशेषता जोड़ता है (पेज 18)।
- विश्वनाथ के अतिथि यहाँ ही बैठेंगे यहाँ रुकना निश्चित है।
प्रश्न: “तो” का स्थान बदलकर अर्थ में परिवर्तन देखें और नए वाक्य बनाएँ।
उत्तर:
- मूल वाक्य: तुम नहाने तो जाओ।
- अर्थ: नहाने पर जोर, सुझाव।
- परिवर्तित: तुम तो नहाने जाओ।
- अर्थ: तुम पर जोर, आश्चर्य या आग्रह।
- परिवर्तित: तुम नहाने जाओ तो।
- अर्थ: शर्त, जैसे नहाने के बाद कुछ होगा।
नए वाक्य:
- अर्थ: शर्त, जैसे नहाने के बाद कुछ होगा।
- ही: मैं खाना ही खाऊँगा। (खाने पर जोर)
- तो: तुम पढ़ाई तो करो। (पढ़ाई पर जोर)
- तो: तुम तो पढ़ाई करो। (तुम पर जोर)
विश्लेषण: “ही” और “तो” वाक्य के अर्थ को बदलते हैं (पेज 18)।
पेज 19: आपकी बात
प्रश्न (क): विश्वनाथ की स्थिति में आपके सामने कोई ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति आई है?
उत्तर: हाँ, एक बार मेरे घर एक अपरिचित व्यक्ति आया, जो मेरे पिता का दोस्त होने का दावा कर रहा था। हमें समझ नहीं आया कि उसे घर में बुलाएँ या नहीं। हमने पहले पिता से पुष्टि की, फिर उसका स्वागत किया। यह स्थिति विश्वनाथ की तरह थी, जहाँ अपरिचित मेहमानों को समझना मुश्किल था (पेज 7, 19)।
प्रश्न (ख): नन्हेमल और बाबूलाल अच्छे मित्र हैं। आपके अच्छे मित्र कौन हैं और क्यों?
उत्तर: मेरे अच्छे मित्र राहुल और प्रिया हैं। वे मुझे इसलिए पसंद हैं, क्योंकि वे मेरी मदद करते हैं, मेरे साथ समय बिताते हैं, और हम एक-दूसरे के सपनों को प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सकारात्मकता और सहयोग मुझे प्रेरित करता है (पेज 19)।
प्रश्न (ग): आप किसी संबंधी या मित्र के घर जाने से पहले क्या-क्या तैयारी करते हैं?
उत्तर: मैं निम्नलिखित तैयारियाँ करता हूँ:
- उनके आने की सूचना पहले देता हूँ।
- उनके पसंदीदा उपहार या मिठाई ले जाता हूँ।
- उनके घर की सुविधाओं के बारे में पूछता हूँ।
- समय पर पहुँचने की योजना बनाता हूँ।
विश्लेषण: यह मेहमानों के प्रति सम्मान को दर्शाता है (पेज 19)।
प्रश्न (घ): विश्वनाथ के पड़ोसी सहयोग नहीं करते। आप अपने पड़ोसियों का कैसे सहयोग करते हैं?
उत्तर: मैं अपने पड़ोसियों का निम्नलिखित तरीकों से सहयोग करता हूँ:
- उनके बच्चों को पढ़ाने में मदद करता हूँ।
- सामान लाने या छोटे कार्यों में सहायता करता हूँ।
- उत्सवों में उनके साथ शामिल होता हूँ।
विश्लेषण: यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ाता है (पेज 19)।
प्रश्न (ङ): नन्हेमल और बाबूलाल का व्यवहार सामान्य अतिथियों जैसा नहीं है। सामान्य अतिथियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए?
उत्तर: सामान्य अतिथियों का व्यवहार निम्नलिखित होना चाहिए:
- पहले से सूचना देना।
- मेजबान की सुविधाओं का सम्मान करना।
- स्पष्ट परिचय देना।
- अनावश्यक असुविधा न करना।
विश्लेषण: नन्हेमल और बाबूलाल का अस्पष्ट और लापरवाह व्यवहार मेजबान को परेशान करता है (पेज 19)।
पेज 19: सावधानी और सुरक्षा
प्रश्न (क): यदि आप विश्वनाथ के स्थान पर होते तो क्या करते?
उत्तर: मैं नन्हेमल और बाबूलाल से उनका स्पष्ट परिचय माँगता। यदि वे परिचित नहीं होते, तो उन्हें घर में आने से पहले उनके द्वारा बताए गए व्यक्ति से संपर्क करता। सावधानी के लिए, मैं उन्हें बाहर ही पानी और भोजन की व्यवस्था करता, ताकि परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो (पेज 19)।
प्रश्न (ख): यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आए तो आप क्या सावधानियाँ बरतेंगे?
उत्तर: मैं निम्नलिखित सावधानियाँ बरतूँगा:
- उनका परिचय और आने का उद्देश्य पूछूँगा।
- माता-पिता या अभिभावकों को सूचित करूँगा।
- बिना पुष्टि के उन्हें घर में प्रवेश नहीं दूँगा।
- पड़ोसियों या स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने की योजना रखूँगा।
विश्लेषण: यह सुरक्षा और सावधानी को सुनिश्चित करता है (पेज 19)।
पेज 19: सृजन
प्रश्न (क): एकांकी की कहानी को अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर: एक दिन मेरे घर में अप्रत्याशित मेहमान आए। हम एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे, जहाँ गर्मी बहुत थी। मेरे पिता ने मेहमानों का स्वागत किया, लेकिन हमें उनका परिचय समझ नहीं आया। माँ को सिरदर्द था, फिर भी उन्होंने मेहमानों के लिए खाना बनाने की तैयारी की। पड़ोसी ने छत पर पानी फैलने की शिकायत की। बाद में, माँ का भाई आया, जिससे हमें राहत मिली। हमने उसका सत्कार किया। यह अनुभव हमें आतिथ्य और कठिनाइयों के बीच संतुलन सिखाता है (पेज 19)।
प्रश्न: गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए क्या सावधानियाँ बरतेंगे?
उत्तर:
- पर्याप्त पानी पीना और बरफ का उपयोग करना।
- हल्के और सूती कपड़े पहनना।
- पंखे या कूलर का उपयोग करना।
- दोपहर में बाहर जाने से बचना।
- फल और हल्का भोजन खाना।
चर्चा: समूह में हमने इन बिंदुओं को चार्ट पर लिखा और बुलेटिन बोर्ड पर लगाया (पेज 19)।
पेज 20: तार से संदेश
प्रश्न (क): तार भेजने के आधार पर अनुमान लगाएँ कि यह एकांकी कितने वर्ष पहले लिखी गई होगी?
उत्तर: तार (टेलीग्राफ) का उल्लेख इंगित करता है कि यह एकांकी 20वीं सदी के मध्य में लिखी गई होगी, संभवतः 1940-1960 के बीच, जब तार संदेश भेजने का आम माध्यम था (पेज 20)।
प्रश्न (ख): आजकल संदेश भेजने के कौन-कौन से माध्यम सुलभ हैं?
उत्तर:
- व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और अन्य मैसेजिंग ऐप्स।
- ईमेल।
- मोबाइल फोन कॉल और एसएमएस।
- सोशल मीडिया जैसे एक्स, फेसबुक।
विश्लेषण: ये आधुनिक और तेज संचार माध्यम हैं (पेज 20)।
प्रश्न (ग): आप संदेश भेजने के लिए किस माध्यम का उपयोग करते हैं?
उत्तर: मैं व्हाट्सएप और ईमेल का उपयोग करता हूँ, क्योंकि ये तेज, सुविधाजनक, और मुफ्त हैं। तत्काल संदेश के लिए व्हाट्सएप और औपचारिक संदेश के लिए ईमेल उपयुक्त हैं (पेज 20)।
प्रश्न (घ): अपने किसी प्रिय व्यक्ति को पत्र लिखकर भारतीय डाक से भेजिए।
उत्तर:
पत्र:
प्रिय मित्र राहुल,
नमस्ते! आशा है तुम स्वस्थ हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने हाल ही में एक नाटक देखा, जो आतिथ्य पर आधारित था। यह मुझे तुम्हारी याद दिलाता है, क्योंकि तुम हमेशा मेहमानों का स्वागत करते हो। जल्दी मिलने की योजना बनाएँ।
तुम्हारा मित्र,
[आपका नाम]
विश्लेषण: यह पत्र डाक से भेजने के लिए तैयार है (पेज 20)।
पेज 20: नाप, तौल और मुद्राएँ
प्रश्न (क): एक रुपये में कितने आने होते हैं?
उत्तर: एक रुपये में 16 आने होते हैं (पेज 20)।
प्रश्न (ख): चार आने में कितने पैसे होते हैं?
उत्तर: एक आना में 12 पैसे होते हैं, इसलिए चार आने में 4 × 12 = 48 पैसे होते हैं (पेज 20)।
प्रश्न (ग): आपके आस-पास नाप शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है?
उत्तर: मेरे आस-पास नाप शब्द का प्रयोग कपड़े की सिलाई, जमीन की माप, और सामान की लंबाई-चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण: “कपड़े का नाप ले लो।” (पेज 20)।
प्रश्न (घ): एक गज में कितनी फीट होती हैं?
उत्तर: एक गज में 3 फीट होती हैं (पेज 20)।
पेज 21: साझी समझ
प्रश्न: अपने घर में अतिथियों का अभिवादन कैसे करते हैं और अपने क्षेत्र का कौन-सा व्यंजन खिलाना चाहेंगे?
उत्तर:
- अभिवादन: मैं अतिथियों का नमस्ते या पैर छूकर स्वागत करता हूँ, उन्हें पानी और बैठने की जगह देता हूँ।
- पारंपरिक व्यंजन: मैं अपने क्षेत्र (उत्तर भारत) का दाल-बाटी-चूरमा खिलाना चाहूँगा, क्योंकि यह स्वादिष्ट और पारंपरिक है।
चर्चा: समूह में हमने विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों जैसे पाव-भाजी, ढोकला, और बिरयानी पर चर्चा की (पेज 21)।
पेज 21: खोजबीन के लिए
प्रश्न: ‘आने’, ‘गज’, और ‘तार’ शब्दों के विषय में जानकारी इकट्ठी करें।
उत्तर:
- आना: भारतीय मुद्रा की पुरानी इकाई, एक रुपये का 1/16वाँ हिस्सा। 1957 तक प्रचलन में थी।
- गज: लंबाई मापने की इकाई, 1 गज = 3 फीट। कपड़े और जमीन मापने के लिए उपयोगी।
- तार: टेलीग्राफ, संदेश भेजने का पुराना माध्यम, जो 20वीं सदी में प्रचलित था।
विश्लेषण: ये शब्द एकांकी के समय और संदर्भ को दर्शाते हैं (पेज 21)।
अध्याय 9-नोट्स: प्रश्न-उत्तर रूप में
प्रश्न 1: कविता के अनुसार ब्रह्मांड में मानव का स्थान कैसा है?
उत्तर: कविता के अनुसार, ब्रह्मांड की तुलना में मानव का स्थान अत्यंत सूक्ष्म है। यह मानव की तुलना सूर्य, चंद्र, और नक्षत्रों से नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि मानव प्रकृति और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में बहुत छोटा है।
प्रश्न 2: कविता में मुख्य रूप से किन दो वस्तुओं के अनुपात को दिखाया गया है?
उत्तर: कविता में मानव और ब्रह्मांड के बीच के अनुपात को दर्शाया गया है। यह मानव की लघुता को ब्रह्मांड की विशालता के साथ तुलना करता है।
प्रश्न 3: कविता के अनुसार मानव किन भावों और कार्यों में लिप्त रहता है?
उत्तर: कविता के अनुसार, मानव ईर्ष्या, अहं, स्वार्थ, और घृणा जैसे नकारात्मक भावों और कार्यों में लिप्त रहता है। यह मानव की कमजोरियों को उजागर करता है।
प्रश्न 4: कविता के अनुसार मानव का सबसे बड़ा दोष क्या है?
उत्तर: मानव का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह अपनी सीमाओं और दुर्व्यवहारों को नहीं समझता। वह अपने छोटेपन को भूलकर अहंकार में डूब जाता है और ब्रह्मांड की विशालता को नजरअंदाज करता है।
प्रश्न 5: कविता का मुख्य भाव क्या है?
उत्तर: कविता का मुख्य भाव मानव की लघुता और ब्रह्मांड की विशालता के बीच का अंतर है। यह मानव को अपनी सीमाओं, कमजोरियों, और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही सकारात्मक गुणों जैसे सहयोग और सहानुभूति को अपनाने की प्रेरणा देता है।
प्रश्न 6: कविता में ‘नम गंगा’ जैसे शब्दों का क्या अर्थ है?
उत्तर: ‘नम गंगा’ जैसे शब्द दो शब्दों (‘नम’ और ‘गंगा’) के संयोजन से बने हैं, जो कविता में रचनात्मकता और अर्थ की गहराई को दर्शाते हैं। यह ब्रह्मांड की विशालता और पवित्रता को संकेत करता है।
अभ्यास के अंतिम प्रश्नों के उत्तर (हिन्दी में)
पेज 5: सोच-विचार के लिए
(क) कविता के अनुसार मानव किन कारणों में स्वयं को सीमाओं में बांधता चला जाता है?
उत्तर: कविता के अनुसार, मानव अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों जैसे ईर्ष्या, अहं, स्वार्थ, और घृणा में उलझकर स्वयं को सीमाओं में बांधता चला जाता है। वह अपनी छोटी सोच और सीमित दृष्टिकोण के कारण ब्रह्मांड की विशालता को समझने में असमर्थ रहता है।
(ख) यदि आपको इस कविता की कोई पंक्ति दीवार पर लिखनी हो, जो आपको प्रतिदिन प्रेरित करे, तो आप कौन-सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों?
उत्तर: मैं पंक्ति चुनूंगा: “पृथ्वी एक छोटा सा बिंदु।”
यह पंक्ति मुझे प्रतिदिन याद दिलाएगी कि हमारी समस्याएँ और अहंकार ब्रह्मांड की विशालता में बहुत छोटे हैं। यह मुझे नम्रता और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।
(ग) कविता मानव को सीमाओं और कमियों की ओर ध्यान दिलाता है, लेकिन कहीं भी क्रोध नहीं दिखाया। आपको इस कविता का भाव क्या लगता है – हाय, करुणा, चिंता या कुछ और? क्यों?
उत्तर: मुझे इस कविता का भाव करुणा और चिंता का मिश्रण लगता है। कविता मानव की कमियों को उजागर करती है, परंतु यह क्रोध के बजाय उसे सुधारने और अपनी सीमाओं को समझने की प्रेरणा देती है। यह करुणा के साथ मानव को बेहतर बनने का मार्ग दिखाती है।
(घ) आपके अनुसार ‘बोध’, ‘उन्नति’, ‘उद्भव’, ‘ईर्ष्या’ आदि शब्दों का अर्थ क्या है या कुछ और भी हो सकता है? अपने विचारानुसार समझाइए।
उत्तर:
- बोध: यह ज्ञान या जागरूकता को दर्शाता है। कविता में यह मानव की अपनी सीमाओं को समझने की क्षमता को संदर्भित कर सकता है।
- उन्नति: यह प्रगति या विकास को दर्शाता है। यह मानव के सकारात्मक गुणों जैसे सहयोग और सहानुभूति के माध्यम से समाज के विकास को संकेत करता है।
- उद्भव: यह उत्पत्ति या शुरुआत को दर्शाता है। यह मानव के नए विचारों या दृष्टिकोण की शुरुआत को संदर्भित कर सकता है।
- ईर्ष्या: यह नकारात्मक भाव है, जो दूसरों की सफलता से जलन को दर्शाता है। कविता इसे मानव की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत करती है।
(ङ) मानवता के विकास में सहयोग, समर्पण, और सहानुभूति जैसी सकारात्मक प्रवृत्तियाँ ईर्ष्या, अहं, स्वार्थ, और घृणा जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से कहीं अधिक प्रभावी हैं। उदाहरण के साथ बताइए कि सहानुभूति या सहयोग के कारण समाज में कैसे परिवर्तन आए हैं?
उत्तर: सहानुभूति और सहयोग ने समाज में कई सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। उदाहरण के लिए, जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने अहिंसा और सहयोग का मार्ग अपनाया, तो पूरे देश ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके अलावा, आपदा के समय लोग एक-दूसरे की सहायता करते हैं, जैसे कि बाढ़ या भूकंप के दौरान स्वयंसेवी संगठन भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहानुभूति और सहयोग समाज को एकजुट करता है और मानवता को मजबूत बनाता है।
पेज 6: अनुमान और कल्पना
(ख) मान लीजिए कि आप एक दिन के लिए पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आप मानव की कौन-कौन सी आदतों को बदलना चाहेंगे? क्यों?
उत्तर: मैं मानव की निम्नलिखित आदतों को बदलना चाहूंगा:
- ईर्ष्या: यह समाज में वैमनस्य और संघर्ष को जन्म देती है। इसे बदलकर सहानुभूति से समाज में एकता बढ़ेगी।
- अहंकार: अहंकार के कारण लोग अपनी सीमाओं को नहीं समझते। इसे नम्रता से बदलकर लोग एक-दूसरे का सम्मान करेंगे।
- स्वार्थ: स्वार्थ के कारण लोग केवल अपने हित देखते हैं। इसे सहयोग से बदलकर समाज में समृद्धि आएगी।
ये परिवर्तन इसलिए आवश्यक हैं ताकि मानव समाज अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील बन सके।
(घ) यदि आप अंतरिक्ष यात्री बन जाएँ और ब्रह्मांड के किसी दूसरे भाग में जाएँ, तो आप किस स्थान (कमरा, घर, नगर आदि) को सबसे अधिक याद करेंगे और क्यों?
उत्तर: मैं अपने घर को सबसे अधिक याद करूंगा। घर वह स्थान है जहाँ मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, जहाँ प्यार, सुरक्षा, और अपनापन है। अंतरिक्ष की विशालता में, घर की स्मृति मुझे मानवीय संबंधों और भावनाओं की याद दिलाएगी, जो मुझे मानसिक बल प्रदान करेगी।
(ग) मान लीजिए कि एक बच्चा या बच्ची कविता में उल्लिखित सभी सीमाओं को पार कर सकता है। वह कहाँ तक जाएगा या जाएगी और क्या देखेगा या देखेगी? एक कल्पनात्मक यात्रा-वृत्तांत लिखिए।
उत्तर: एक बच्चा, जिसका नाम आरव है, कविता की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड की गहराइयों में यात्रा पर निकलता है। वह पहले चंद्रमा पर पहुँचता है, जहाँ वह धूल भरे गड्ढों और शांत चाँदनी को देखता है। फिर वह मंगल ग्रह की लाल मिट्टी और विशाल ज्वालामुखियों को देखता है। वह सौरमंडल को पार कर आकाशगंगा के तारों के बीच पहुँचता है, जहाँ वह चमकते नीहारिकाओं और रंग-बिरंगे तारों को देखता है। अंत में, वह एक ब्लैक होल के पास पहुँचता है, जहाँ समय और अंतरिक्ष एक रहस्यमयी नृत्य करते हैं। इस यात्रा में आरव को यह समझ आता है कि ब्रह्मांड की विशालता के सामने उसका शरीर छोटा हो सकता है, पर उसका मन और कल्पना अनंत हैं।
(घ) इस कविता को पढ़ने के बाद, आप स्वयं को ब्रह्मांड के अनुभवों में कैसा अनुभव करते हैं? एक अनुच्छेद लिखिए- ‘मैं ब्रह्मांड में एक… हूँ!’
उत्तर: मैं ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण हूँ, जो इस अनंत सृष्टि में अपनी जगह तलाश रहा है। यह कविता मुझे सिखाती है कि मेरी समस्याएँ और अहंकार इस विशाल ब्रह्मांड में कितने तुच्छ हैं। फिर भी, मेरे भीतर की जिज्ञासा, प्रेम, और सहानुभूति मुझे इस सृष्टि का हिस्सा बनाती है। मैं एक ऐसा यात्री हूँ, जो अपनी सीमाओं को समझते हुए, ब्रह्मांड की सुंदरता और रहस्यों को खोजने के लिए उत्सुक है।
(ङ) मान लीजिए कि किसी दूसरे संसार में आपके पास संदेश आया है कि उसे पृथ्वी के किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। आप किसे भेजना चाहेंगे और क्यों?
उत्तर: मैं एक वैज्ञानिक को भेजना चाहूँगा, जैसे कि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को, जिनके पास ज्ञान, जिज्ञासा, और मानवता के प्रति समर्पण था। उनकी वैज्ञानिक सोच और मानवता के प्रति प्रेम दूसरे संसार के लिए प्रेरणा बन सकता है। वे वहाँ के प्राणियों के साथ सहयोग और समझ को बढ़ावा दे सकते हैं।
(च) कविता में ‘पृथ्वी’, ‘आह’, ‘सारथी’ जैसी प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है। कल्पना कीजिए कि एक दिन के लिए, ये भाव सभी व्यक्तियों में समाप्त हो जाएँ, तो उससे समाज में क्या-क्या परिवर्तन होगा?
उत्तर: यदि एक दिन के लिए ईर्ष्या, अहं, और स्वार्थ जैसे भाव समाप्त हो जाएँ, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। लोग एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, आपसी प्रेम और समर्पण बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने या उससे जलन करने की कोशिश नहीं करेगा। इससे समाज में शांति, एकता, और समृद्धि बढ़ेगी। लोग प्रकृति के साथ भी तालमेल बिठाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
(छ) यदि आपको इस कविता का एक पोस्टर बनाना है, जिसमें इसके मूल भाव- ‘विस्तारता और लघुता’ तथा ‘मनुष्य का भ्रम’ – दर्शाया जाए, तो आप क्या चित्र, प्रतीक, और शब्द उपयोग करेंगे? संक्षेप में बताइए।
उत्तर: मैं पोस्टर में निम्नलिखित तत्वों का उपयोग करूंगा:
- चित्र: एक विशाल, तारों से भरा आकाश जिसमें पृथ्वी एक छोटा सा बिंदु हो।
- प्रतीक: एक छोटा सा मानव आकृति जो तारों की ओर देख रही हो, यह दर्शाने के लिए कि मानव ब्रह्मांड की विशालता के सामने छोटा है।
- शब्द: “पृथ्वी एक बिंदु, मानव एक कण, फिर भी अहंकार में डूबा मन।” यह वाक्य कविता के मूल भाव को संक्षेप में दर्शाएगा।
पेज 7: अभ्यास प्रश्न
(क) कविता में कौम से लेकर खाई तक का विस्तार दिखाया गया है। इस क्रम को अपनी तरह से एक रेखाचित्र, मोहो, या मानसिक-चित्र (गाइड-मैप) द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक स्तर पर कुछ विशेषताएँ लिखिए- जैसे- पास पड़ोस की एक विशेष बात, नगर का कोई खास, उसकी विशेषता आदि। उसके नीचे एक पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए- मैं इस चित्र में कहाँ हूँ और क्यों?
उत्तर:
रेखाचित्र:
- कमरा: विशेषता – व्यक्तिगत स्थान, जहाँ मैं अपने विचारों के साथ अकेला हूँ।
- घर: विशेषता – परिवार का प्यार और सुरक्षा।
- पड़ोस: विशेषता – सामुदायिक मेलजोल और सहायता।
- नगर: विशेषता – संस्कृति और विविधता का संगम।
- देश: विशेषता – राष्ट्रीय एकता और गौरव।
- पृथ्वी: विशेषता – प्रकृति और मानवता का घर।
- ब्रह्मांड: विशेषता – अनंत तारे और रहस्य।
मैं इस चित्र में कहाँ हूँ और क्यों?
मैं इस चित्र में कमरे में हूँ, क्योंकि यहीं से मेरे विचार और सपने शुरू होते हैं, जो मुझे ब्रह्मांड की विशालता तक ले जाते हैं।
(ख) अगर इस कविता की तरह कोई कहानी लिखनी हो, जिसका नाम हो ‘उद्भव में मानव’, तो उसको आरंभ कैसे करेंगे? कुछ वाक्य लिखिए।
उत्तर:
“एक अनंत आकाश में, जहाँ तारे अनगिनत कहानियाँ कहते थे, एक छोटे से ग्रह पर मानव का उद्भव हुआ। वह पृथ्वी नामक इस नीले बिंदु पर खड़ा था, अपने छोटे से कमरे में, यह सोचते हुए कि वह इस विशाल सृष्टि का केंद्र है। परंतु, जैसे ही उसने आकाश की ओर देखा, उसे अपनी लघुता का बोध हुआ।”
(ग) ‘एक कमरे में मैं दो दीया रखता हूँ’ पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। अगर आपका कहा जाए कि आप एक ऐसी कविता बनाएँ, जिसमें कोई दीवार न हो, तो वह कैसी होगी? उसका वर्णन कीजिए।
उत्तर: ऐसी कविता में दीवारों की अनुपस्थिति स्वतंत्रता और अनंतता का प्रतीक होगी। यह कविता खुले आकाश, अनंत तारों, और मानव के विचारों की स्वच्छंद उड़ान को दर्शाएगी। इसमें मानव की सीमाएँ, जैसे अहंकार और स्वार्थ, गायब होंगी, और वह ब्रह्मांड के साथ एकरूप हो जाएगा। कविता में पंक्तियाँ होंगी जैसे: “न कोई दीवार, न कोई सीमा, मैं हूँ ब्रह्मांड का एक हिस्सा, अनंत में समाया।”
(घ) एक चित्र श्रींखला बनाएँ, जिसमें ये क्रम दिखे
आदमी—> कमरा —> घर —> पडोसी क्षेत्र—>नगर—>देश —> पृथ्वी —>ब्रह्मांड
प्रत्येक स्तर में आकार का अनुपात दिखाया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो कि आदमी कितना छोटा है।
उत्तर: चित्र का वर्णन:
- एक गोलाकार गुम्बद जिसमें केंद्र में एक छोटा सा बिंदु (मानव) हो।
- इसके चारों ओर गाढ़े रंग का एक छोटा वृत्त (कमरा), फिर बड़ा वृत्त (घर), फिर पड़ोस, नगर, देश, पृथ्वी, और सबसे बाहरी परत में तारों से भरा ब्रह्मांड।
- प्रत्येक स्तर पर आकार बढ़ता जाए, जिससे मानव की तुलना में ब्रह्मांड की विशालता स्पष्ट हो।
- रंगों का उपयोग: मानव के लिए हल्का नीला, और ब्रह्मांड के लिए गहरा नीला, जो अनंतता दर्शाए।
अध्याय 10-तरूण के स्वप्न- नोट्स: प्रश्न-उत्तर रूप में
प्रश्न 1: सुभाषचंद्र बोस के स्वप्न का मुख्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर: सुभाषचंद्र बोस का स्वप्न एक स्वाधीन, समान, और प्रगतिशील समाज और राष्ट्र का निर्माण करना था, जहाँ जातिभेद, नारी-पुरुष असमानता, और आर्थिक विषमता न हो। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति के समान अवसर मिलें, और समाज में श्रम व कर्म की मर्यादा हो।
प्रश्न 2: बोस के अनुसार आदर्श समाज की विशेषताएँ क्या थीं?
उत्तर: आदर्श समाज में व्यक्ति सभी दृष्टियों से मुक्त हो, जातिभेद न हो, नारी को पुरुषों के समान अधिकार मिलें, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों, और श्रम व कर्म को सम्मान मिले। समाज में अकर्मण्यता के लिए कोई स्थान न हो।
प्रश्न 3: सुभाषचंद्र बोस ने अपने स्वप्न को क्यों असीम शक्ति और आनंद का स्रोत माना?
उत्तर: सुभाषचंद्र बोस ने अपने स्वप्न को असीम शक्ति और आनंद का स्रोत माना क्योंकि यह स्वप्न भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता, समानता, और प्रगति का प्रतीक था। यह उन्हें कठिनाइयों का सामना करने और बलिदान देने की प्रेरणा देता था।
प्रश्न 4: बोस ने अपने भाषण में किसे संबोधित किया और क्यों?
उत्तर: बोस ने अपने भाषण में भारतवासियों, विशेष रूप से युवाओं को संबोधित किया, क्योंकि वे चाहते थे कि युवा पीढ़ी उनके स्वप्न को अपनाए और उसे साकार करने के लिए कार्य करे।
प्रश्न 5: सुभाषचंद्र बोस ने ‘आजाद हिंद फौज’ की स्थापना क्यों की?
उत्तर: सुभाषचंद्र बोस ने ‘आजाद हिंद फौज’ की स्थापना की ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया जा सके और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो। उन्होंने सैनिकों को “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा” जैसे नारों से प्रेरित किया।
प्रश्न 6: बोस के भाषण में प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्द और उनके अर्थ क्या हैं?
उत्तर:
- स्वाधीन: स्वतंत्र, अपने अधीन।
- आदर्श: उच्चतम उदाहरण या लक्ष्य।
- उन्नति: प्रगति, विकास।
- जातिभेद: जाति के आधार पर भेदभाव।
- समानता: सभी के लिए समान अवसर और अधिकार।
अभ्यास के अंतिम प्रश्नों के उत्तर (हिन्दी में)
पेज 5: पक्तियों पर चर्चा
(क) “उस समाज में अर्थ की विषमता न हो।”
उत्तर: इस पंक्ति का अर्थ है कि सुभाषचंद्र बोस एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ धन और संसाधनों का असमान वितरण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समान अवसर मिलें, ताकि गरीबी और अभाव समाप्त हो। यह समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में एक कदम है।
(ख) “यही स्वप्न उनकी शक्ति का उद्गम बना और उनके आनंद का निर्धारण रहा।”
उत्तर: इस पंक्ति का अर्थ है कि सुभाषचंद्र बोस का स्वप्न (स्वाधीन और समान समाज) उनकी प्रेरणा और शक्ति का स्रोत था। यह स्वप्न उन्हें संघर्ष करने और बलिदान देने की ऊर्जा देता था, साथ ही उनके जीवन को आनंद और उद्देश्य प्रदान करता था।
(ग) “उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हों।”
उत्तर: इस पंक्ति का अर्थ है कि बोस एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, और मानसिक बंधनों से मुक्त हो। इसका मतलब है कि जाति, लिंग, धर्म, या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न हो, और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके।
पेज 5: सोच-विचार के लिए
(क) नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने किस प्रकार के राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखा था?
उत्तर: नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने एक स्वाधीन, समान, और प्रगतिशील राष्ट्र का स्वप्न देखा था। यह राष्ट्र जातिभेद, आर्थिक विषमता, और सामाजिक दबाव से मुक्त हो, जहाँ नारी-पुरुष को समान अधिकार मिलें, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति के अवसर प्राप्त हों, और श्रम व कर्म को सम्मान मिले। यह राष्ट्र विश्व के समक्ष एक आदर्श के रूप में स्थापित हो।
(ख) नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने किस लक्ष्य की प्राप्ति को अपने जीवन की सर्वशक्तता के रूप में देखा?
उत्तर: नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता और एक आदर्श समाज के निर्माण को अपने जीवन की सर्वशक्तता के रूप में देखा। वे चाहते थे कि भारत एक स्वाधीन राष्ट्र बने, जो सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित हो और विश्व में आदर्श प्रस्तुत करे। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और बलिदान की प्रेरणा दी।
(ग) “आदमों तथा अकर्मण्यों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा” सुभाषचंद्र बोस ने ऐसा क्यों कहा होगा?
उत्तर: सुभाषचंद्र बोस ने यह कहा क्योंकि वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ प्रत्येक व्यक्ति कर्मठ और सक्रिय हो। वे चाहते थे कि समाज में आलस्य, निष्क्रियता, और अकर्मण्यता न हो, बल्कि सभी लोग श्रम और कर्म के माध्यम से समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान दें। अकर्मण्य लोग समाज की प्रगति में बाधा बनते हैं, इसलिए उनके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
(घ) नेताजी सुभाषचंद्र बोस के लक्ष्यों का लेखा जोखा करने के लिए आज की युवा पीढ़ी क्या-क्या कर सकती है?
उत्तर: आज की युवा पीढ़ी नेताजी के लक्ष्यों को साकार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकती है:
- शिक्षा और जागरूकता: युवा शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता और जातिभेद के खिलाफ जागरूकता फैला सकते हैं।
- सामाजिक कार्य: सामाजिक कार्यों में भाग लेकर गरीबी, असमानता, और अशिक्षा को दूर करने में योगदान दे सकते हैं।
- नारी सशक्तीकरण: नारी के अधिकारों और समानता के लिए कार्य कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय एकता: विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।
- कर्मठता: अपने कार्यों में मेहनत और समर्पण के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकते हैं।
पेज 5: अनुमान और कल्पना से
(क) “उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हों” सुभाषचंद्र बोस ने किन-किन दृष्टियों से मुक्ति की बात की होगी?
उत्तर: सुभाषचंद्र बोस ने निम्नलिखित दृष्टियों से मुक्ति की बात की होगी:
- सामाजिक दृष्टि: जाति, धर्म, और लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्ति।
- आर्थिक दृष्टि: धन और संसाधनों की असमानता से मुक्ति।
- मानसिक दृष्टि: अज्ञानता, अंधविश्वास, और संकीर्ण सोच से मुक्ति।
- राजनीतिक दृष्टि: विदेशी शासन और दबाव से मुक्ति।
- सांस्कृतिक दृष्टि: परंपराओं के बंधनों से मुक्त होकर प्रगतिशील सोच अपनाना।
(ख) “उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज में पुरुषों की तरह समान अधिकार का…” सुभाषचंद्र बोस को उनके भाषण में नारी के लिए समान अधिकारों की बात क्यों कही पड़ी?
उत्तर: सुभाषचंद्र बोस ने नारी के लिए समान अधिकारों की बात इसलिए कही क्योंकि वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ कोई भेदभाव न हो। उस समय नारियाँ सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक रूप से पुरुषों से पीछे थीं। बोस का मानना था कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब नारी को पुरुषों के समान अवसर और अधिकार मिलें, ताकि वे समाज और राष्ट्र के निर्माण में बराबर का योगदान दे सकें।
(ग) आपके विचार में समाज में और कौन-कौन से लोग हैं जिन्हें समान अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है?
उत्तर: मेरे विचार में समाज में निम्नलिखित लोगों को समान अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: गरीब और वंचित समुदायों को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए।
- दिव्यांगजन: शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम लोगों को समान सुविधाएँ और सम्मान मिलना चाहिए।
- अल्पसंख्यक समुदाय: धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को बिना भेदभाव के समान अधिकार मिलने चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लोग: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी सुविधाओं के समान अवसर मिलने चाहिए।
(घ) सुभाषचंद्र बोस देश के समक्ष युवा को संबोधित करते हुए कहते हैं “यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ- स्वीकार करो।” सुभाषचंद्र बोस के इस स्वप्न पर आपके (युवा) की क्या प्रतिक्रिया होगी?
उत्तर: एक युवा के रूप में, मैं सुभाषचंद्र बोस के इस स्वप्न को पूरे उत्साह और समर्पण के साथ स्वीकार करूँगा। उनका स्वप्न एक समान, स्वाधीन, और प्रगतिशील समाज का है, जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं अपने कार्यों और विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाऊँ। मैं शिक्षा, सामाजिक समानता, और नारी सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में कार्य करके उनके स्वप्न को साकार करने का प्रयास करूँगा।
पेज 6: अभ्यास प्रश्न
(क) अपने नेताजी सुभाषचंद्र बोस के भाषण का एक अंश पढ़ा है, इस ‘सपनों के स्वप्न’ शीर्षक दिया गया है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि यह शीर्षक क्यों दिया गया होगा?
उत्तर: यह शीर्षक इसलिए दिया गया होगा क्योंकि सुभाषचंद्र बोस ने अपने भाषण में एक आदर्श समाज और राष्ट्र के स्वप्न की बात की है। यह स्वप्न उनकी प्रेरणा और शक्ति का स्रोत था, और वे चाहते थे कि यह स्वप्न भारतवासियों, विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा बने। ‘सपनों के स्वप्न’ शीर्षक उनके इस उच्च और प्रेरणादायक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
(ख) यदि आपको भाषण के इस अंश को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा? यह भी लिखिए।
उत्तर: मैं इस भाषण के अंश को “आदर्श भारत का स्वप्न” नाम दूँगा। मैंने यह नाम इसलिए सोचा क्योंकि यह भाषण भारत के लिए एक स्वाधीन, समान, और प्रगतिशील समाज के निर्माण की दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह नाम बोस के आदर्शवादी और प्रेरणादायक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
(ग) सुभाषचंद्र बोस ने अपने समय की स्थितियों या समस्याओं को अपने संबोधन में स्थान दिया है। यदि आपको अपनी कक्षा को संबोधित करने का अवसर मिले तो आप किन-किन विषयों को अपने उद्बोधन में सम्मिलित करेंगे और उसका क्या शीर्षक रहेगा?
उत्तर: यदि मुझे अपनी कक्षा को संबोधित करने का अवसर मिले, तो मैं निम्नलिखित विषयों को शामिल करूँगा:
- शिक्षा का महत्व: सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता।
- पर्यावरण संरक्षण: जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता।
- सामाजिक समानता: जाति, लिंग, और आर्थिक भेदभाव को समाप्त करना।
- युवाओं की भूमिका: समाज और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की जिम्मेदारी।
शीर्षक: “नए भारत की नींव: युवा और समानता”।
पेज 6: भाषा की बात
(क) सुभाषचंद्र बोस ने अपने भाषण में संज्ञा, संबोधन या भाव आदि का बोध करने वाले शब्दों के साथ उनकी विशेषता अथवा गुण बताने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। उनके भाषण से विशेषता अथवा गुण बताने वाले शब्द ढूँढकर दिए गए शब्द समूह को पूरा लिखिए।
उत्तर: सुभाषचंद्र बोस के भाषण से विशेषता या गुण बताने वाले कुछ शब्द और उनके संदर्भ:
- स्वाधीन (विशेषण): स्वतंत्र, अपने अधीन (उदाहरण: स्वाधीन राष्ट्र)।
- आदर्श (विशेषण): उच्चतम और प्रेरणादायक (उदाहरण: आदर्श समाज)।
- समान (विशेषण): बराबर, भेदरहित (उदाहरण: समान अधिकार)।
- प्रगतिशील (विशेषण): उन्नति की ओर बढ़ने वाला (उदाहरण: प्रगतिशील समाज)।
- कर्मठ (विशेषण): मेहनती, सक्रिय (उदाहरण: कर्मठ व्यक्ति)।
(ख) सुभाषचंद्र बोस ने तो उपर्युक्त विशेषताओं के साथ इन शब्दों को रखा है। आप किन विशेषताओं के साथ इन उपयुक्त शब्दों को रखना चाहेंगे और क्यों? लिखिए।
उत्तर: मैं निम्नलिखित विशेषताओं के साथ इन शब्दों को रखना चाहूँगा:
- स्वाधीन: मैं इसे “जिम्मेदार” विशेषता के साथ रखूँगा, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आती है।
- आदर्श: मैं इसे “प्रेरणादायक” विशेषता के साथ रखूँगा, क्योंकि आदर्श समाज दूसरों को प्रेरित करता है।
- समान: मैं इसे “निष्पक्ष” विशेषता के साथ रखूँगा, क्योंकि समानता निष्पक्षता पर आधारित होनी चाहिए।
- प्रगतिशील: मैं इसे “नवाचारी” विशेषता के साथ रखूँगा, क्योंकि प्रगति के लिए नवाचार आवश्यक है।
- कर्मठ: मैं इसे “समर्पित” विशेषता के साथ रखूँगा, क्योंकि कर्मठता में समर्पण का भाव होना चाहिए।
कारण: ये विशेषताएँ आधुनिक समाज की जरूरतों को दर्शाती हैं और बोस के स्वप्न को और सशक्त बनाती हैं।
पेज 7: विपरीतार्थी शब्द और उनके प्रयोग
(क) “और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र” इस वाक्यांश में स्वाधीन का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है ‘पराधीन’। इसी प्रकार के कुछ विपरीतार्थी शब्द आप दिए गए हैं, लेकिन वे आपके सामने नहीं हैं। स्वयं विचारकर विपरीतार्थी शब्दों के सही जोड़े बनाएँ।
उत्तर: निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी जोड़े:
- स्वाधीन – पराधीन
- समान – असमान
- उन्नति – अवनति
- कर्मठ – अकर्मण्य
- आदर्श – त्रुटिपूर्ण
(ख) अब सं. 1 और सं. 2 के सभी शब्दों से दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाएँ, जैसे- “समाज की उन्नति अकर्मण्य नहीं अपितु कर्मण्य व्यक्तियों पर निर्भर है।”
उत्तर:
- स्वाधीन – पराधीन: राष्ट्र की प्रगति स्वाधीन व्यक्तियों पर निर्भर है, न कि पराधीन मानसिकता वालों पर।
- समान – असमान: समाज में समान अवसरों से विकास होता है, असमान व्यवहार से नहीं।
- उन्नति – अवनति: देश की उन्नति कर्मठता पर निर्भर है, अवनति पर नहीं।
- कर्मठ – अकर्मण्य: समाज का विकास कर्मठ लोगों से होता है, अकर्मण्य लोगों से नहीं।
- आदर्श – त्रुटिपूर्ण: एक आदर्श समाज प्रेरणा देता है, जबकि त्रुटिपूर्ण व्यवस्था निराश करती है।
पेज 7: आपकी बात
(क) आपने सुभाषचंद्र बोस के स्वप्न के बारे में जाना। आप अपने विद्यालय, राज्य और देश के बारे में कैसे स्वप्न देखते हैं? लिखिए।
उत्तर: मैं अपने विद्यालय, राज्य, और देश के लिए निम्नलिखित स्वप्न देखता हूँ:
- विद्यालय: मेरा विद्यालय ऐसा हो जहाँ प्रत्येक छात्र को समान अवसर मिलें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और नवाचार को प्रोत्साहन मिले।
- राज्य: मेरा राज्य आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो, जहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान विकास हो, और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए।
- देश: मेरा देश एक ऐसा राष्ट्र हो जहाँ जाति, धर्म, और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, सभी को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिलें, और भारत विश्व में शांति और प्रगति का प्रतीक बने।
(ख) हमें बड़ी लड़ाई के बाद स्वतंत्रता मिली थी। अपनी इस स्वतंत्रता का मान स्वयं के लिए हम अपने स्तर पर क्या-क्या कर सकते हैं? लिखिए।
उत्तर: अपनी स्वतंत्रता का मान रखने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
- शिक्षा और जागरूकता: स्वयं को शिक्षित करें और दूसरों को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करें।
- सामाजिक समानता: जाति, धर्म, और लिंग भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएँ।
- पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण और कचरा प्रबंधन जैसे कार्य करें।
- कर्मठता: अपने कार्यों में मेहनत और ईमानदारी से समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान दें।
- राष्ट्रीय एकता: विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा दें।
पेज 8: अभ्यास प्रश्न
(क) नीचे स्तंभ 1 में स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं और स्तंभ 2 में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए गए हैं। तथ्यों का स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से सही मिलान कीजिए।
उत्तर:
| क्रम | स्तंभ 1 | स्तंभ 2 | सही मिलान |
|---|---|---|---|
| 1. | 8 अप्रैल, 1929 को चंद्रशेखर आजाद में स्वयं पंचने वाले क्रांतिकारी, शहीद-ए-आजम के नाम से जाने जाते हैं। | 1. सरदार वल्लभभाई पटेल | चंद्रशेखर आजाद |
| 2. | ‘स्वराज पार्टी’ के संस्थापकों में से एक, सुभाषचंद्र बोस के राजनीतिक गुरु बने। | 2. महात्मा गांधी | चितरंजन दास |
| 3. | जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजनीतिक बंदियों के समान व्यवहार न होने के कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से भूख हड़ताल शुरू कर दी। अवसर के निःसंदेह दिन जेल में इन्हें देहांत हो गया। | जतिंद्रनाथ दास |
पेज 9: स्त्री सशक्तीकरण
(क) सुभाषचंद्र बोस ने नारियों के लिए समान अधिकार की बात की है। अपने अनुमानों के आधार पर बताइए कि उन्हें कौन-कौन से विशेष अधिकार चाहिए?
उत्तर: सुभाषचंद्र बोस ने नारियों के लिए निम्नलिखित विशेष अधिकारों की बात की होगी:
- शिक्षा का अधिकार: नारियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर।
- रोजगार का अधिकार: नारियों को सभी क्षेत्रों में समान रोजगार के अवसर।
- राजनीतिक भागीदारी: नारियों को राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान भागीदारी।
- सामाजिक सम्मान: सामाजिक भेदभाव से मुक्ति और सम्मानजनक व्यवहार।
- आर्थिक स्वतंत्रता: संपत्ति और संसाधनों पर समान अधिकार।
(ख) सुभाषचंद्र बोस ने ‘आजाद हिंद फौज’ जो गठित किया था, उसमें एक टुकड़ी नारियों की भी थी। उस टुकड़ी का नाम पता लगाकर लिखिए। उस टुकड़ी की भूमिका क्या थी? यह भी बताइए।
उत्तर:
- टुकड़ी का नाम: रानी झाँसी रेजिमेंट।
- भूमिका: रानी झाँसी रेजिमेंट आजाद हिंद फौज का एक हिस्सा थी, जिसमें महिलाएँ सैनिक के रूप में प्रशिक्षित थीं। इस टुकड़ी की भूमिका भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष में भाग लेना, युद्ध में सहायता करना, और नारी सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना था। यह टुकड़ी महिलाओं की साहस और समर्पण की प्रतीक थी।
पेज 9: आपके प्रिय स्वतंत्रता सेनानी
(क) आप किस स्वतंत्रता सेनानी के कार्यों व विचारों से प्रभावित हैं? कारण सहित लिखिए और अभिव्यक्ति (रोल प्ले) करते हुए उनके विचारों की कक्षा में चर्चा कीजिए।
उत्तर: मैं सुभाषचंद्र बोस के कार्यों और विचारों से अत्यधिक प्रभावित हूँ।
कारण:
- साहस और नेतृत्व: बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया।
- आदर्श समाज की दृष्टि: उन्होंने एक समान, स्वाधीन, और प्रगतिशील समाज की कल्पना की, जिसमें नारी-पुरुष को समान अधिकार मिलें।
- प्रेरणादायक नारे: “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा” जैसे नारों से उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया।
रोल प्ले में चर्चा: मैं कक्षा में बोस के रूप में उनके स्वप्न को प्रस्तुत करूँगा, जिसमें मैं युवाओं को समानता और कर्मठता के लिए प्रेरित करूँगा, और उनके नारे का उपयोग करके स्वतंत्रता और एकता का संदेश दूँगा।
पेज 9: नारा और स्वतंत्रता सेनानी
(ख) नोट लिस्ट 1 में कुछ नारे दिए गए हैं। नोट करें लिस्टन लिखिए, कि वह किसके द्वारा दिया गया? आप पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं।
उत्तर:
| नारा | स्वतंत्रता सेनानी |
|---|---|
| स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है | बाल गंगाधर तिलक |
| करो या मरो | महात्मा गांधी |
| मैं आजाद हूँ, आजाद रहूँगा और आजाद ही मरूँगा | चंद्रशेखर आजाद |
| इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद | भगत सिंह |
| पूर्ण स्वराज | जवाहरलाल नेहरू |
पेज 10: परियोजना कार्य
(क) आप सभी राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में पढ़कर उनमें से 10 महिला एवं 10 पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों का संग्रह करके एक सांख्यिकीय तंत्र कीजिए। चित्रों के नीचे उनके विशेष योगदान के बारे में एक-दो वाक्य भी लिखिए। अपनी संश्लिष्ट तैयार करते समय ध्यान रखिए कि आप किसी भी राज्य से एक से अधिक व्यक्ति न चुनें।
उत्तर: 10 महिला स्वतंत्रता सेनानी:
- रानी लक्ष्मीबाई (उत्तर प्रदेश): झाँसी की रानी ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया।
- सावित्रीबाई फुले (महाराष्ट्र): महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किया।
- दुर्गाबाई देशमुख (आंध्र प्रदेश): स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया।
- कमला नेहरू (उत्तराखंड): स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और महिलाओं को संगठित किया।
- अरुणा आसफ अली (पंजाब): 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- कस्तूरबा गांधी (गुजरात): अहिंसक आंदोलनों में गांधीजी के साथ सक्रिय रही।
- सरोजिनी नायडू (पश्चिम बंगाल): कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया।
- भिकाजी कामा (महाराष्ट्र): विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया।
- उषा मेहता (गुजरात): गुप्त रेडियो स्टेशन चलाकर स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन दिया।
- लक्ष्मी सहगल (तमिलनाडु): आजाद हिंद फौज की रानी झाँसी रेजिमेंट की कमांडर थीं।
10 पुरुष स्वतंत्रता सेनानी:
- महात्मा गांधी (गुजरात): अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया।
- जवाहरलाल नेहरू (उत्तर प्रदेश): स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने।
- सुभाषचंद्र बोस (पश्चिम बंगाल): आजाद हिंद फौज के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष किया।
- भगत सिंह (पंजाब): क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी।
- चंद्रशेखर आजाद (मध्य प्रदेश): क्रांतिकारी संगठनों का नेतृत्व किया और शहीद हुए।
- लाला लाजपत राय (पंजाब): ‘लाल-बाल-पाल’ तिकड़ी के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया।
- बाल गंगाधर तिलक (महाराष्ट्र): ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है’ का नारा दिया।
- चितरंजन दास (पश्चिम बंगाल): स्वराज पार्टी की स्थापना की और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया।
- राजेंद्र प्रसाद (बिहार): स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने।
- सरदार वल्लभभाई पटेल (गुजरात): भारत की एकता के लिए ‘लौह पुरुष’ के रूप में कार्य किया।
नोट: चित्रों का संग्रह करने के लिए पुस्तकालय या इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है, और प्रत्येक चित्र के नीचे उनके योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखा जाएगा।